BPSC PYQ Mains Answer Writing,Day -4
By - Gurumantra Civil Class
At - 2025-09-23 17:35:48
BPSC PYQ Mains Program Answer Writing
Session I – Polity + Bihar + Special + Economy
Day – 4
1. संसदीय संप्रभुताष्ठ का क्या अर्थ है? क्या आप भारतीय संसद को प्रभुत्व संपन्न या गैर प्रभुत्व संपन्न या दोनों समझते हैं? आप अपने विचार दीजिए ।
What is the meaning of "Parliamentary Sovereignty" ? Do you consider Indian Parliament A sovereign or a non sovereign or both? Give your views. (In 250 Words.)
2. नीचे दिए गए प्रश्नों को सौ से डेढ़ सौ शब्दों में लिखे ।
Write down the following questions in a hundred to one hundred and fifty words.
(a) भारतवर्ष के संविधान में निहित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की विवेचना कीजिए एवं उसका महत्व बतलाइए।
Discuss the directive principles of state policy enshrined in the indian constitution and state their importance.
(b) बिहार में समृद्ध प्राकृतिक साधनों के बावजूद औद्योगिक विकास की गति धीमी क्यों है ?
Why is the pace of industrial development in Bihar poor inspite or rich natural resources. Discuss.
3. नीचे दिए गए प्रश्नों को सौ से डेढ़ सौ शब्दों में लिखे ।
Write down the following questions in a hundred to one hundred and fifty words.
(a) विकास के लिए बढ़ती जनसंख्या एक प्रमुख बाधक है।विवेचना ।
Rising population is a great hindrance to development. Discuss it.
(b) जिला योजना से आप क्या समझते है ? इसके सफल होने के कौन से शर्त है ?
What do you mean by district planning? What are the conditions of its success?
📚 BPSC Mains Writing Practice – 40 Days Program
(39th - 70th BPSC Mains PYQ – Complete Writing Practice)
⚡ 40 दिन का दमदार राइटिंग प्रोग्राम – सफलता की गारंटी की ओर पहला कदम! ⚡
✨ अब तैयारी होगी और भी सटीक ✨
👉 विशेष रूप से 71st & 72nd BPSC Mains के लिए
👉 Offline + Online Mode में सुविधा
👉 साथ में Answer Module भी उपलब्ध
📅 Batch Start: 18 September 2025
📞 Admission Helpline:
9135904639 | 7250380187
App.- Gurumantra.online
🏛️ Offline Centre:
Parwati Market, West Boring Canal Road,
Beside Power Substation, Patna – 01
1 Ans.-
1. संसदीय संप्रभुताष्ठ का क्या अर्थ है? क्या आप भारतीय संसद को प्रभुत्व संपन्न या गैर प्रभुत्व संपन्न या दोनों समझते हैं? आप अपने विचार दीजिए ।
संसदीय संप्रभुता एक राजनीतिक और संवैधानिक अवधारणा है, जो मुख्य रूप से ब्रिटिश संवैधानिक व्यवस्था से जुड़ी हुई है। इसका मूल अर्थ यह है कि संसद (या विधायिका) राज्य की सर्वोच्च शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है, और उसके द्वारा बनाए गए कानूनों पर कोई अन्य संस्था (जैसे न्यायपालिका या कार्यपालिका) चुनौती नहीं दे सकती।
ए.वी. डाइसी (A.V. Dicey) ने इसे तीन मुख्य सिद्धांतों में परिभाषित किया है:
संसद कोई भी कानून बना सकती है: संसद को किसी भी विषय पर कानून बनाने की पूर्ण स्वतंत्रता है, चाहे वह कितना भी असामान्य या विवादास्पद क्यों न हो। उदाहरण: ब्रिटेन में संसद ने 1949 में "Parliament Act" के माध्यम से हाउस ऑफ लॉर्ड्स की शक्ति को सीमित किया, जिससे हाउस ऑफ कॉमन्स की प्रधानता स्थापित हुई। इससे पता चलता है कि संसद खुद अपनी शक्तियों को बदल सकती है।
पूर्व संसद बाद की संसद को बाध्य नहीं कर सकती: कोई भी संसद अपने उत्तराधिकारी को बंधन में नहीं बांध सकती। उदाहरण: ब्रिटेन में 1716 का "Septennial Act" संसद की अवधि को 3 से 7 वर्ष कर दिया गया, लेकिन बाद में इसे बदला गया। हाल ही में, ब्रेक्सिट (2016 रेफरेंडम के बाद) के दौरान संसद ने यूरोपीय संघ से बाहर निकलने के लिए कानून बनाए, जो पूर्व संधियों को ओवरराइड कर देते हैं।
न्यायपालिका संसद के कानूनों की वैधता पर सवाल नहीं उठा सकती: न्यायालय केवल कानूनों की व्याख्या कर सकते हैं, उन्हें असंवैधानिक घोषित नहीं। उदाहरण: ब्रिटेन के "Factortame Case" (1990) में, हालांकि यूरोपीय कानूनों के कारण संसद की शक्ति पर बहस हुई, लेकिन मूल सिद्धांत बना रहा। हालांकि, आधुनिक समय में मानवाधिकार अधिनियम (1998) और यूरोपीय संघ के प्रभाव से इसकी पूर्णता पर सवाल उठे हैं, लेकिन ब्रिटेन में अभी भी कोई लिखित संविधान नहीं है, इसलिए संसद सर्वोच्च बनी हुई है।
यह अवधारणा अन्य देशों में अलग-अलग रूपों में दिखती है। उदाहरण के लिए, न्यूजीलैंड और इजराइल में भी अनलिखित संविधान के कारण संसद संप्रभु है, जबकि अमेरिका और जर्मनी जैसे देशों में संविधान सर्वोच्च है, और न्यायालय कानूनों को रद्द कर सकता है। भारत में यह अवधारणा ब्रिटिश प्रभाव से आई, लेकिन लिखित संविधान के कारण सीमित है।
ब्रिटिश संसदीय संप्रभुता का उदाहरणसंसदीय संप्रभुता का सबसे प्रमुख उदाहरण यूनाइटेड किंगडम की संसद है। ब्रिटिश न्यायविद् ए.वी. डाइसी के अनुसार, ब्रिटिश संसदीय संप्रभुता की तीन मुख्य विशेषताएं हैं:
संसद कोई भी कानून बना, संशोधित या निरस्त कर सकती है
संविधान संबंधी कानून सामान्य कानूनों की भांति ही बनाए जा सकते हैं
न्यायपालिका संसद के कानूनों को असंवैधानिक घोषित नहीं कर सकती
भारतीय संसद और संप्रभुता की स्थिति-
भारतीय संसद को पूर्ण संप्रभु निकाय नहीं माना जा सकता क्योंकि यह संविधान के प्रावधानों के अधीन है। ब्रिटिश संसद के विपरीत, भारत में संविधान सर्वोच्च है, संसद नहीं।
भारतीय संसद की संप्रभुता की सीमाएं-
लिखित संविधान: भारत का संविधान एक लिखित दस्तावेज़ है जो राज्य के सभी अंगों पर सीमाएं आरोपित करता है। संसद इस लिखित दस्तावेज़ से ऊपर नहीं हो सकती।
न्यायिक समीक्षा: भारत में न्यायपालिका संसद द्वारा बनाए गए कानूनों की समीक्षा कर सकती है और यदि वे संविधान के प्रतिकूल हों तो उन्हें शून्य घोषित कर सकती है।
संघीय व्यवस्था: संविधान की सातवीं अनुसूची के अंतर्गत केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन है। संसद केवल संघ सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बना सकती है।
मौलिक अधिकार: अनुच्छेद 13 के तहत, कोई भी कानून जो मौलिक अधिकारों का हनन करता है, वह शून्य माना जाता है।
संविधान संशोधन की सीमित शक्ति: केशवानंद भारती मामले (1973) में स्थापित मूल संरचना सिद्धांत के अनुसार, संसद संविधान की मूल संरचना को नष्ट नहीं कर सकती।
भारतीय संसद: प्रभुत्व संपन्न (Sovereign) पक्ष का विस्तार
भारतीय संसद को कुछ अर्थों में प्रभुत्व संपन्न माना जा सकता है, क्योंकि संविधान उसे व्यापक शक्तियां देता है। यह ब्रिटिश मॉडल से प्रेरित है, लेकिन भारतीय संदर्भ में अनुकूलित। मुख्य बिंदु:
विधायी शक्तियां: अनुच्छेद 245-246 के तहत, संसद केंद्र और समवर्ती सूचियों पर कानून बना सकती है। उदाहरण: जीएसटी एक्ट (2017) के माध्यम से संसद ने कर प्रणाली में बड़ा बदलाव किया, जो राज्य और केंद्र की शक्तियों को एकीकृत करता है। यह संसद की क्षमता दिखाता है कि वह आर्थिक नीतियों को राष्ट्रीय स्तर पर लागू कर सकती है।
संविधान संशोधन की शक्ति: अनुच्छेद 368 संसद को संविधान बदलने की अनुमति देता है। विशिष्ट उदाहरण:
44वां संशोधन (1978): इमरजेंसी के बाद, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर निर्देशक सिद्धांतों में डाला गया। इससे संसद ने मौलिक अधिकारों को भी प्रभावित किया, जो उसकी संप्रभुता का प्रमाण है।
42वां संशोधन (1976): इमरजेंसी के दौरान, संसद ने संविधान में बड़े बदलाव किए, जैसे मौलिक अधिकारों को निलंबित करने की शक्ति और न्यायिक समीक्षा को सीमित करना। हालांकि बाद में इसे आंशिक रूप से रद्द किया गया, लेकिन यह दिखाता है कि संसद कितनी दूर जा सकती है।b17176
आर्टिकल 370 का रद्दीकरण (2019): संसद ने जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद को रद्द किया, और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया। 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे वैध माना, जो संसद की संप्रभुता को मजबूत करता है, क्योंकि कोर्ट ने कहा कि यह संविधान के ढांचे में फिट बैठता है।
कार्यपालिका पर नियंत्रण: संसद सरकार बनाती और गिराती है। उदाहरण: 1991 में पी.वी. नरसिम्हा राव सरकार ने संसद के समर्थन से आर्थिक सुधार किए, जो देश की दिशा बदल दी।
भारतीय संसद: गैर प्रभुत्व संपन्न (Non-Sovereign) पक्ष का विस्तार
भारत में संविधान सर्वोच्च है, इसलिए संसद की शक्ति सीमित है। न्यायपालिका (सुप्रीम कोर्ट) संसद के कार्यों की समीक्षा कर सकती है। मुख्य बिंदु:
संविधान की सर्वोच्चता: अनुच्छेद 13 के तहत, कोई कानून मौलिक अधिकारों के विपरीत नहीं हो सकता। उदाहरण: शायरा बानो केस (2017) में ट्रिपल तलाक को असंवैधानिक घोषित किया गया, भले ही संसद ने बाद में कानून बनाया।
मूल संरचना सिद्धांत: यह संसद की सबसे बड़ी सीमा है। विशिष्ट उदाहरण:
गोलकनाथ केस (1967): सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद मौलिक अधिकारों को संशोधित नहीं कर सकती। इससे संसद की संप्रभुता पर पहला बड़ा हमला हुआ।
केशवानंद भारती केस (1973): कोर्ट ने मूल संरचना सिद्धांत स्थापित किया, जिसमें संघीय ढांचा, धर्मनिरपेक्षता, न्यायिक समीक्षा आदि शामिल हैं। उदाहरण: 24वें संशोधन को चुनौती दी गई, और कोर्ट ने कहा कि संसद मूल संरचना नहीं बदल सकती।
मिनर्वा मिल्स केस (1980): 42वें संशोधन के कुछ हिस्सों को रद्द किया गया, क्योंकि वे मूल संरचना (जैसे मौलिक अधिकार vs निर्देशक सिद्धांत) को प्रभावित करते थे। कोर्ट ने कहा कि संसद की संशोधन शक्ति असीमित नहीं है।
इंदिरा नेहरू गांधी vs राज नारायण (1975): इमरजेंसी के दौरान चुनावी धांधली पर कोर्ट ने फैसला दिया, और संसद के 39वें संशोधन को आंशिक रूप से रद्द किया।
NJAC केस (2015): 99वां संशोधन (नेशनल ज्यूडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन) को असंवैधानिक घोषित किया गया, क्योंकि यह न्यायिक स्वतंत्रता (मूल संरचना का हिस्सा) को प्रभावित करता था।
रिसेंट उदाहरण: इलेक्टोरल बॉन्ड्स स्कीम (2024): सुप्रीम कोर्ट ने संसद द्वारा बनाई गई इस स्कीम को असंवैधानिक घोषित किया, क्योंकि यह सूचना के अधिकार और समानता को प्रभावित करती थी। यह दिखाता है कि कोर्ट संसद के कानूनों को रद्द कर सकता है।
संघीय सीमाएं: संसद राज्य सूचियों पर अतिक्रमण नहीं कर सकती। उदाहरण: एस.आर. बोम्मई केस (1994) में कोर्ट ने अनुच्छेद 356 (राष्ट्रपति शासन) के दुरुपयोग को रोका।
मूल संरचना सिद्धांत और संसदीय संप्रभुताकेशवानंद भारती मामले (1973) में सुप्रीम कोर्ट ने मूल संरचना सिद्धांत स्थापित किया। इस सिद्धांत के अनुसार:
संसद की संविधान संशोधन की शक्ति निरपेक्ष नहीं है।
संविधान की कुछ मूलभूत विशेषताएं अपरिवर्तनीय हैं ।
न्यायपालिका संवैधानिक संशोधनों की समीक्षा कर सकती है।
मूल संरचना के तत्वों में शामिल हैं: संविधान की सर्वोच्चता, कानून का शासन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, संघवाद, धर्मनिरपेक्षता, लोकतांत्रिक व्यवस्था आदि।
अतः भारतीय संसद सीमित संप्रभु है—यह शक्तिशाली है लेकिन संविधान और न्यायपालिका द्वारा नियंत्रित। यह व्यवस्था "चेक एंड बैलेंस" सुनिश्चित करती है, जो लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। ब्रिटिश मॉडल की तुलना में, भारत में यह अधिक सुरक्षित है, क्योंकि यह बहुमत की तानाशाही से बचाता है। हालांकि, रिसेंट बहसों में (जैसे वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ के बयान, 2023), कुछ लोग संसद को पूर्ण संप्रभु मानते हैं, लेकिन कोर्ट के फैसले इससे असहमत हैं। यह संतुलन भारत की विविधता और इतिहास को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त है, लेकिन कभी-कभी संसद और कोर्ट के बीच टकराव (जैसे NJAC) से चुनौतियां आती हैं। कुल मिलाकर, यह "संवैधानिक संप्रभुता" का बेहतरीन उदाहरण है।
2(a) Ans.-
भारतवर्ष के संविधान में निहित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की विवेचना
भारतीय संविधान के भाग IV (अनुच्छेद 36 से 51) में राज्य के नीति निर्देशक तत्व (Directive Principles of State Policy – DPSP) निहित हैं। ये तत्व राज्य (केंद्र और राज्य सरकारों) को नीति निर्माण के लिए दिशा-निर्देश प्रदान करते हैं, ताकि एक कल्याणकारी राज्य (Welfare State) की स्थापना हो सके। इनकी प्रेरणा मुख्य रूप से आयरलैंड के संविधान से ली गई है, लेकिन इन्हें भारतीय सामाजिक-आर्थिक संदर्भ में अनुकूलित किया गया है। DPSP गैर-न्यायोचित (non-justiciable) हैं, अर्थात् इनकी अवहेलना पर कोई अदालत में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, लेकिन ये राज्य की शासन व्यवस्था में मौलिक (fundamental) हैं। डॉ. बी.आर. आंबेडकर ने इन्हें “संविधान की आत्मा” कहा था, क्योंकि ये सामाजिक और आर्थिक न्याय की दिशा में राज्य को प्रेरित करते हैं।
प्राकृतिक रूप: नीति निर्देशक तत्व राज्य को कानून-निर्माण और शासन चलाने के लिए मार्गदर्शन देते हैं। ये तत्व कानून द्वारा न्यायालयों में प्रवर्तनीय नहीं हैं, लेकिन संवैधानिक रूप से राज्य को इन्हें लागू करने का निर्देश देते हैं।
संवैधानिक आधार: अनुच्छेद 37 के अनुसार, नीति निर्देशक तत्वों को किसी भी न्यायालय में लागू नहीं किया जा सकता, लेकिन वे राज्य के शासन में मौलिक माने जाते हैं।
DPSP की विवेचना निम्नलिखित बिंदुओं में की जा सकती है, जहां इन्हें उनकी प्रकृति के आधार पर वर्गीकृत किया गया है (हालांकि संविधान में औपचारिक वर्गीकरण नहीं है, लेकिन विद्वानों द्वारा ऐसा किया जाता है):
- सामाजिकवादी सिद्धांत (Socialist Principles)
इनका उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को कम करना तथा न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करना है।
अनुच्छेद 38: राज्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करेगा तथा असमानताओं को कम करेगा। यह कल्याणकारी राज्य की आधारशिला है।
अनुच्छेद 39: राज्य उत्पादन के साधनों का वितरण ऐसा करेगा कि संपदा का संकेंद्रण न हो (39A: समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता)। उदाहरण: भूमि सुधार कानून और बैंक राष्ट्रीयकरण (1970s) इसी से प्रेरित हैं।
अनुच्छेद 41: रोजगार, शिक्षा और बेरोजगारी की स्थिति में सहायता का अधिकार।
अनुच्छेद 42: कार्य की न्यायपूर्ण और मानवीय स्थितियां, प्रसूति सहायता।
अनुच्छेद 43: जीवनयापन योग्य मजदूरी, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग। (43A: श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी; 43B: सहकारी समितियों का प्रोत्साहन)।
अनुच्छेद 47: पोषण स्तर और स्वास्थ्य सुधार, मादक पेयों पर प्रतिबंध।
- गांधीवादी सिद्धांत (Gandhian Principles)
ये महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित हैं, जो ग्रामीण विकास और आत्मनिर्भरता पर जोर देते हैं।
अनुच्छेद 40: ग्राम पंचायतों का संगठन।
अनुच्छेद 43: कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन।
अनुच्छेद 46: अनुसूचित जातियों/जनजातियों और कमजोर वर्गों का शैक्षिक-आर्थिक उत्थान।
अनुच्छेद 47: स्वास्थ्य और पोषण सुधार।
अनुच्छेद 48: कृषि और पशुपालन का वैज्ञानिक संगठन, गौ-हत्या पर प्रतिबंध।
- उदारवादी-बौद्धिक सिद्धांत (Liberal-Intellectual Principles)
ये मानवाधिकार, शिक्षा और पर्यावरण पर केंद्रित हैं।
अनुच्छेद 44: समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code)।
अनुच्छेद 45: 6-14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा (2002 में अनुच्छेद 21A द्वारा मौलिक अधिकार बनाया गया)।
अनुच्छेद 48A: पर्यावरण संरक्षण और वन्यजीव सुरक्षा (42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया)।
अनुच्छेद 49: राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण।
अनुच्छेद 50: न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण।
अनुच्छेद 51: अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का प्रोत्साहन।
ये सिद्धांत संविधान सभा की बहसों से निकले हैं, जहां इन्हें मौलिक अधिकारों (Fundamental Rights) के पूरक के रूप में देखा गया। हालांकि, शुरू में इन्हें कम महत्व दिया गया, लेकिन समय के साथ संशोधनों (जैसे 42वां, 44वां) से नए सिद्धांत जोड़े गए।
विवेचना (Features)-
सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र का लक्ष्य: इनका मुख्य उद्देश्य ऐसे सामाजिक और आर्थिक हालात बनाना है, जहाँ सभी नागरिक एक अच्छा जीवन जी सकें और उन्हें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिले।
कल्याणकारी राज्य की स्थापना: ये सिद्धांत एक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को साकार करते हैं, जहाँ राज्य का मुख्य कार्य जनता का कल्याण सुनिश्चित करना होता है।
न्यायालय द्वारा अप्रवर्तनीय: ये सिद्धांत कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं हैं, यानी इन्हें अदालतों के माध्यम से लागू नहीं कराया जा सकता है।
सरकार के लिए मार्गदर्शक: ये तत्व सरकार के लिए नैतिक और नीति-निर्माण के मार्गदर्शक होते हैं, जो कानून और नीतियां बनाते समय इनका ध्यान रखती है।
सकारात्मक और नकारात्मक दायित्व: जहाँ मौलिक अधिकार राज्य पर नकारात्मक दायित्व (क्या नहीं करना है) थोपते हैं, वहीं नीति निर्देशक तत्व राज्य पर सकारात्मक दायित्व (क्या करना है) डालते हैं, जैसे सार्वजनिक भलाई के लिए काम करना।
राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का महत्व-
DPSP का महत्व भारतीय संविधान की संरचना और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में गहराई से जुड़ा है। ये न केवल राज्य की नीतियों को दिशा देते हैं, बल्कि एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना में सहायक हैं:-
कल्याणकारी राज्य की स्थापना: DPSP भारत को एक समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने का लक्ष्य रखते हैं। वे आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देते हैं, जहां मौलिक अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र सुनिश्चित करते हैं। उदाहरण: मनरेगा (MGNREGA) अनुच्छेद 41 से प्रेरित है, जो ग्रामीण रोजगार प्रदान करता है।
मौलिक अधिकारों के साथ सामंजस्य: हालांकि DPSP गैर-न्यायोचित हैं, लेकिन न्यायपालिका ने इन्हें मौलिक अधिकारों के साथ जोड़ा है। केशवानंद भारती केस (1973) में DPSP को संविधान की मूल संरचना का हिस्सा माना गया। मिनर्वा मिल्स केस (1980) में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मौलिक अधिकार और DPSP “संविधान के दो पहिए” हैं, और DPSP को लागू करने के लिए अधिकारों को सीमित किया जा सकता है।उदाहरण: ट्रिपल तलाक पर फैसला अनुच्छेद 44 (समान नागरिक संहिता) से प्रभावित था।
सामाजिक-आर्थिक न्याय: ये असमानताओं को दूर करने में महत्वपूर्ण हैं। भूमि सुधार, शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE), पर्यावरण कानून (जैसे वन संरक्षण अधिनियम) DPSP से निकले हैं। वे राज्य को कमजोर वर्गों (SC/ST, महिलाएं, बच्चे) के उत्थान के लिए बाध्य करते हैं।
नीति निर्माण में मार्गदर्शन: अनुच्छेद 37 कहता है कि DPSP राज्य की नीतियों में मौलिक हैं। संसद और राज्य विधानसभाएं इन्हें ध्यान में रखकर कानून बनाती हैं। उदाहरण: आधार योजना और जीएसटी DPSP के आर्थिक न्याय से जुड़े हैं।
न्यायिक व्याख्या और विकास: शुरू में गोलकनाथ केस (1967) में DPSP को मौलिक अधिकारों से नीचे रखा गया, लेकिन बाद के फैसलों (जैसे ओल्गा टेलिस केस, 1985) में इन्हें जीवन के अधिकार (अनुच्छेद 21) के साथ जोड़ा गया।इससे DPSP व्यावहारिक रूप से न्यायोचित हो गए हैं।
हालांकि, आलोचना यह है कि ये “कागजी वादे” हैं, क्योंकि इनका पूर्ण कार्यान्वयन नहीं हुआ (जैसे समान नागरिक संहिता)। फिर भी, DPSP संविधान की प्रगतिशीलता को दर्शाते हैं और भारत जैसे विकासशील देश में सामाजिक परिवर्तन के लिए आवश्यक हैं।
2(b) Ans.-
बिहार में प्राकृतिक संसाधन जैसे कोयला (झारखंड विभाजन से पहले अधिक थे, लेकिन अभी भी कुछ क्षेत्रों में), बॉक्साइट, चूना पत्थर, और गंगा की उपजाऊ घाटी मौजूद हैं, जो कृषि-आधारित और खनन-आधारित उद्योगों के लिए अनुकूल हैं। फिर भी, 2025 तक बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान मात्र 19% के आसपास है, जबकि राष्ट्रीय औसत 25-30% है।808375 2025-26 के लिए GSDP अनुमानित रूप से 10.97 लाख करोड़ रुपये (128.89 बिलियन डॉलर) है, जो 2015-16 से 11.42% की CAGR से बढ़ा है, लेकिन यह मुख्य रूप से सेवा क्षेत्र से प्रेरित है, न कि उद्योग से।
इसके कारण निम्न है -
1. कमजोर बुनियादी ढांचा (Weak Infrastructure)-
बिहार की औद्योगिक पिछड़ापन की जड़ में बुनियादी सुविधाओं की कमी है, जो निवेशकों को दूर रखती है। राज्य में सड़क घनत्व राष्ट्रीय औसत (2.1 किमी/100 वर्ग किमी) से कम है—केवल 1.5 किमी/100 वर्ग किमी।रेल नेटवर्क भी अपर्याप्त है, और हवाई संपर्क मुख्य रूप से पटना तक सीमित है। बाढ़-प्रभावित क्षेत्र (राज्य के 73% हिस्से) में उद्योग स्थापित करना चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि हर साल बाढ़ से 10-15 लाख करोड़ की क्षति होती है।
विशिष्ट उदाहरण: पूर्वांचल एक्सप्रेसवे (2023 में पूरा) ने कुछ सुधार किया, लेकिन ग्रामीण इलाकों में लॉजिस्टिक्स लागत 25-30% अधिक है।ccfbc6 बिजली की उपलब्धता में 2005 के बाद सुधार हुआ (अब 24 घंटे की आपूर्ति का दावा), लेकिन औद्योगिक उपयोग के लिए ब्लैकआउट अभी भी सामान्य हैं, जिससे उत्पादन प्रभावित होता है। 2025 की एक रिपोर्ट के अनुसार, बिहार में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत राष्ट्रीय औसत से 50% कम है।377e54 जल प्रबंधन की कमी से सिंचाई और औद्योगिक जल आपूर्ति प्रभावित होती है, जैसे कोसी नदी की बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में।
2. राजनीतिक अस्थिरता और भ्रष्टाचार (Political Instability and Corruption)-
बिहार का राजनीतिक इतिहास (विशेष रूप से 1970-2000 का दौर) अस्थिरता से भरा है, जिसमें जाति-आधारित हिंसा, लगातार सरकार बदलाव और "जंगल राज" शामिल हैं। यह निवेशकों के विश्वास को तोड़ता है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के अनुसार, बिहार भ्रष्टाचार सूचकांक में ऊपरी स्थान पर है, जहां लाइसेंस, भूमि अधिग्रहण और सब्सिडी में रिश्वतखोरी आम है।61201e
विशिष्ट उदाहरण: 2006 में नीतीश कुमार सरकार ने औद्योगिक नीति लाई, लेकिन 2025 तक भी यह प्रभावी नहीं हुई—एमओयू साइन हुए, लेकिन केवल 20-30% परियोजनाएं शुरू हुईं।a0d9e5 ऐतिहासिक रूप से, केंद्र की फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी (1952-1991) ने बिहार के खनिजों को सस्ता बनाकर अन्य राज्यों (जैसे पश्चिमी भारत) में उद्योग स्थानांतरित कर दिया, जिससे स्थानीय विकास रुक गया।432732 2000 में झारखंड विभाजन ने बिहार से 80% खनिज संसाधन छीन लिए, जो पहले स्टील और कोयला उद्योगों का आधार थे। 2025 के बजट में औद्योगिक पार्कों के लिए 5000 करोड़ आवंटित किए गए, लेकिन भ्रष्टाचार से केवल 25% कार्यान्वयन हुआ।470c50
3. कौशल विकास और मानव संसाधन की कमी (Lack of Skilled Manpower)-
बिहार की जनसंख्या 13 करोड़ से अधिक है, लेकिन साक्षरता दर 70% के आसपास है, और कौशल प्रशिक्षण की कमी से कुशल श्रमिक उपलब्ध नहीं। 2025 की रिपोर्ट्स के अनुसार, 60% युवा औद्योगिक कौशल से वंचित हैं, जिससे कंपनियां ट्रेनिंग पर अतिरिक्त खर्च करती हैं।9c2785 ब्रेन ड्रेन बड़ा मुद्दा है—हर साल 20-25 लाख युवा अन्य राज्यों में मजदूरी या नौकरी के लिए पलायन करते हैं।
विशिष्ट उदाहरण: आईटीआई और पॉलिटेक्निक संस्थानों की संख्या कम है (केवल 200 से अधिक), जबकि गुजरात में 500+ हैं।61f3e0 स्किल इंडिया कार्यक्रम ने कुछ सुधार किया, लेकिन 2025 तक केवल 10% युवाओं को औद्योगिक प्रशिक्षण मिला। सरकारी नौकरियों की भीड़ (जैसे BPSC परीक्षाओं में लाखों आवेदन) निजी क्षेत्र को हतोत्साहित करती है, क्योंकि युवा स्थिरता की तलाश में हैं।
4. निवेश और नीतिगत बाधाएं (Low Investment and Policy Hurdles)-
बिहार में एफडीआई राष्ट्रीय औसत से 60% कम है—2024-25 में मात्र 500 करोड़ डॉलर।5c47f6 नीतियां जैसे बिहार बिजनेस कनेक्ट (2023) और इंडस्ट्रियल पॉलिसी (2022) आकर्षक हैं (टैक्स छूट, सब्सिडी), लेकिन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में बिहार 20वें स्थान पर है।
विशिष्ट उदाहरण: 2023 के ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 1 लाख करोड़ के एमओयू साइन हुए, लेकिन 2025 तक केवल 15% लागू हुए, मुख्य रूप से भूमि और पर्यावरण क्लीयरेंस में देरी से।1c090a कृषि पर 50% निर्भरता उद्योगों को बढ़ावा नहीं दे पाती, और छोटे-मध्यम उद्यम (MSME) में भी कमी है।
5. आर्थिक असमानता और गरीबी का चक्र (Cycle of Inequality and Poverty)-
बिहार में जिनी कोएफिशिएंट (आय असमानता) 0.38 है, जो भारत में सबसे अधिक है।21a29b गरीबी दर 23% है, और प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से 50% कम (लगभग 50,000 रुपये वार्षिक)। यह उपभोक्ता बाजार को छोटा बनाता है, जो बड़े उद्योगों को आकर्षित नहीं करता।
विशिष्ट उदाहरण: ग्रामीण-शहरी विभाजन से सामाजिक तनाव बढ़ता है, और 2025 की रिपोर्ट्स बताती हैं कि असमानता विकास को 20-30% धीमा करती है।b36764 ऐतिहासिक रूप से, ब्रिटिश काल से ही बिहार कृषि-आधारित रहा, और स्वतंत्रता के बाद केंद्र की नीतियां (जैसे फ्रेट पॉलिसी) ने इसे और पिछड़ा बनाया।
6. प्राकृतिक आपदाओं और पर्यावरणीय चुनौतियां (Natural Disasters and Environmental Issues)-
वार्षिक बाढ़ (कोसी, गंडक नदियां) और सूखा संसाधनों को नष्ट करते हैं। 2024 की बाढ़ ने 5 लाख हेक्टेयर फसल नष्ट की, जो औद्योगिक कच्चे माल को प्रभावित करती है।
विशिष्ट उदाहरण: एनजीटी (नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल) के सख्त नियमों से खनन उद्योग रुका—2025 में कई खदानें बंद हुईं। पर्यावरण संरक्षण की जरूरत (जैसे वन कवर बढ़ाना) उद्योगों को सीमित करती है।
आँकड़ों से संकेत -
सक्रिय फैक्ट्रियों की संख्या 2013-14 में 3,132 से घटकर 2022-23 में 2,782 हुई—औद्योगिक आधार के सिमटने का संकेत।
ASI के अनुसार, विनिर्माण में बिहार का राष्ट्रीय GVA योगदान अत्यंत कम है; राज्य के औद्योगिक ठहराव और रोजगार सृजन पर नकारात्मक प्रभाव दिखता है।
निर्माण/विनिर्माण हिस्सेदारी में हाल के वर्षों में उतार-चढ़ाव और गिरावट दर्ज—द्वितीयक क्षेत्र की कमजोरी दर्शाती है।
निष्कर्ष और संभावित सुधार-
बिहार का औद्योगिक विकास धीमा होना ऐतिहासिक (फ्रेट पॉलिसी, विभाजन), संरचनात्मक (ढांचा, कौशल) और प्रशासनिक (भ्रष्टाचार, नीति कार्यान्वयन) कारणों का मिश्रण है। हालांकि, सकारात्मक बदलाव हो रहे हैं—2025 में औद्योगिक विकास कृषि को पीछे छोड़ चुका है, और GSDP में 15% की वृद्धि दर्ज हुई।
सुधार के लिए: बुनियादी ढांचे पर निवेश (जैसे अमृत भारत योजना), कौशल विकास (स्किल हब्स), पारदर्शी शासन (ई-गवर्नेंस), और निवेश प्रोत्साहन (टैक्स ब्रेक) आवश्यक हैं। यदि ये लागू हुए, तो बिहार के संसाधन (जैसे एग्रो-प्रोसेसिंग में) विकास का इंजन बन सकते हैं।
3(a) Ans.-
"विकास के लिए बढ़ती जनसंख्या एक प्रमुख बाधक है" यह कथन आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय विकास के संदर्भ में अक्सर चर्चा का विषय रहा है, विशेष रूप से विकासशील देशों जैसे भारत में। बढ़ती जनसंख्या को जहां एक ओर "जनसंख्या लाभांश" (demographic dividend) के रूप में देखा जाता है, वहीं दूसरी ओर यह संसाधनों पर अत्यधिक दबाव डालकर विकास की गति को धीमा कर सकती है। यहां मैं इस कथन की विवेचना करूंगा, जिसमें दोनों पक्षों—बाधक और संभावित लाभ—को शामिल किया जाएगा। विवेचना मुख्य रूप से भारत के संदर्भ में होगी, जहां 2025 में जनसंख्या लगभग 1.46 अरब है और वृद्धि दर लगभग 1% है, लेकिन कुल जनसंख्या अभी भी तेजी से बढ़ रही है। यह विवेचना आर्थिक सिद्धांतों (जैसे माल्थसियन थ्योरी), वर्तमान आंकड़ों और रिपोर्टों पर आधारित है।
1. बढ़ती जनसंख्या को बाधक मानने के कारण -
बढ़ती जनसंख्या विकास के लिए प्रमुख बाधक सिद्ध होती है क्योंकि यह सीमित संसाधनों को तेजी से खपत करती है, जिससे आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय असंतुलन पैदा होता है। मुख्य कारण निम्नलिखित हैं:
संसाधनों पर अत्यधिक दबाव: बढ़ती जनसंख्या प्राकृतिक संसाधनों जैसे जल, भूमि और ऊर्जा पर बोझ बढ़ाती है। भारत में, जहां जनसंख्या 1.4 अरब से अधिक है, यह जल संकट, वनों की कटाई, प्रदूषण और मिट्टी की क्षरण को बढ़ावा देती है। उदाहरण के लिए, जनसंख्या वृद्धि से प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक उपभोग होता है, जिससे जल की कमी और प्रदूषण बढ़ता है। ग्लोबल कार्बन बजट रिपोर्ट 2022 के अनुसार, भारत की उत्सर्जन दर 6% बढ़ने की संभावना है, जो पर्यावरणीय विकास को बाधित करती है। इससे सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) जैसे जलवायु परिवर्तन से निपटना कठिन हो जाता है।
आर्थिक विकास पर प्रभाव: तेज जनसंख्या वृद्धि रोजगार सृजन को पीछे छोड़ देती है, जिससे बेरोजगारी, गरीबी और असमानता बढ़ती है। माल्थसियन सिद्धांत के अनुसार, जनसंख्या ज्यामितीय अनुपात में बढ़ती है जबकि संसाधन अंकगणितीय, जिससे प्रति व्यक्ति आय कम होती है। भारत में, उच्च जनसंख्या वृद्धि से रोजगार की कमी होती है, पूंजी निर्माण दर कम होती है और निवेश की आवश्यकता बढ़ जाती है।f6c2a9 परिणामस्वरूप, राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर प्रभावित होती है, क्योंकि बढ़ती जनसंख्या से बचत और निवेश की क्षमता कम हो जाती है। 2025 में, भारत की आर्थिक वृद्धि दर तेज है (लगभग 6-7%), लेकिन जनसंख्या दबाव से क्षेत्रीय असमानताएं बढ़ रही हैं, जैसे उत्तर बनाम दक्षिण भारत।
सामाजिक सेवाओं पर बोझ: शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास जैसी बुनियादी सेवाओं पर दबाव बढ़ता है। भारत में, जनसंख्या वृद्धि से गरीबी और असमानता बढ़ती है, क्योंकि संसाधनों का वितरण असमान होता है।उदाहरण के लिए, जनसंख्या वृद्धि से रोजगार अवसरों की कमी होती है, जो आर्थिक विकास को बाधित करती है। UNFPA की 2025 रिपोर्ट के अनुसार, कई व्यक्ति अपनी प्रजनन लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाते, जो अप्रत्यक्ष रूप से विकास को प्रभावित करता है।
पर्यावरणीय और शहरीकरण की चुनौतियां: शहरीकरण बढ़ने से स्लम्स, प्रदूषण और आधारभूत संरचना पर दबाव पड़ता है। भारत में, जनसंख्या वृद्धि से जल आवश्यकताएं बढ़ती हैं, लेकिन प्रबंधन की कमी से संकट उत्पन्न होता है। यह पर्यावरणीय क्षति को बढ़ावा देती है, जो दीर्घकालिक विकास के लिए बाधक है।
प्रशासनिक और नियोजन संबंधी चुनौतियाँ:- बढ़ती जनसंख्या के समुचित प्रबंधन के लिए प्रभावी योजनाएँ और नीतियाँ बनानी होती हैं, पर:सरकारी बजट, मानव संसाधन और संस्थागत क्षमताओं में कमी के कारण योजनाएँ अधूरा रह जाती हैं।जनसंख्या-नियंत्रण, परिवार नियोजन और जन–स्वास्थ्य अभियानों का कार्यान्वयन असंगठित तथा अपर्याप्त रहता है।ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में असंतुलित विकास से क्षेत्रीय विषमताएँ तीव्र होती हैं, जिससे सामाजिक असंतोष बढ़ता है।
बढ़ती जनसंख्या का सकारात्मक पक्ष: जनसंख्या लाभांश -
हालांकि कथन में इसे बाधक कहा गया है, लेकिन विवेचना में संतुलन के लिए सकारात्मक पक्ष को भी देखना जरूरी है। यदि जनसंख्या युवा और कुशल हो, तो यह विकास का इंजन बन सकती है:-
कार्यशील आयु वर्ग का लाभ: भारत में, कुल प्रजनन दर (TFR) 1992-93 में 3.4 से घटकर 2019-21 में 2.0 हो गई है, जिससे कार्यशील आयु (15-64 वर्ष) की आबादी बढ़ रही है। यह डेमोग्राफिक डिविडेंड प्रदान कर सकती है, जहां आर्थिक वृद्धि बढ़ती है। उदाहरण के लिए, भारत की आर्थिक वृद्धि में मध्यम वर्ग की वृद्धि से योगदान अपेक्षित है। IIASA की 2025 स्टडी के अनुसार, भारत की सामाजिक-आर्थिक क्षमता चीन से आगे निकल सकती है यदि मानव पूंजी में निवेश हो।
आर्थिक अवसर: बड़ी जनसंख्या बाजार और श्रम शक्ति प्रदान करती है, जो डिजिटल अर्थव्यवस्था और व्यापार में लाभ देती है।हालांकि, यह लाभ तभी मिलता है जब शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार नीतियां मजबूत हों।अन्यथा, यह बाधक बन जाती है।
नीतिगत संदर्भ: दक्षिणी राज्य जैसे तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश ने जनसंख्या नियंत्रण से लाभ उठाया है, लेकिन उत्तरी राज्यों में असमान वृद्धि से राजनीतिक चुनौतियां हैं।08b80f 2025 में जनगणना और सीट वितरण से यह मुद्दा और उभरेगा।
बढ़ती आबादी की प्रमुख चुनौतियाँ-
स्थिर जनसंख्या : स्थिर जनसंख्या वृद्धि के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये यह आवश्यक है कि सर्वप्रथम प्रजनन दर में कमी की जाए। यह बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में काफी अधिक है, जो एक बड़ी चुनौती बनी हुई है।
जीवन की गुणवत्ता : नागरिकों को न्यूनतम जीवन गुणवत्ता प्रदान करने के लिये शिक्षा और स्वास्थ प्रणाली के विकास पर निवेश करना होगा, अनाजों और खाद्यान्नों का अधिक-से-अधिक उत्पादन करना होगा, लोगों को रहने के लिये घर देना होगा, स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति बढ़ानी होगी एवं सड़क, परिवहन और विद्युत उत्पादन तथा वितरण जैसे बुनियादी ढाँचे को मज़बूत बनाने पर काम करना होगा।
नागरिकों की मूलभूत ज़रूरतों को पूरा करने और बढ़ती आबादी को सामाजिक बुनियादी ढाँचा प्रदान करके समायोजित करने के लिये भारत को अधिक खर्च करने की आवश्यकता है और इसके लिये भारत को सभी संभावित माध्यमों से अपने संसाधन बढ़ाने होंगे।
जनसांख्यिकीय विभाजन : बढ़ती जनसंख्या का लाभ उठाने के लिये भारत को मानव पूंजी का मज़बूत आधार बनाना होगा ताकि वे लोग देश की अर्थव्यवस्था में अपना महत्त्वपूर्ण योगदान दे सकें, लेकिन भारत की कम साक्षरता दर (लगभग 74 प्रतिशत) इस मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है।
सतत शहरी विकास : वर्ष 2050 तक देश की शहरी आबादी 87.7 मिलियन तक हो जाएगी, जिसके चलते शहरी सुविधाओं में सुधार और सभी को आवास उपलब्ध कराने की चुनौती होगी और इन सभी के लिये पर्यावरण को भी मद्देनज़र रखना ज़रूरी होगा।
असमान आय वितरण : आय का असमान वितरण और लोगों के बीच बढ़ती असमानता अत्यधिक जनसंख्या के नकारात्मक परिणामों के रूप में सामने आएगा।
क्या किया जा सकता है -
भविष्य में सभी के लिये खाद्यान्न सुनिश्चित करने हेतु यह महत्त्वपूर्ण है कि कृषि को लाभकारी बनाया जाए और खाद्यान्नों की कीमतों में बहुत अधिक परिवर्तन न हो अर्थात् कमोबेश वे स्थिर रहें।
न्यूनतम मासिक आय (Universal Basic Income) को सुरक्षा कवच के रूप में लागू करना भी बड़ी संख्या में बेरोज़गार युवाओं को रोज़गार के अवसर प्रदान करने में मदद करेगा।
वन और जल संसाधनों का उचित प्रबंधन करना होगा ताकि उन्हें सतत इस्तेमाल के लिये बचाया जा सके।
सतत विकास लक्ष्यों (Sustainable Development Goals) की प्राप्ति किसी भी नीति निर्माण का केंद्र बिंदु होना चाहिये।
अपेक्षाकृत कम आय और घनी आबादी वाले भारत के उत्तरी राज्यों को दक्षिणी राज्यों से सीख लेते हुए महिलाओं की साक्षरता, स्वास्थ्य और कार्यबल में भागीदारी जैसे कुछ महत्त्वपूर्ण निर्णय लेने होंगे।
जनसंख्या में कमी, अधिकतम समानता, बेहतर पोषण, सार्वभौमिक शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं जैसे सभी लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये सरकारों और मज़बूत नागरिक सामाजिक संस्थाओं के बीच बेहतर सामंजस्य की आवश्यकता है।
बढ़ती जीवन प्रत्याशा (Life Expectancy) और किशोरों की बढ़ती आबादी सेवा के नए क्षेत्रों में रोज़गार के अवसर तलाशने में मदद करेगी।
AMRUT, स्मार्ट सिटी, मेक इन इंडिया और सतत विकास लक्ष्य जैसी योजनाएँ निश्चित रूप से देश की सामाजिक आधारिक संरचना को बढ़ाने में सहायता करेंगी।
आगे की राह (अन्य संभावित उपाय)-
भारत को स्वास्थ्य क्षेत्र में खर्च बढ़ाना होगा। वर्तमान में यह GDP का केवल 1.3% है। कुल स्वास्थ्य बजट में से परिवार कल्याण (नियोजन) पर मात्र 4% ही खर्च होता है और इसमें से भी केवल 1.5% जन्म में अंतर रखने के उपायों पर खर्च किया जाता है।
बुजुर्ग होती आबादी के लिये निवेश को बढ़ाना होगा, क्योंकि वर्ष 2050 तक भारत में बुजुर्गों की आबादी वर्तमान से लगभग 10 गुना अधिक तक बढ़ सकती है।
शिक्षा बहुत महत्त्वपूर्ण है, न केवल महिलाओं को सशक्त बनाने के लिये बल्कि प्रजनन क्षमता में गिरावट के लिये भी। बेहतर शिक्षा महिलाओं को परिवार नियोजन के लिये सही निर्णय लेने में मदद करेगी।
जब तक महिलाएं कार्यबल का हिस्सा नहीं होंगी, कोई भी समाज प्रजनन दर में कमी नहीं ला सकता। ऐसे में प्रभावी नीतियाँ बनाकर कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी में कमी को रोकना चाहिये।
ऐसे कुछ क्षेत्रों पर विशेष ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है जो सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं। 140 ऐसे ज़िलों की पहचान करना इस दिशा में सरकार द्वारा उठाया गया सही कदम है।
देश में लैंगिक अनुपात में गिरावट और लड़कियों के प्रति भेदभाव काफी अधिक है। इस मुद्दे पर ध्यान देना बेहद ज़रूरी है ताकि लोग लड़का होने की उम्मीद में अधिक संख्या में बच्चों को जन्म न दें।
परिवार नियोजन के साथ जोड़कर भारत कई सहस्राब्दी विकास लक्ष्य हासिल कर सकता है। मातृ मृत्यु दर और बाल मृत्यु दर कम करने के लिये परिवार नियोजन एक प्रोत्साहक और निवारक उपाय है।
जनसंख्या वृद्धि के मुद्दे को न केवल राष्ट्रीय दृष्टिकोण से बल्कि राज्य के दृष्टिकोण से भी देखना महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि विभिन्न राज्यों को जनसंख्या वृद्धि को थामने के लिये अलग-अलग कदम उठाने हेतु प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।
निष्कर्ष
कुल मिलाकर, बढ़ती जनसंख्या विकास के लिए प्रमुख बाधक है, क्योंकि यह संसाधनों, आर्थिक बचत और सामाजिक सेवाओं पर दबाव डालती है, जैसा कि भारत के संदर्भ में देखा जा सकता है जहां ओवरपॉपुलेशन आर्थिक विकास की राह में बाधा है। हालांकि, यदि नीतियां जैसे परिवार नियोजन, शिक्षा निवेश और सतत विकास पर फोकस करें, तो यह लाभ में बदल सकती है। भारत में, जहां जनसंख्या वृद्धि अब धीमी हो रही है लेकिन मोमेंटम से जारी है, समग्र दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है।विकासशील देशों के लिए, जनसंख्या प्रबंधन आर्थिक सफलता की कुंजी है, अन्यथा यह "जनसंख्या विस्फोट" बनकर विकास को रोक सकती है।
3(b) Ans.-
जिला योजना (District Planning) भारत में विकेंद्रीकृत योजना प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो स्थानीय स्तर पर विकास को सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन की गई है। यह जिला स्तर पर एक एकीकृत विकास योजना तैयार करने की प्रक्रिया है, जिसमें उपलब्ध संसाधनों (प्राकृतिक, मानवीय और वित्तीय) को ध्यान में रखते हुए स्थानीय सरकारों (पंचायतें, नगरपालिकाएं और जिला परिषद) द्वारा योजनाएं बनाई जाती हैं।इसका मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय और राज्य स्तर की नीतियों को स्थानीय जरूरतों के साथ जोड़ना है, ताकि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों का संतुलित विकास हो सके। संविधान के 73वें और 74वें संशोधन (1992) के बाद यह प्रक्रिया मजबूत हुई, जिसके तहत अनुच्छेद 243ZD जिला योजना समिति (District Planning Committee – DPC) का गठन अनिवार्य किया गया। DPC का कार्य ग्रामीण और शहरी योजनाओं को एकीकृत करके ड्राफ्ट डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्लान तैयार करना है।
जिला योजना समिति के सदस्यों की संख्या हर राज्य में अलग-अलग हो सकती है, क्योंकि यह राज्य के नियमों और जिले की आबादी के अनुपात पर निर्भर करती है। हालांकि, कई राज्यों में सदस्य संख्या निश्चित नहीं होती है और समिति में जिला परिषद के अध्यक्ष, नगरपालिका के महापौर/अध्यक्ष और ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के निर्वाचित सदस्यों का प्रतिनिधित्व शामिल होता है।
सदस्यता के आधार:
जिला परिषद के अध्यक्ष: समिति के पदेन अध्यक्ष हो सकते हैं।
महापौर/अध्यक्ष: जिला मुख्यालय पर स्थित किसी भी नगर पालिका के महापौर या अध्यक्ष शामिल हो सकते हैं।
निर्वाचित सदस्य: कम से कम 4/5 सदस्य जिले के ग्रामीण क्षेत्रों (जिला परिषद के निर्वाचित सदस्यों) और शहरी क्षेत्रों (नगर पंचायतों और नगर निगमों के पार्षदों) के बीच आबादी के अनुपात में चुने जाते हैं।
उदाहरण: केरल में जिला योजना समिति में 15 सदस्य होते हैं, जिनकी अध्यक्षता जिला पंचायत अध्यक्ष करते हैं और जिला कलेक्टर सदस्य सचिव के रूप में कार्य करते हैं।
इसमें निम्नलिखित बातें शामिल होती हैं:-
विश्लेषण: जिले की वर्तमान स्थिति, उसकी ताकत, कमजोरियों, अवसरों और चुनौतियों का विश्लेषण किया जाता है।
उद्देश्य निर्धारण: जिले के विकास के लिए स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं।
कार्यान्वयन रणनीतियाँ: इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कार्य-योजनाएं और संसाधन जुटाने के तरीके बताए जाते हैं।
समन्वय: यह योजना जिले में पंचायतों और नगर पालिकाओं द्वारा तैयार की गई योजनाओं का एकीकरण करती है, जिससे पूरे जिले का एक एकीकृत विकास हो सके।
जिला योजना का अर्थ मुख्य रूप से निम्नलिखित है:
एकीकृत दृष्टिकोण: यह गांव, ब्लॉक, जिला और शहर स्तर की योजनाओं को एक साथ जोड़ती है, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, बुनियादी ढांचा, कृषि, पर्यावरण और आर्थिक विकास जैसे क्षेत्र शामिल होते हैं। उदाहरण के लिए, 11वीं पंचवर्षीय योजना में इसे समावेशी विकास (Inclusive Growth) का प्रमुख साधन माना गया।
भागीदारीपूर्ण प्रक्रिया: स्थानीय निवासी, निर्वाचित प्रतिनिधि, एनजीओ और विशेषज्ञों की भागीदारी पर जोर, ताकि योजना नीचे से ऊपर (Bottom-Up) बने।
संसाधन-आधारित: उपलब्ध फंड्स (केंद्र, राज्य, स्थानीय राजस्व) का मैपिंग और उपयोग, साथ ही जीआईएस (Geographical Information System) जैसे उपकरणों से डेटा विश्लेषण।
दीर्घकालिक विजन: आमतौर पर 15-20 वर्ष की दृष्टि और 5 वर्षीय परिप्रेक्ष्य योजना, जिसमें वार्षिक योजनाएं शामिल होती हैं।
यह प्रक्रिया भारत के संघीय ढांचे में महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह केंद्रीकृत योजना की सीमाओं को दूर करके स्थानीय आवश्यकताओं (जैसे पिछड़े क्षेत्रों में बाढ़ प्रबंधन या स्वास्थ्य सेवाएं) पर फोकस करती है। हालांकि, कई राज्यों में इसका पूर्ण कार्यान्वयन अभी भी चुनौतीपूर्ण है।
जिला योजना के सफल होने की शर्तें-
जिला योजना की सफलता कई कारकों पर निर्भर करती है, क्योंकि यह एक जटिल, बहु-हितधारक प्रक्रिया है। भारत में कई प्रयासों (जैसे राज्यों में DPC का गठन) के बावजूद, कमजोर क्रियान्वयन के कारण असफलताएं देखी गई हैं। सफलता की प्रमुख शर्तें निम्नलिखित हैं, जो विभिन्न अध्ययनों और रिपोर्टों से निकली हैं:
मजबूत संस्थागत ढांचा और विकेंद्रीकरण: DPC का प्रभावी गठन और कार्य आवश्यक है, जिसमें निर्वाचित सदस्यों की बहुलता हो। राज्य सरकारों द्वारा शक्तियों का हस्तांतरण (Functions, Funds, Functionaries – 3Fs) महत्वपूर्ण है। उदाहरण: जहां DPC को पर्याप्त अधिकार नहीं दिए जाते, योजना असफल हो जाती है।सफलता के लिए, राज्य स्तर पर स्पष्ट दिशानिर्देश और कानूनी समर्थन जरूरी है।
भागीदारी और क्षमता निर्माण: स्थानीय समुदाय, महिलाओं, अल्पसंख्यकों और कमजोर वर्गों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना। ग्राम सभाओं, वार्ड समितियों और कार्यशालाओं के माध्यम से फीडबैक लेना। इसके लिए क्षमता निर्माण (ट्रेनिंग) आवश्यक है, ताकि प्रतिनिधि योजना प्रक्रिया समझ सकें। असफलता का एक कारण: भागीदारी की कमी से योजनाएं अवास्तविक हो जाती हैं।
संसाधनों का प्रभावी प्रबंधन: वित्तीय संसाधनों का सटीक मैपिंग (केंद्र/राज्य अनुदान, स्थानीय राजस्व) और पारदर्शी आवंटन। अनटाइड फंड्स का उपयोग प्राथमिकताओं के लिए। उदाहरण: PlanPlus जैसे सॉफ्टवेयर से डुप्लीकेशन रोकना। कमी होने पर योजना विफल हो जाती है।
डेटा-आधारित और तकनीकी समर्थन: बेसलाइन डेटा का संग्रह (जनसांख्यिकी, इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स) और जीआईएस, डेवलपमेंट रडार जैसे उपकरणों का उपयोग। पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन (EIA) शामिल करना। सफलता के लिए, डेटा की उपलब्धता और विश्लेषण क्षमता जरूरी है।
समन्वय और एकीकरण: रूरल-अर्बन, सेक्टर-वाइज (स्वास्थ्य, शिक्षा) और लाइन डिपार्टमेंट्स के बीच समन्वय। DPC द्वारा योजनाओं का कंसोलिडेशन। असफलता का कारण: ओवरलैप या असंगति।
निगरानी, मूल्यांकन और सामाजिक ऑडिट: निरंतर मॉनिटरिंग सिस्टम और सोशल ऑडिट से पारदर्शिता। वार्षिक समीक्षा और फीडबैक लूप। स्पष्ट लक्ष्य सेटिंग और प्रोग्राम मैनेजमेंट सफलता की कुंजी है।
राजनीतिक इच्छाशक्ति और समयबद्धता: राज्य और केंद्र सरकारों की प्रतिबद्धता, साथ ही समय पर कार्यशालाएं और फाइनलाइजेशन। राजनीतिक हस्तक्षेप की कमी और सतत फॉलो-अप।
ये शर्तें पूरी होने पर जिला योजना समावेशी विकास सुनिश्चित कर सकती है, जैसा कि कुछ जिलों (जैसे कोल्लम, जयपुर) में देखा गया।अन्यथा, यह केवल कागजी प्रक्रिया बनकर रह जाती है।
1 Ans.-
- What is the meaning of Parliamentary Sovereignty? Do you consider the Indian Parliament as sovereign, non-sovereign, or both? Give your views.
Parliamentary sovereignty is a political and constitutional concept primarily associated with the British constitutional system. Its basic meaning is that Parliament (or the legislature) represents the supreme power of the state, and no other institution (such as the judiciary or executive) can challenge the laws made by it.
A.V. Dicey defined it in three main principles:
Parliament can make any law: Parliament has full freedom to make laws on any subject, no matter how unusual or controversial. Example: In Britain, through the “Parliament Act” of 1949, Parliament limited the powers of the House of Lords, establishing the primacy of the House of Commons. This shows that Parliament can change its own powers.
A previous Parliament cannot bind a subsequent one: No Parliament can bind its successor. Example: In Britain, the “Septennial Act” of 1716 extended Parliament’s term from 3 to 7 years, but it was later changed. More recently, during Brexit (after the 2016 referendum), Parliament made laws to exit the European Union, overriding previous treaties.
The judiciary cannot question the validity of Parliament’s laws: Courts can only interpret laws, not declare them unconstitutional. Example: In Britain’s “Factortame Case” (1990), although there was debate over Parliament’s power due to European laws, the fundamental principle remained. However, in modern times, the Human Rights Act (1998) and the influence of the European Union have raised questions about its absoluteness, but Britain still has no written constitution, so Parliament remains supreme.
This concept appears in different forms in other countries. For example, in New Zealand and Israel, Parliament is sovereign due to unwritten constitutions, while in countries like the United States and Germany, the constitution is supreme, and courts can strike down laws. In India, this concept came from British influence but is limited due to the written constitution.
Example of British Parliamentary Sovereignty
The most prominent example of parliamentary sovereignty is the Parliament of the United Kingdom. According to British jurist A.V. Dicey, the three main features of British parliamentary sovereignty are:
Parliament can make, amend, or repeal any law.
Constitutional laws can be made like ordinary laws.
The judiciary cannot declare Parliament’s laws unconstitutional.
Position of the Indian Parliament and Sovereignty-
The Indian Parliament cannot be considered a fully sovereign body because it is subject to the provisions of the Constitution. Unlike the British Parliament, in India, the Constitution is supreme, not Parliament.
Limitations on the Sovereignty of the Indian Parliament-
Written Constitution: India’s Constitution is a written document that imposes limits on all branches of the state. Parliament cannot be above this written document.
Judicial Review: In India, the judiciary can review laws made by Parliament and declare them void if they are contrary to the Constitution.
Federal System: Under the Seventh Schedule of the Constitution, there is a division of powers between the Center and the States. Parliament can only make laws on subjects in the Union List and Concurrent List.
Fundamental Rights: Under Article 13, any law that violates fundamental rights is considered void.
Limited Power to Amend the Constitution: According to the Basic Structure Doctrine established in the Kesavananda Bharati case (1973), Parliament cannot destroy the basic structure of the Constitution.
Indian Parliament: Expansion on the Sovereign Aspect
The Indian Parliament can be considered sovereign in some senses because the Constitution grants it broad powers. It is inspired by the British model but adapted to the Indian context. Main points:
Legislative Powers: Under Articles 245-246, Parliament can make laws on the Union and Concurrent Lists. Example: Through the GST Act (2017), Parliament made a major change in the tax system, integrating the powers of the states and the center. This demonstrates Parliament’s ability to implement economic policies at the national level.
Power to Amend the Constitution: Article 368 allows Parliament to amend the Constitution. Specific examples:
44th Amendment (1978): After the Emergency, the right to property was removed from fundamental rights and placed in the Directive Principles. This shows Parliament affecting fundamental rights, which is evidence of its sovereignty.
42nd Amendment (1976): During the Emergency, Parliament made major changes to the Constitution, such as the power to suspend fundamental rights and limit judicial review. Although partially repealed later, it shows how far Parliament can go.
Abrogation of Article 370 (2019): Parliament revoked the article giving special status to Jammu and Kashmir and divided the state into two Union Territories. In 2023, the Supreme Court upheld it as valid, strengthening Parliament’s sovereignty, as the Court said it fits within the constitutional framework.
Control over the Executive: Parliament forms and dissolves governments. Example: In 1991, the P.V. Narasimha Rao government, with Parliament’s support, implemented economic reforms that changed the country’s direction.
Indian Parliament: Expansion on the Non-Sovereign Aspect
In India, the Constitution is supreme, so Parliament’s power is limited. The judiciary (Supreme Court) can review Parliament’s actions. Main points:
Supremacy of the Constitution: Under Article 13, no law can be contrary to fundamental rights. Example: In the Shayara Bano case (2017), triple talaq was declared unconstitutional, even though Parliament later made a law.
Basic Structure Doctrine: This is the biggest limitation on Parliament. Specific examples:
Golaknath Case (1967): The Supreme Court said Parliament cannot amend fundamental rights. This was the first major attack on Parliament’s sovereignty.
Kesavananda Bharati Case (1973): The Court established the Basic Structure Doctrine, which includes federal structure, secularism, judicial review, etc. Example: The 24th Amendment was challenged, and the Court said Parliament cannot change the basic structure.
Minerva Mills Case (1980): Parts of the 42nd Amendment were struck down because they affected the basic structure (e.g., fundamental rights vs. Directive Principles). The Court said Parliament’s amendment power is not unlimited.
Indira Nehru Gandhi vs. Raj Narain (1975): During the Emergency, the Court ruled on election rigging, and partially struck down the 39th Amendment.
NJAC Case (2015): The 99th Amendment (National Judicial Appointments Commission) was declared unconstitutional because it affected judicial independence (part of the basic structure).
Recent Example: Electoral Bonds Scheme (2024): The Supreme Court declared the scheme created by Parliament unconstitutional because it affected the right to information and equality. This shows that the Court can strike down Parliament’s laws.
Federal Limitations: Parliament cannot encroach on state lists. Example: In the S.R. Bommai case (1994), the Court stopped the misuse of Article 356 (President’s Rule).
Basic Structure Doctrine and Parliamentary Sovereignty
In the Kesavananda Bharati case (1973), the Supreme Court established the Basic Structure Doctrine. According to this doctrine:
Parliament’s power to amend the Constitution is not absolute.
Some fundamental features of the Constitution are unalterable.
The judiciary can review constitutional amendments.
Elements of the basic structure include: Supremacy of the Constitution, rule of law, independence of the judiciary, federalism, secularism, democratic system, etc.
Thus, the Indian Parliament is limited sovereign—it is powerful but controlled by the Constitution and the judiciary. This system ensures “checks and balances,” which is essential for democracy. Compared to the British model, it is more secure in India, as it protects against majority dictatorship. However, in recent debates (such as Vice President Jagdeep Dhankhar’s statement in 2023), some people consider Parliament fully sovereign, but court decisions disagree. This balance is appropriate considering India’s diversity and history, but sometimes conflicts between Parliament and the Court (like NJAC) pose challenges. Overall, it is an excellent example of “constitutional sovereignty.”
2(a) Ans.-
Discussion of the Directive Principles of State Policy Embedded in the Constitution of India
The Directive Principles of State Policy (DPSP) are embedded in Part IV (Articles 36 to 51) of the Indian Constitution. These principles provide guidelines to the state (central and state governments) for policy formulation to establish a welfare state. Their inspiration is mainly drawn from the Irish Constitution, but they have been adapted to the Indian socio-economic context. DPSP are non-justiciable, meaning no court case can be filed for their violation, but they are fundamental in the governance system of the state. Dr. B.R. Ambedkar called them the “soul of the Constitution” because they inspire the state towards social and economic justice.
Natural Form: The Directive Principles provide guidance to the state for law-making and running the administration. These principles are not enforceable in courts by law, but constitutionally, they direct the state to implement them.
Constitutional Basis: According to Article 37, the Directive Principles cannot be enforced in any court, but they are considered fundamental in the governance of the state.
The discussion of DPSP can be done in the following points, where they are classified based on their nature (although there is no formal classification in the Constitution, scholars do so):
- Socialist Principles
Their objective is to reduce social and economic inequalities and establish a just society.
Article 38: The state shall ensure social, economic, and political justice and reduce inequalities. This is the foundation of a welfare state.
Article 39: The state shall distribute the means of production in such a way that wealth is not concentrated (39A: Equal justice and free legal aid). Example: Land reform laws and bank nationalization (1970s) are inspired by this.
Article 41: Right to employment, education, and assistance in case of unemployment.
Article 42: Just and humane conditions of work, maternity relief.
Article 43: Living wage, promotion of cottage industries in rural areas. (43A: Workers’ participation in management; 43B: Promotion of cooperative societies).
Article 47: Improvement in nutrition levels and health, prohibition on intoxicating drinks.
- Gandhian Principles
These are inspired by Mahatma Gandhi’s ideas, which emphasize rural development and self-reliance.
Article 40: Organization of village panchayats.
Article 43: Promotion of cottage industries.
Article 46: Educational and economic upliftment of Scheduled Castes/Tribes and weaker sections.
Article 47: Improvement in health and nutrition.
Article 48: Scientific organization of agriculture and animal husbandry, prohibition on cow slaughter.
- Liberal-Intellectual Principles
These focus on human rights, education, and environment.
Article 44: Uniform Civil Code.
Article 45: Free and compulsory education for children aged 6-14 (made a fundamental right under Article 21A in 2002).
Article 48A: Protection of environment and wildlife (added by the 42nd Amendment).
Article 49: Protection of monuments of national importance.
Article 50: Separation of judiciary from the executive.
Article 51: Promotion of international peace and security.
These principles emerged from the debates in the Constituent Assembly, where they were seen as complementary to Fundamental Rights. Although initially given less importance, new principles were added through amendments (like the 42nd and 44th).
Discussion (Features)-
Goal of Social and Economic Democracy: Their main objective is to create such social and economic conditions where all citizens can live a good life and receive social, economic, and political justice.
Establishment of Welfare State: These principles realize the concept of a welfare state, where the primary function of the state is to ensure the welfare of the people.
Non-Enforceable by Courts: These principles are not legally binding, meaning they cannot be enforced through courts.
Guiding for Government: These elements serve as moral and policy-making guides for the government, which keeps them in mind while making laws and policies.
Positive and Negative Obligations: While Fundamental Rights impose negative obligations on the state (what not to do), Directive Principles impose positive obligations (what to do), such as working for public welfare.
Importance of the Directive Principles of State Policy-
The importance of DPSP is deeply connected to the structure of the Indian Constitution and the democratic process. They not only guide the state’s policies but also assist in establishing a just society:-
Establishment of Welfare State: DPSP aim to make India a socialist, secular, and democratic republic. They promote economic democracy, where Fundamental Rights ensure political democracy. Example: MGNREGA is inspired by Article 41, which provides rural employment.
Harmony with Fundamental Rights: Although DPSP are non-justiciable, the judiciary has linked them with Fundamental Rights. In the Kesavananda Bharati case (1973), DPSP were considered part of the basic structure of the Constitution. In the Minerva Mills case (1980), the Supreme Court said that Fundamental Rights and DPSP are “two wheels of the Constitution,” and rights can be limited to implement DPSP. Example: The decision on triple talaq was influenced by Article 44 (Uniform Civil Code).
Social-Economic Justice: These are important in removing inequalities. Land reforms, Right to Education Act (RTE), environmental laws (like Forest Conservation Act) have emerged from DPSP. They bind the state to uplift weaker sections (SC/ST, women, children).
Guidance in Policy Formulation: Article 37 states that DPSP are fundamental in the state’s policies. Parliament and state legislatures make laws keeping them in mind. Example: Aadhaar scheme and GST are linked to economic justice in DPSP.
Judicial Interpretation and Development: Initially, in the Golaknath case (1967), DPSP were placed below Fundamental Rights, but later decisions (like Olga Tellis case, 1985) linked them with the right to life (Article 21). This has made DPSP practically justiciable.
However, the criticism is that these are “paper promises” because they have not been fully implemented (like Uniform Civil Code). Nevertheless, DPSP reflect the progressiveness of the Constitution and are essential for social change in a developing country like India.
2(b) Ans.-
Bihar has natural resources such as coal (more abundant before the Jharkhand division, but still present in some areas), bauxite, limestone, and the fertile Gangetic valley, which are conducive to agriculture-based and mining-based industries. However, as of 2025, the contribution of the industrial sector to Bihar’s Gross State Domestic Product (GSDP) is only around 19%, while the national average is 25-30%. For 2025-26, the GSDP is estimated at 10.97 lakh crore rupees (128.89 billion dollars), which has grown at a CAGR of 11.42% since 2015-16, but this is primarily driven by the services sector, not industry.
The reasons for this are as follow” -
- Weak Infrastructure-
The root of Bihar’s industrial backwardness lies in the lack of basic facilities, which keeps investors away. The road density in the state is lower than the national average (2.1 km/100 sq km)—only 1.5 km/100 sq km. The rail network is also inadequate, and air connectivity is mainly limited to Patna. Establishing industries in flood-affected areas (73% of the state) is challenging, as annual floods cause damage of 10-15 lakh crore.
Specific Example: The Purvanchal Expressway (completed in 2023) has brought some improvement, but logistics costs in rural areas are 25-30% higher. Power availability has improved since 2005 (now claiming 24-hour supply), but blackouts for industrial use are still common, affecting production. According to a 2025 report, per capita electricity consumption in Bihar is 50% lower than the national average. Water management deficiencies affect irrigation and industrial water supply, such as in areas impacted by floods from the Kosi River.
- Political Instability and Corruption-
Bihar’s political history (especially the 1970-2000 period) is filled with instability, including caste-based violence, frequent government changes, and “jungle raj.” This erodes investor confidence. According to Transparency International, Bihar ranks high on the corruption index, where bribery in licenses, land acquisition, and subsidies is common.
Specific Example: In 2006, the Nitish Kumar government introduced an industrial policy, but even by 2025, it has not been effective—MOUs were signed, but only 20-30% of projects started. Historically, the central government’s Freight Equalization Policy (1952-1991) made Bihar’s minerals cheap, transferring industries to other states (like western India), stalling local development. The 2000 Jharkhand division took away 80% of Bihar’s mineral resources, which were the base for steel and coal industries. In the 2025 budget, 5000 crore was allocated for industrial parks, but due to corruption, only 25% implementation occurred.
- Lack of Skilled Manpower-
Bihar’s population is over 13 crore, but the literacy rate is around 70%, and the lack of skill training means skilled labor is unavailable. According to 2025 reports, 60% of youth lack industrial skills, forcing companies to spend extra on training. Brain drain is a major issue—every year, 20-25 lakh youth migrate to other states for labor or jobs.
Specific Example: The number of it is and polytechnic institutions is low (only over 200), while Gujarat has 500+. The Skill India program has brought some improvement, but by 2025, only 10% of youth received industrial training. The rush for government jobs (like millions of applications in BPSC exams) discourages the private sector, as youth seek stability.
- Low Investment and Policy Hurdles-
FDI in Bihar is 60% lower than the national average—in 2024-25, only 500 crore dollars. Policies like Bihar Business Connect (2023) and Industrial Policy (2022) are attractive (tax exemptions, subsidies), but in the Ease of Doing Business ranking, Bihar is at 20th place.
Specific Example: In the 2023 Global Investor Summit, MOUs worth 1 lakh crore were signed, but by 2025, only 15% were implemented, mainly due to delays in land and environmental clearances. Dependence on agriculture by 50% does not promote industries, and there is also a shortage in small-medium enterprises (MSMEs).
- Cycle of Inequality and Poverty-
Bihar’s Gini coefficient (income inequality) is 0.38, the highest in India. The poverty rate is 23%, and per capita income is 50% lower than the national average (about 50,000 rupees annually). This makes the consumer market small, which does not attract large industries.
Specific Example: Rural-urban divide increases social tensions, and 2025 reports indicate that inequality slows development by 20-30%. Historically, since the British era, Bihar has remained agriculture-based, and post-independence central policies (like freight policy) made it even more backward.
- Natural Disasters and Environmental Issues-
Annual floods (Kosi, Gandak rivers) and droughts destroy resources. The 2024 flood destroyed 5 lakh hectares of crops, affecting industrial raw materials.
Specific Example: Strict NGT (National Green Tribunal) rules have stalled the mining industry—many mines closed in 2025. The need for environmental conservation (like increasing forest cover) limits industries.
Indications from Data -
The number of active factories decreased from 3,132 in 2013-14 to 2,782 in 2022-23—an indication of the shrinking industrial base.
According to ASI, Bihar’s contribution to national GVA in manufacturing is extremely low; negative impacts are seen on the state’s industrial stagnation and job creation.
Fluctuations and decline in the share of construction/manufacturing in recent years indicate the weakness of the secondary sector.
Conclusion and Potential Reforms-
Bihar’s slow industrial development is a mix of historical (freight policy, division), structural (infrastructure, skills), and administrative (corruption, policy implementation) reasons. However, positive changes are happening—in 2025, industrial growth has surpassed agriculture, and a 15% increase in GSDP has been recorded.
For reforms: Investment in infrastructure (like Amrit Bharat Yojana), skill development (skill hubs), transparent governance (e-governance), and investment incentives (tax breaks) are necessary. If implemented, Bihar’s resources (like in agro-processing) can become engines of development.
3(a) Ans.-
“The growing population is a major obstacle to development” This statement has often been a subject of discussion in the context of economic, social, and environmental development, especially in developing countries like India. While the growing population is seen on one hand as a “demographic dividend,” on the other hand, it can slow down the pace of development by putting excessive pressure on resources. Here, I will discuss this statement, including both sides—obstacle and potential benefits. The discussion will mainly be in the context of India, where the population in 2025 is approximately 1.46 billion and the growth rate is about 1%, but the total population is still increasing rapidly. This discussion is based on economic theories (such as Malthusian theory), current data, and reports.
- Reasons for Considering Growing Population as an Obstacle -
The growing population proves to be a major obstacle to development because it rapidly consumes limited resources, creating economic, social, and environmental imbalances. The main reasons are as follows:
Excessive Pressure on Resources: The growing population increases the burden on natural resources like water, land, and energy. In India, where the population exceeds 1.4 billion, it promotes water crisis, deforestation, pollution, and soil erosion. For example, population growth leads to excessive consumption of natural resources, increasing water scarcity and pollution. According to the Global Carbon Budget Report 2022, India’s emission rate is likely to increase by 6%, which hinders environmental development. This makes it difficult to deal with Sustainable Development Goals (SDGs) like climate change.
Impact on Economic Development: Rapid population growth outpaces job creation, leading to unemployment, poverty, and inequality. According to Malthusian theory, population grows geometrically while resources grow arithmetically, resulting in lower per capita income. In India, high population growth leads to job shortages, lower capital formation rates, and increased need for investment. As a result, the growth rate of national income and per capita income is affected, because the growing population reduces the capacity for savings and investment. In 2025, India’s economic growth rate is rapid (about 6-7%), but population pressure is increasing regional inequalities, such as North versus South India.
Burden on Social Services: Pressure increases on basic services like education, health, and housing. In India, population growth increases poverty and inequality because resource distribution is uneven. For example, population growth leads to a lack of employment opportunities, which hinders economic development. According to the UNFPA’s 2025 report, many individuals are unable to achieve their reproductive goals, which indirectly affects development.
Environmental and Urbanization Challenges: Increasing urbanization leads to slums, pollution, and pressure on infrastructure. In India, population growth increases water requirements, but lack of management creates crises. This promotes environmental damage, which is an obstacle to long-term development.
Administrative and Planning Challenges: Effective plans and policies need to be made for the proper management of the growing population, but due to shortages in government budgets, human resources, and institutional capacities, plans remain incomplete. The implementation of population control, family planning, and public health campaigns remains disorganized and inadequate. Unbalanced development in rural and urban areas intensifies regional disparities, leading to increased social discontent.
Positive Side of Growing Population: Demographic Dividend -
Although the statement calls it an obstacle, for balance in the discussion, it is necessary to also look at the positive side. If the population is young and skilled, it can become an engine of development:-
Benefit of Working-Age Group: In India, the Total Fertility Rate (TFR) has decreased from 3.4 in 1992-93 to 2.0 in 2019-21, leading to an increase in the working-age population (15-64 years). This can provide a demographic dividend, where economic growth increases. For example, the growth of the middle class is expected to contribute to India’s economic growth. According to IIASA’s 2025 study, India’s socio-economic potential can surpass China’s if there is investment in human capital.
Economic Opportunities: A large population provides a market and labor force, which benefits the digital economy and trade. However, this benefit is only realized when education, skill development, and employment policies are strong. Otherwise, it becomes an obstacle.
Policy Context: Southern states like Tamil Nadu and Andhra Pradesh have benefited from population control, but uneven growth in northern states poses political challenges. In 2025, this issue will emerge further with the census and seat distribution.
Major Challenges of Growing Population -
Stable Population: To achieve the goal of stable population growth, it is necessary to first reduce the fertility rate. It is quite high in states like Bihar, Uttar Pradesh, Haryana, Madhya Pradesh, Jharkhand, and Chhattisgarh, which remains a major challenge.
Quality of Life: To provide citizens with minimum quality of life, investment in education and health systems will be required, more food grains and foodstuffs will need to be produced, homes will need to be provided for living, supply of clean drinking water will need to be increased, and work will need to be done to strengthen basic infrastructure like roads, transportation, and electricity production and distribution.
India needs to spend more to meet the basic needs of citizens and to accommodate the growing population by providing social infrastructure, and for this, India will have to increase its resources through all possible means.
Demographic Division: To take advantage of the growing population, India needs to build a strong base of human capital so that people can make significant contributions to the country’s economy, but India’s low literacy rate (about 74 percent) is the biggest obstacle in this path.
Sustainable Urban Development: By 2050, the country’s urban population will reach 87.7 million, which will pose challenges in improving urban facilities and providing housing to all, and for all this, the environment will also need to be kept in mind.
Unequal Income Distribution: Unequal income distribution and increasing inequality among people will emerge as negative consequences of excessive population.
What Can Be Done -
To ensure food for everyone in the future, it is important to make agriculture profitable and keep food prices from changing too much, i.e., keep them more or less stable.
Implementing Universal Basic Income as a safety net will also help in providing employment opportunities to a large number of unemployed youth.
Proper management of forest and water resources will be necessary to save them for sustainable use.
Achieving Sustainable Development Goals (SDGs) should be the central point of any policy formulation.
India’s northern states, with relatively low income and dense population, will need to take some important decisions like women’s literacy, health, and workforce participation, learning from the southern states.
Better coordination between governments and strong civil society institutions is needed to achieve all goals such as population reduction, maximum equality, better nutrition, universal education, and health facilities.
Increasing life expectancy and the growing adolescent population will help in exploring employment opportunities in new service sectors.
Schemes like AMRUT, Smart City, Make in India, and Sustainable Development Goals will certainly help in enhancing the country’s social infrastructure.
The Way Forward (Other Possible Measures)-
India needs to increase spending in the health sector. Currently, it is only 1.3% of GDP. Out of the total health budget, only 4% is spent on family welfare (planning), and out of that, only 1.5% is spent on measures for spacing births.
Investment for the aging population will need to be increased, because by 2050, the elderly population in India could increase to about 10 times the current level.
Education is very important, not only for empowering women but also for reducing fertility rates. Better education will help women make the right decisions for family planning.
No society can reduce fertility rates until women are part of the workforce. Therefore, effective policies should be made to stop the decline in women’s participation in the workforce.
There is a need to focus especially on areas that are socially, culturally, and economically backward. Identifying 140 such districts is a right step taken by the government in this direction.
The gender ratio in the country is declining, and discrimination against girls is quite high. It is extremely important to pay attention to this issue so that people do not give birth to more children in the hope of having a boy.
By linking with family planning, India can achieve many Millennium Development Goals. Family planning is an encouraging and preventive measure to reduce maternal mortality rate and child mortality rate.
It is important to view the issue of population growth not only from a national perspective but also from the state perspective, because different states need to be encouraged to take different steps to curb population growth.
Conclusion
Overall, the growing population is a major obstacle to development, as it puts pressure on resources, economic savings, and social services, as can be seen in the context of India where overpopulation is a barrier in the path of economic development. However, if policies focus on family planning, investment in education, and sustainable development, it can turn into a benefit. In India, where population growth is now slowing but continues due to momentum, it is necessary to adopt a holistic approach. For developing countries, population management is the key to economic success; otherwise, it can become a “population explosion” and halt development.
3(b) Ans.-
District Planning is an important part of the decentralized planning process in India, designed to ensure development at the local level. It is the process of preparing an integrated development plan at the district level, where plans are made by local governments (panchayats, municipalities, and district councils) taking into account available resources (natural, human, and financial). Its main objective is to connect national and state-level policies with local needs, so that balanced development of rural and urban areas can be achieved. This process was strengthened after the 73rd and 74th Amendments (1992) to the Constitution, under which Article 243ZD made the formation of the District Planning Committee (DPC) mandatory. The function of the DPC is to prepare a Draft District Development Plan by integrating rural and urban plans.
The number of members in the District Planning Committee can vary in each state, as it depends on the state's rules and the district's population proportion. However, in many states, the number of members is not fixed, and the committee includes representation from the district council president, municipal mayor/chairperson, and elected members from rural and urban areas.
Membership Basis:
District Council President: Can be the ex-officio chairperson of the committee.
Mayor/Chairperson: The mayor or chairperson of any municipality located at the district headquarters can be included.
Elected Members: At least 4/5 members are elected in proportion to the population between the district's rural areas (elected members of the district council) and urban areas (councilors of town panchayats and municipal corporations).
Example: In Kerala, the District Planning Committee has 15 members, chaired by the district panchayat president, with the district collector serving as the member secretary.
It includes the following aspects:-
Analysis: Analysis of the district's current situation, its strengths, weaknesses, opportunities, and challenges.
Objective Determination: Clear goals are set for the district's development.
Implementation Strategies: Action plans and methods for mobilizing resources to achieve these goals are outlined.
Coordination: This plan integrates the plans prepared by panchayats and municipalities in the district, enabling integrated development of the entire district.
The meaning of District Planning is mainly as follows:
Integrated Approach: It connects village, block, district, and city-level plans together, including sectors such as health, education, infrastructure, agriculture, environment, and economic development. For example, in the 11th Five-Year Plan, it was considered a major tool for inclusive growth.
Participatory Process: Emphasis on the participation of local residents, elected representatives, NGOs, and experts, so that the plan is built from the bottom-up.
Resource-Based: Mapping and utilization of available funds (central, state, local revenue), along with data analysis using tools like Geographical Information System (GIS).
Long-Term Vision: Typically a 15-20 year vision and a 5-year perspective plan, which includes annual plans.
This process is important in India's federal structure, as it addresses the limitations of centralized planning by focusing on local needs (such as flood management or health services in backward areas). However, its full implementation remains challenging in many states.
Conditions for the Success of District Planning-
The success of district planning depends on several factors, as it is a complex, multi-stakeholder process. Despite many efforts in India (such as the formation of DPCs in states), failures have been observed due to weak implementation. The key conditions for success are as follows, derived from various studies and reports:
Strong Institutional Framework and Decentralization: Effective formation and functioning of the DPC is essential, with a majority of elected members. Transfer of powers by state governments (Functions, Funds, Functionaries - 3Fs) is crucial. Example: Where DPCs are not given sufficient authority, the planning fails. For success, clear guidelines and legal support at the state level are necessary.
Participation and Capacity Building: Ensuring active participation of local communities, women, minorities, and weaker sections. Gathering feedback through gram sabhas, ward committees, and workshops. Capacity building (training) is essential for this, so that representatives can understand the planning process. One reason for failure: Lack of participation makes plans unrealistic.
Effective Resource Management: Accurate mapping of financial resources (central/state grants, local revenue) and transparent allocation. Use of untied funds for priorities. Example: Preventing duplication using software like PlanPlus. Shortage leads to plan failure.
Data-Based and Technical Support: Collection of baseline data (demographics, infrastructure gaps) and use of tools like GIS and Development Radar. Including Environmental Impact Assessment (EIA). For success, availability of data and analysis capacity is essential.
Coordination and Integration: Coordination between rural-urban, sector-wise (health, education), and line departments. Consolidation of plans by DPC. Reason for failure: Overlap or inconsistency.
Monitoring, Evaluation, and Social Audit: Continuous monitoring system and social audit for transparency. Annual reviews and feedback loops. Clear goal setting and program management are key to success.
Political Will and Timeliness: Commitment from state and central governments, along with timely workshops and finalization. Absence of political interference and sustained follow-up.
When these conditions are met, district planning can ensure inclusive development, as seen in some districts (like Kollam, Jaipur). Otherwise, it remains merely a paper exercise.
Comments
Releted Blogs
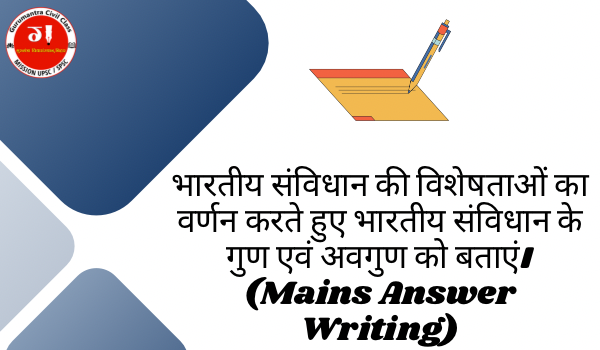
भारतीय संविधान की विशेषताओं का वर्णन करते हुए भारतीय संविधान के गुण एवं अवगुण को बताएं।(Mains Answer Writing)
By - Gurumantra Civil Class
Gurumantra GS Answer Writing Practice

भारत में जनसंख्या नियंत्रण के उपाय पर प्रकाश डालें - Answer writing for Mains Exam
By - Gurumantra Civil Class
जनसंख्या नियंत्रण के लिए किए गए प्रयास एवं उपाय
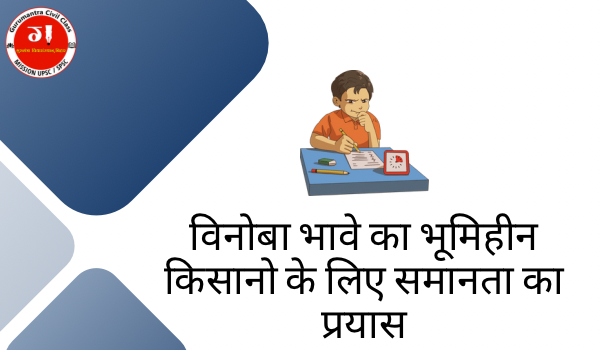
विनोबा भावे का भूमिहीन किसानों के लिए समानता का प्रयास(Vinoba Bhave's attempt at equality for the landless farmers) GS Mains Writing
By - Gurumantra Civil Class
GS Mains Writing for Civil Service

महासागरीय लवणता में विभिन्नता के कारण और प्रभाव ( Causes and Effects of Variation in Ocean Salinity) GS Mains Answer Writing
By - Gurumantra Civil Class
GS Mains Answer Writing for Civil Service Exam.