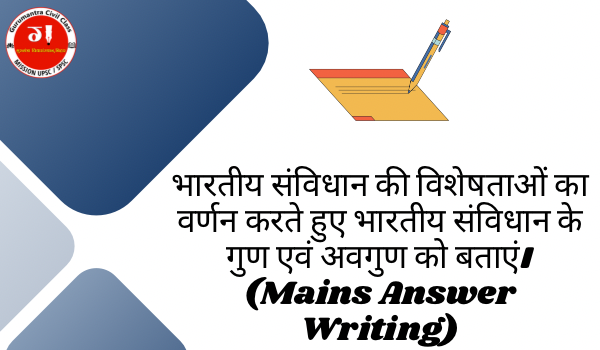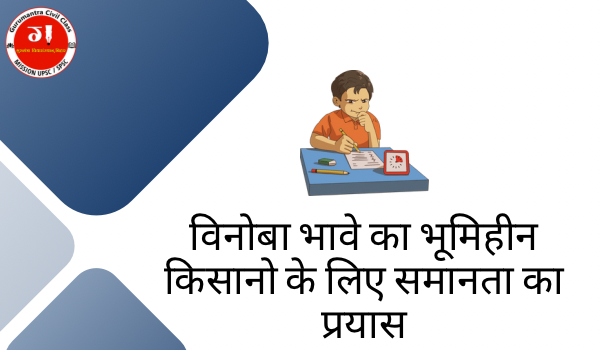|
BPSC PYQ Mains Program Answer Writing
Session I – Polity + Bihar + Special + Current Issues
Day – 2
1. नीचे दिए गए प्रश्नों को सौ से डेढ़ सौ शब्दों में लिखे ।
Write down the following questions in a hundred to one hundred and fifty words.
(a) बिरसा आंदोलन पर विशेष प्रकाश डालते हुए बिहार के आदिवासी आंदोलनों की समीक्षा कीजिए।
Briefly examine the tribal movements of bihar, with a special reference to the Birsa movement.
(b) बिहार के किसान आंदोलनों का समान्यत: वर्णन करते हुए चंपारण आंदोलन में विशेषत: गाँधी जी के हस्तक्षेप की विशेषता कीजिए।
Discuss the present moment of bihar in general and the intervention of gandhiji, particularly in the champaran movement.
2. भारत ने पंचायती राज्य के उद्देश्यों तथा उसकी विशेषताओं का उल्लेख कीजिए ।
Describe the objectives and features of the panchayati raj in india. (In 250 -300 Words)
3. नीचे दिए गए प्रश्नों को सौ से डेढ़ सौ शब्दों में लिखे ।
Write down the following questions in a hundred to two hundred words.
(a) तकनीकी स्तर से क्या अभिप्राय है? इस विषय पर चर्चा करें कि तकनीकी स्तर विकास स्तर को बढ़ावा दे रहा है या मशीनीकरण से बेरोजगारी की समस्या बढ़ रही है या आने वाले समय में बढ़ सकती है।
"What is meant by the term technological level? Discuss whether the technological level is promoting the level of development or whether mechanization is increasing the problem of unemployment, or may increase it in the future."
(b) भारतीय सिनेमा में बढ़ती हुई हिंसा व नग्नता के पक्ष तथा विपक्ष में अपना आलोचनात्मक मत प्रस्तुत कीजिए।इसमें सेंसर बोर्ड की भूमिका की समीक्षा कीजिए।
Write a critical note in favour and against of increasing violations and nugityn Indian cinema and the role of censorship.
📚 BPSC Mains Writing Practice – 40 Days Program
(39th - 70th BPSC Mains PYQ – Complete Writing Practice)
⚡ 40 दिन का दमदार राइटिंग प्रोग्राम – सफलता की गारंटी की ओर पहला कदम! ⚡
✨ अब तैयारी होगी और भी सटीक ✨
👉 विशेष रूप से 71st & 72nd BPSC Mains के लिए
👉 Offline + Online Mode में सुविधा
👉 साथ में Answer Module भी उपलब्ध
📅 Batch Start: 18 September 2025
📞 Admission Helpline:
9135904639 | 7250380187
App.- Gurumantra.online
🏛️ Offline Centre:
Parwati Market, West Boring Canal Road,
Beside Power Substation, Patna – 01
Solutions
1.(a) ans.-
बिहार का इतिहास आदिवासी आंदोलनों से भरा पड़ा है, जो मुख्य रूप से ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन, जमींदारों और बाहरी साहूकारों (दिकुओं) की शोषणकारी नीतियों के विरुद्ध संघर्ष का प्रतीक हैं। ये आंदोलन भूमि हड़पने, ऊँचे लगान, बंधुआ मजदूरी, धार्मिक हस्तक्षेप और सांस्कृतिक विस्थापन जैसी समस्याओं से उपजे थे। 19वीं शताब्दी में चोटानागपुर (वर्तमान झारखंड सहित) क्षेत्र में ये आंदोलन अधिक सक्रिय रहे, क्योंकि यहाँ मुंडा, संथाल, हो, कोल आदि आदिवासी समुदायों की घनी आबादी थी। ये आंदोलन असंगठित, स्थानीय और आवर्ती थे, लेकिन इन्होंने आदिवासी पहचान को मजबूत किया और स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया। कुल मिलाकर, ये आंदोलन ब्रिटिश शासन की कमजोरियों को उजागर करते हुए सामाजिक-आर्थिक सुधारों का आधार बने।
“बिरसा मुंडा आंदोलन” भारतीय इतिहास में अनेकों महान आंदोलनों में से एक है, जिसने देश को स्वतंत्रता की ओर अग्रसर किया है। यह आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण चरित्र के रूप में मान्यता प्राप्त कर चुका है। बिरसा मुंडा आंदोलन/विद्रोह की शुरुआत 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में हुई। इस विद्रोह के प्रमुख नेता बिरसा मुंडा थें जिनका जन्म 15 नवंबर 1875 को झारखंड में हुआ था। उनके पिता का नाम सुगना मुंडा और माता का नाम करमी था। वह जनजाति क्षेत्र के लोगों के बीच देवा के नाम से भी प्रसिद्ध थे। मुंडा एक जनजातीय समूह था जो छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में निवास करते थें जिसे दामन-ए-कोह भी कहा जाता था।
बिरसा आंदोलन से पहले भी बिहार (विशेषकर छोटानागपुर क्षेत्र) में आदिवासी आंदोलन हुए थे, जिनके पीछे मुख्य रूप से अंग्रेजी हुकूमत के आने के बाद हुए भूमि और सांस्कृतिक परिवर्तन थे:
आर्थिक कारण:
- भू-राजस्व नीतियों में बदलाव: अंग्रेजों ने अपनी भू-राजस्व नीतियों में बदलाव किए, जिससे आदिवासी समुदायों की पारंपरिक भूमि व्यवस्था अस्त-व्यस्त हो गई।
- जमींदारों और महाजनों का शोषण: बाहरी लोगों (जिन्हें 'दिकु' कहा जाता था) का आगमन बढ़ा और उन्होंने जमींदार व महाजन बनकर आदिवासियों का आर्थिक शोषण करना शुरू कर दिया।
- वन कानूनों का प्रतिबंध: वन विभाग द्वारा बंजर भूमि को अधिग्रहित किया गया और वन उत्पादों पर प्रतिबंध लगाए गए, जिससे आदिवासियों की जीवनशैली प्रभावित हुई।
सामाजिक और सांस्कृतिक कारण:
- धर्मांतरण और ईसाई मिशनरी का प्रभाव: मिशनरियों ने आदिवासी समुदायों में धर्मांतरण बढ़ाया, जिससे आदिवासी संस्कृति और परंपराओं पर बाहरी प्रभाव बढ़ा।
- सामंती व्यवस्था का विस्तार: अंग्रेजों ने आदिवासी क्षेत्रों में सामंती व्यवस्था को बढ़ावा दिया, जिससे आदिवासियों की स्वायत्तता कम हुई।
बिहार के आदिवासी आंदोलन कालानुक्रमिक रूप से निम्नलिखित प्रमुख हैं:
- हो और मुंडा विद्रोह (1820-22): सिंहभूम क्षेत्र में ब्रिटिश भूमि राजस्व नीतियों और बंगाली समुदाय के प्रवेश पर प्रतिबंध के विरुद्ध। नेता: राजा पहाड़। परिणाम: ब्रिटिश दमन के बाद शांत, लेकिन जमींदारों के शोषण पर चेतावनी।
- भूमिज विद्रोह (1832-33): पूर्वी भारत कंपनी की नई भूमि विनियमों से किसानों की आर्थिक शोषण के खिलाफ। नेता: गंगा नारायण। परिणाम: नेता की मृत्यु से हिंसा कम हुई, ब्रिटिश प्रभाव सीमित।
- कोल विद्रोह (1831-32): भूमि का मुसलमानों और सिखों को हस्तांतरित होना, साहूकारों-जमींदारों का प्रवेश, ऊँचा कर और बंधुआ मजदूरी। नेता: बुद्धू भगत (आदिवासी कोल समुदाय)। परिणाम: कोल, ओरांव और भील समुदायों के शोषण को उजागर किया, लेकिन दबा दिया गया।
- संथाल विद्रोह (1855-56): जमींदारी प्रथा, साहूकारों के ऊँचे ब्याज और भूमि हड़पने के विरुद्ध। नेता: सिद्धू और कान्हू मुर्मू। परिणाम: जून 1855 में 10,000 संथालों की भागीदारी के बावजूद ब्रिटिश दमन से समाप्त; बाद में संथाल परगना की स्थापना हुई। यह सबसे बड़ा आदिवासी विद्रोह था, जिसने ब्रिटिश नीतियों पर सवाल उठाए।
- सफा होर विद्रोह (1870): धार्मिक भावनाओं पर प्रतिबंध और सामाजिक सुधार (एक ईश्वर की अवधारणा) के लिए। नेता: बाबा भगिरथ मांझी, लाल हेम्ब्रम, पैका मुर्मू (खरवार आंदोलन)। परिणाम: ब्रिटिश दमन, लेकिन 'सफा होर' (शुद्ध मनुष्य) की अवधारणा से आत्म-शुद्धिकरण को बढ़ावा।
- ताना भगत आंदोलन (1914-19): जमींदारों, साहूकारों और ब्रिटिश शासन के विरुद्ध; प्रारंभ में अहिंसक धार्मिक (कुरुख धर्म)। नेता: जत्रा भगत। परिणाम: ब्रिटिश क्रूर दमन से समाप्त, लेकिन गैर-हिंसा की प्रेरणा दी।
ये आंदोलन सामान्यतः असफल रहे, लेकिन इन्होंने ब्रिटिश शासन को सुधारात्मक कदम उठाने पर मजबूर किया, जैसे भूमि संरक्षण कानून।
बिरसा मुंडा का नेतृत्व वाला मुंडा विद्रोह (उलगुलान) बिहार (चोटानागपुर) के आदिवासी आंदोलनों में सबसे महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक रहा। यह न केवल राजनीतिक संघर्ष था, बल्कि सामाजिक-धार्मिक पुनरुत्थान का प्रतीक भी था। बिरसा मुंडा (1875-1900), एक युवा आदिवासी नेता, को 'भगवान' और 'धरती आबा' (पृथ्वी का पिता) कहा जाता था। उनका जन्म उलिहातू गाँव (रांची) में हुआ और बचपन में भेड़ चराने वाले बिरसा ने सलगा में प्रारंभिक शिक्षा ली, जर्मन मिशनरी स्कूल में ईसाई बनकर पढ़ाई की, लेकिन बाद में ईसाई धर्म त्याग दिया और आदिवासी परंपराओं की ओर लौटे। उन्होंने 'बिरसैत' धर्म की स्थापना की, जिसमें एक ईश्वर की पूजा और बोंगा (आदिवासी देवताओं) का त्याग था।
बहरहाल बिरसा द्वारा घोषित उद्देश्यों की दृष्टि से देखा जाए तो इन्होंने न तो ब्रिटिश शासन का अंत कर स्वतंत्र मुंडा राज्य की स्थापना की और न ही अपने क्षेत्र से सभी दिकुओं को बाहर निकालने में सफल हुए।
बिरसा मुंडा आंदोलन के परिणाम-
1.राजनीतिक प्रशासनिक परिणाम -
- 1903 में काश्तकारी संशोधन एक्ट द्वारा पहली बार मुंडा को खूंटकटी व्यवस्था को कानूनी मान्यता प्रदान की गई।
- 1905 में प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से खूँटी तथा गुमला न अनुमंडल बनाए गए।
- ब्रिटिश प्रशासन आदिवासियों के प्रति अधिक संवेदनशील हो गई।
2.आर्थिक परिणाम - इन्हें बेगारी से मुक्ति मिली। मुंडाओं को जमीन संबंधी कई अधिकार प्राप्त हुए। इनके जमीन का सर्वे कराया गया। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के तहत इन्हें इनकी जमीन वापस की गई साथ ही इनकी भूमि बंदोबस्ती भी करवाई गई।
3.सामाजिक-सांस्कृतिक-धार्मिक परिणाम - कई सामाजिक,सांस्कृतिक तथा धार्मिक समस्याओं जैसे- शराबखोरी, अशिक्षा, बलिप्रथा बहुदेववाद आदि का उन्मूलन हुआ तथा समाज में आधुनिकता को बढ़ावा मिली।
4.दीर्घकालिक परिणाम - राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष में बिरसा मुंडा आंदोलन/विद्रोह प्रेरणा का स्रोत बना। इस विद्रोह के उद्देश्य, प्रकृति, संगठन जैसे तत्वों को गांधीवादी आंदोलन में देखा जा सकता है।
बिरसा मुंडा आंदोलन की प्रकृति-
1.स्थानीय व जनजाति - चूँकि इस आंदोलन का प्रभाव क्षेत्र सीमित था साथ ही इसमें भाग लेने वाले लोगों से लेकर नेतृत्वकर्ता तक जनजाति समूह से थें।
2.उपनिवेश विरोधी - अंग्रेजों द्वारा हमेशा बाहरी जमींदारों का समर्थन किया जाता था इसलिए यह आंदोलन उपनिवेश विरोधी हो गया था।
3.सामाजिक धार्मिक प्रवृत्ति - बिरसा मुंडा ने स्वयं को भगवान का अवतार बताया तथा सिंगबोंगा की पूजा का आहवान किया साथ ही समाज में फैली विभिन्न बुराइयों के उन्मूलन हेतु प्रयास किए।
4.हिंसक - इस आंदोलन में मुख्यतया महाजनों को क्षति पहुंचाई गई, ऋण संबंधी दस्तावेजों को जला दिया गया तथा अंग्रेजों के साथ संघर्ष में मुंडाओं ने वीरता का परिचय दिया
5.शोषण विरोधी - औपनिवेशिक शक्तियों की दोषपूर्ण नीति तथा जंगलों पर से इन जनजातीय समूह को वंचित कर देना, इस विद्रोह का मुख्य कारण रहा।
6.राष्ट्रवादी - उल्लेखनीय है कि बिरसा मुंडा एक स्वतंत्र मुंडा राज्य की स्थापना करना चाहते थें। अतः इस विद्रोह को 1857 के विद्रोह का प्रेरणास्रोत भी माना जाता है।
7.सुधारवादी- उस समय में मुंडाओं के समाज में विभिन्न व्याधियों ने जगह बना ली थीं जैसे – मदिरापान घरेलू हिंसा आदि। बिरसा मुंडा इन्हीं कुरीतियों को खत्म कर एक स्वस्थ एवं आदर्श समाज की स्थापना करना चाहते थें।
8.मसीहावादी - बिरसा मुंडा खुद को सिंगबोंगा का अवतार मानते थें इसलिए कुछ विद्वान इस आंदोलन के स्वरूप को मसीहवाद की संज्ञा देते हैं।
वस्तुतः यह आंदोलन/ बिरसा मुंडा विद्रोह असफल रहा साथ ही मुंडा जनजाति को तात्कालिक कोई लाभ नहीं मिल पाया। परंतु विद्रोह की भयावहता तथा उग्रता के कारण सरकार को उनकी समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करना पड़ा।
निष्कर्षतः कहा जाए तो जनजातीय व् राष्ट्रीय आन्दोलनों की श्रेणी में बिरसा मुंडा आंदोलन का नाम अग्रणी है। इस आंदोलन को न केवल ब्रिटिश शासन ने चोट पहुंचायी बल्कि आने वाले राष्ट्रव्यापी आन्दोलनों के लिए प्रकाश पुंज का कार्य किया। इस आन्दोलन की महत्ता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसके मूल्य वर्तमान समाज के लिए प्रेरणास्रोत हैं। इस दिशा में वर्त्तमान प्रधानमंत्री द्वारा बिरसा मुंडा के जन्म दिवस यथा 26 नवम्बर को ‘जनजातीय गौरव दिवस’ के रूप में मनाया जाना वर्त्तमान प्रासंगिकता को उजागर करता है।
संक्षेप में -
बिरसा आंदोलन पर विशेष प्रकाश (मुंडा उलगुलान, 1899-1900) -
बिरसा मुंडा का नेतृत्व वाला मुंडा विद्रोह (उलगुलान) बिहार (चोटानागपुर) के आदिवासी आंदोलनों में सबसे महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक रहा। यह न केवल राजनीतिक संघर्ष था, बल्कि सामाजिक-धार्मिक पुनरुत्थान का प्रतीक भी था। बिरसा मुंडा (1875-1900), एक युवा आदिवासी नेता, को 'भगवान' और 'धरती आबा' (पृथ्वी का पिता) कहा जाता था। उनका जन्म उलिहातू गाँव (रांची) में हुआ और वे ईसाई मिशनरियों से प्रभावित होकर शिक्षा ग्रहण करने के बाद आदिवासी संस्कृति की रक्षा के लिए लौटे।
कारण:
- भूमि अलगाव: ब्रिटिश भूमि नीतियों ने पारंपरिक 'खुंटकट्टी' प्रथा को नष्ट कर दिया, जिससे आदिवासी भूमि जमींदारों और साहूकारों (दिकुओं) के हाथों चली गई।
- आर्थिक शोषण: ऊँचे ब्याज, बेगार (बंधुआ मजदूरी) और गरीबी।
- धार्मिक हस्तक्षेप: ईसाई मिशनरियों का रूपांतरण प्रयास, जो आदिवासी परंपराओं (जैसे पशु बलि) को चुनौती देता था।
- सामाजिक दमन: बिरसा ने विदेशी प्रभाव से मुक्ति और मुंडा राज की स्थापना का नारा दिया।
घटनाक्रम:
- 1894 में बिरसा ने मुंडा, ओरांव आदि को एकजुट किया और कर-ऋण न चुकाने की सलाह दी।
- 1895 में गिरफ्तारी के बाद आंदोलन तेज हुआ।
- 24 दिसंबर 1899 (क्रिसमस ईव) को उलगुलान शुरू: आदिवासियों ने पारंपरिक हथियारों से जमींदारों, ठेकेदारों, पुलिस और मिशनरियों पर हमला किया, उनके घर जलाए।
- जनवरी 1900 में संघर्ष चरम पर: 5 जनवरी को चौकीदारों पर हमला, 7 जनवरी को पुलिसकर्मी की हत्या।
- ब्रिटिश ने 13-26 जनवरी तक दमन अभियान चलाया। बिरसा की गिरफ्तारी 3 फरवरी 1900 को हुई; वे जेल में हैजा से 9 जून 1900 को मृत्यु को प्राप्त हुए (कुछ स्रोतों में विषाक्त भोजन का संदेह)। लगभग 350 मुंडाओं पर मुकदमा चला, 3 को फाँसी और 44 को आजीवन कारावास।
परिणाम और प्रभाव:
- विद्रोह जनवरी 1900 तक दबा दिया गया, लेकिन इसने मुंडा समाज को मजबूत किया।
- 1905 में खूंटी और गुमला को उप-विभाग बनाया गया।
- 1908 का चोटानागपुर किरायेदारी अधिनियम: आदिवासी भूमि संरक्षण, दिकुओं का हस्तक्षेप रोकना और बेगार निषेध।
- महत्व: यह आंदोलन आदिवासी प्रतिरोध का प्रतीक बना, जिसने स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित किया। बिरसा जयंती (15 नवंबर) झारखंड में छुट्टी है, और राज्य का गठन भी इसी दिन (2000) हुआ। यह आंदोलन ब्रिटिश अन्याय के विरुद्ध आदिवासी बलिदान को रेखांकित करता है।
प्रमुख घटनाएँ:
- 1895: चालकाड़ में ईसाई धर्म त्याग, स्वयं को पैगंबर घोषित; किरायेदारों को किराया न देने का आदेश। 24 अगस्त को गिरफ्तार, दो वर्ष जेल।
- 1898: रिहाई के बाद चुटिया में दस्तावेज संग्रह, मंदिर स्थापना के प्रयास।
- दिसंबर 1899: क्रिसमस पर 7000 अनुयायी एकत्र, उलगुलान की घोषणा; मुरहू और सरवाड़ा में मिशनों पर हमला।
- 5 जनवरी 1900: एटकेड़ीह में दो पुलिसकर्मियों की हत्या।
- 7 जनवरी 1900: खूंटी थाने पर हमला, एक कांस्टेबल की हत्या, दुकानों का विध्वंस।
- 3 फरवरी 1900: जामकोपाई जंगल में बिरसा गिरफ्तार।
The history of Bihar is replete with tribal movements, which are symbols of struggle primarily against the exploitative policies of British colonial rule, zamindars, and outsider moneylenders (dikus). These movements arose from issues such as land grabbing, high rents, bonded labor, religious interference, and cultural displacement. In the 19th century, these movements were particularly active in the Chotanagpur (including present-day Jharkhand) region, where there was a dense population of tribal communities like the Mundas, Santhals, Hos, Kols, etc. These movements were unorganized, local, and recurrent, but they strengthened tribal identity and contributed to the freedom struggle. Overall, these movements exposed the weaknesses of British rule and laid the foundation for socio-economic reforms.
The "Birsa Munda Movement" is one of the many great movements in Indian history that propelled the country toward independence. This movement/rebellion has been recognized as an important chapter in the Indian freedom struggle. The Birsa Munda movement/rebellion began in the last years of the 19th century. Its main leader was Birsa Munda, who was born on November 15, 1875, in Jharkhand. His father's name was Sugna Munda and his mother's name was Karmi. He was also famous among the tribal people of the region by the name of Deva. The Munda was a tribal group that inhabited the Chotanagpur Plateau region, which was also known as Daman-e-Koh.
Before the Birsa Movement, there had been tribal movements in Bihar (especially in the Chotanagpur region), which were mainly due to land and cultural changes after the arrival of British rule:
Economic Causes:
- Changes in land revenue policies: The British made changes in their land revenue policies, which disrupted the traditional land system of tribal communities.
- Exploitation by zamindars and moneylenders: The influx of outsiders (called 'dikus') increased, and they began economic exploitation of tribals by becoming zamindars and moneylenders.
- Restrictions from forest laws: The forest department acquired fallow lands and imposed bans on forest products, which affected the tribals' way of life.
Social and Cultural Causes:
- Conversion to Christianity and the influence of Christian missionaries: Missionaries increased conversions among tribal communities, leading to greater external influence on tribal culture and traditions.
- Expansion of the feudal system: The British promoted the feudal system in tribal areas, which reduced the tribals' autonomy.
Chronologically, the major tribal movements in Bihar are as follows:
- Ho and Munda Rebellion (1820-22): In the Singhbhum region, against British land revenue policies and the entry of the Bengali community. Leader: Raja Pahad. Outcome: Calmed after British suppression, but served as a warning against zamindar exploitation.
- Bhumij Rebellion (1832-33): Against the economic exploitation of farmers due to the new land regulations of the East India Company. Leader: Ganga Narayan. Outcome: Violence subsided after the leader's death, with limited British influence.
- Kol Rebellion (1831-32): Due to the transfer of land to Muslims and Sikhs, entry of moneylenders-zamindars, high taxes, and bonded labor. Leader: Budhu Bhagat (from the tribal Kol community). Outcome: Exposed the exploitation of Kol, Oraon, and Bhil communities, but was suppressed.
- Santhala Rebellion (1855-56): Against the zamindari system, high interest from moneylenders, and land grabbing. Leaders: Sidhu and Kanhu Murmu. Outcome: Ended due to British suppression despite participation of 10,000 Santhals in June 1855; later led to the establishment of Santhal Pargana. It was the largest tribal rebellion, which raised questions about British policies.
- Safa Hor Rebellion (1870): For religious sentiments against restrictions and social reform (concept of one God). Leaders: Baba Bhagirath Manjhi, Lal Hembram, Paika Murmu (Kharwar movement). Outcome: British suppression, but the concept of 'Safa Hor' (pure human) promoted self-purification.
- Tana Bhagat Movement (1914-19): Against zamindars, moneylenders, and British rule; initially a non-violent religious (Kurukh religion) movement. Leader: Jatra Bhagat. Outcome: Ended due to brutal British suppression, but inspired non-violence.
These movements were generally unsuccessful, but they forced the British administration to take reformative steps, such as land protection laws.
The Munda rebellion (Ulugulan) led by Birsa Munda remained the most important and inspirational among the tribal movements in Bihar (Chotanagpur). It was not only a political struggle but also a symbol of social-religious revival. Birsa Munda (1875-1900), a young tribal leader, was called 'God' and 'Dharti Aaba' (Father of the Earth). He was born in Ulihatu village (Ranchi) and in childhood, while herding sheep, Birsa received his early education in Salga, studied in a German missionary school by converting to Christianity, but later renounced Christianity and returned to tribal traditions. He founded the 'Birsait' religion, which involved worship of one God and the abandonment of Bonga (tribal deities).
However, from the perspective of the objectives declared by Birsa, they neither ended British rule to establish an independent Munda state nor succeeded in expelling all dikus from their area.
Outcomes of the Birsa Munda Movement -
1. Political-Administrative Outcomes - In 1903, the Tenancy Amendment Act legally recognized the Khuntkatti system for Mundas for the first time.
In 1905, Khunti and Gumla were made sub-divisions for administrative convenience.
The British administration became more sensitive toward tribals.
2. Economic Outcomes - They were freed from begar (forced labor). Mundas gained several land-related rights. Their land was surveyed. Under the Chotanagpur Tenancy Act 1908, their land was returned to them, and their land settlement was also carried out.
3. Social-Cultural-Religious Outcomes - Many social, cultural, and religious problems such as alcoholism, illiteracy, animal sacrifice, polytheism, etc., were eradicated, and modernity was promoted in society.
4. Long-term Outcomes - The Birsa Munda movement/rebellion became a source of inspiration in the national freedom struggle. Elements like its objectives, nature, and organization can be seen in the Gandhian movement.
Nature of the Birsa Munda Movement -
1. Local and Tribal - Since the movement's area of influence was limited and all participants, including the leadership, were from tribal groups.
2. Anti-Colonial - The British always supported outsider zamindars, so the movement became anti-colonial.
3. Social-Religious Orientation - Birsa Munda declared himself an incarnation of God and called for the worship of Singbonga, along with efforts to eradicate various evils in society.
4. Violent - In this movement, moneylenders were mainly targeted, debt documents were burned, and Mundas displayed valor in clashes with the British.
5. Anti-Exploitation - The faulty policies of colonial powers and depriving tribal groups of forests were the main causes of this rebellion.
6. Nationalist - Notably, Birsa Munda wanted to establish an independent Munda state. Hence, this rebellion is also considered an inspiration for the 1857 rebellion.
7. Reformist - At that time, various ailments had taken root in Munda society, such as alcohol consumption and domestic violence. Birsa Munda wanted to eliminate these evils and establish a healthy and ideal society.
8. Messianic - Birsa Munda considered himself an incarnation of Singbonga, so some scholars term the nature of this movement as messianism.
In fact, this movement/Birsa Munda rebellion was unsuccessful, and the Munda tribe did not gain any immediate benefits. However, due to the ferocity and intensity of the rebellion, the government was forced to focus on their problems.
In conclusion, it can be said that the Birsa Munda movement holds a leading position in the category of tribal and national movements. Not only did this movement inflict a blow on British rule, but it also served as a beacon for future nationwide movements. The importance of this movement can be gauged from the fact that its values are a source of inspiration for contemporary society. In this direction, the current Prime Minister's declaration of Birsa Munda's birth anniversary, i.e., November 26, as 'Tribal Pride Day' highlights its current relevance.
In summary -
Special Focus on Birsa Movement (Munda Ulugulan, 1899-1900)
The Munda rebellion (Ulugulan) led by Birsa Munda remained the most important and inspirational among the tribal movements in Bihar (Chotanagpur). It was not only a political struggle but also a symbol of social-religious revival. Birsa Munda (1875-1900), a young tribal leader, was called 'God' and 'Dharti Aaba' (Father of the Earth). He was born in Ulihatu village (Ranchi) and after being influenced by Christian missionaries and receiving education, he returned to protect tribal culture.
Causes:
- Land alienation: British land policies destroyed the traditional 'Khuntkatti' system, causing tribal land to fall into the hands of zamindars and moneylenders (dikus).
- Economic exploitation: High interest rates, begar (bonded labor), and poverty.
- Religious interference: Christian missionaries' conversion efforts, which challenged tribal traditions (such as animal sacrifice).
- Social oppression: Birsa called for liberation from foreign influence and the establishment of a Munda kingdom.
Sequence of Events:
- In 1894, Birsa united Mundas, Oraons, etc., and advised them not to pay rent or debts.
- In 1895, after arrest, the movement intensified.
- On December 24, 1899 (Christmas Eve), Ulugulan began: Tribals attacked zamindars, contractors, police, and missionaries with traditional weapons, burning their homes.
- In January 1900, the struggle peaked: Attack on chowkidars on January 5, murder of a policeman on January 7.
- The British conducted a suppression campaign from January 13-26. Birsa was arrested on February 3, 1900; he died of cholera in jail on June 9, 1900 (some sources suspect poisoned food). About 350 Mundas were tried, 3 were hanged, and 44 were sentenced to life imprisonment.
Outcomes and Impact:
- The rebellion was suppressed by January 1900, but it strengthened Munda society.
- In 1905, Khunti and Gumla were made sub-divisions.
- Chotanagpur Tenancy Act 1908: Protected tribal land, stopped diku interference, and prohibited begar.
- Importance: This movement became a symbol of tribal resistance, inspiring the freedom struggle. Birsa Jayanti (November 15) is a holiday in Jharkhand, and the state was formed on the same day (2000). This movement underscores the tribal sacrifice against British injustice.
Major Events:
- 1895: Renounced Christianity at Chalkad, declared himself a prophet; ordered tenants not to pay rent. Arrested on August 24, jailed for two years.
- 1898: After release, collected documents in Chutia, attempted to establish a temple.
- December 1899: On Christmas, 7000 followers gathered, declaration of Ulugulan; attacks on missions in Murhu and Sarwada.
- January 5, 1900: Murder of two policemen in Etkedih.
- January 7, 1900: Attack on Khunti police station, murder of one constable, destruction of shops.
- February 3, 1900: Birsa arrested in Jamkopai jungle.
(b) ans.-
बिहार के किसान आंदोलन मुख्य रूप से नील की खेती से संबंधित थे, जिसकी मजबूरी के खिलाफ किसानों ने विद्रोह किया, खासकर चंपारण में तिनकठिया प्रथा के तहत जबरन नील की खेती करानी पड़ती थी। गांधीजी ने राजकुमार शुक्ला के आग्रह पर चंपारण में हस्तक्षेप किया, जहां उन्होंने सत्याग्रह के माध्यम से तिनकठिया प्रथा को खत्म कराया और किसानों के अधिकारों की रक्षा की। बिहार के किसान आंदोलन मुख्य रूप से ब्रिटिश औपनिवेशिक काल (19वीं-20वीं शताब्दी) में केंद्रित थे, जो जमींदारी प्रथा, उच्च लगान, अवैध वसूलियाँ (अबवाब), बेगार (जबरन श्रम), नील की जबरन खेती और भूमि हड़पने के विरुद्ध थे। बिहार की अर्थव्यवस्था कृषि-आधारित होने के कारण (लगभग 96% आबादी कृषि पर निर्भर), ये आंदोलन ग्रामीण शोषण, भूमि असमानता और आर्थिक संकट से प्रेरित थे। प्रारंभिक आंदोलन स्थानीय और असंगठित थे, लेकिन 20वीं शताब्दी में राष्ट्रीय आंदोलनों से जुड़ गए, जिससे वे अधिक संगठित हुए। इनमें आदिवासी विद्रोह (जैसे संथाल और मुंडा) भी शामिल थे, जो किसान आंदोलनों का हिस्सा बने। ये आंदोलन स्वतंत्रता संग्राम को मजबूत करने और भूमि सुधारों (जैसे जमींदारी उन्मूलन) का आधार बने।
प्रमुख किसान आंदोलनों का संक्षिप्त विवरण
बिहार के प्रमुख किसान आंदोलनों में निम्नलिखित शामिल हैं:
- नील विद्रोह (1859-60): बिहार के चंपारण, तिरहुत और सारण क्षेत्रों में नील की जबरन खेती और निम्न मूल्य के विरुद्ध। कारण: ब्रिटिश नील कारखानों द्वारा किसानों का शोषण। नेता: स्थानीय किसान। परिणाम: 1860 का नील आयोग गठित, लेकिन पूर्ण सफलता नहीं मिली।
- पंडौल विद्रोह (1866-67): बिहार में सबसे पहले 1866-67 के दौरान मधुबनी जिले के पंडौल गांव में किसानों का विद्रोह हुआ। यह दरभंगा कमिश्नरी के अंतर्गत आता था और जमींदारों के बढ़ते अत्याचारों के विरोध में शुरू हुआ था
- संथाल विद्रोह (1855-56): संथाल परगना में जमींदारों, साहूकारों और बाहरी व्यापारियों के विरुद्ध। कारण: भूमि हड़पना और उच्च ब्याज। नेता: सिद्धू-कान्हू। परिणाम: ब्रिटिश दमन, लेकिन संथाल परगना की स्थापना।
- मुंडा विद्रोह (1899-1900): छोटानागपुर में भूमि असमानता और बाहरी हस्तक्षेप के विरुद्ध। कारण: पारंपरिक भूमि प्रथा का उल्लंघन। नेता: बिरसा मुंडा। परिणाम: दमन, लेकिन 1908 का छोटानागपुर किरायेदारी अधिनियम।
- दरभंगा राज के विरुद्ध आंदोलन (1919-20): दरभंगा राज द्वारा उच्च भूमि राजस्व के विरुद्ध। कारण: प्रथम विश्व युद्ध के बाद आर्थिक दबाव। नेता: स्वामी विद्यानंद। परिणाम: व्यापक समर्थन, लेकिन सीमित सफलता।
- बकास्ट आंदोलन (1930s): जमींदारों द्वारा बकास्ट भूमि (किरायेदारों से पुनः हड़पी भूमि) के विरुद्ध। कारण: भूमि पुनर्वास और बेगार। नेता: स्वामी सहजानंद सरस्वती (बिहार प्रांतीय किसान सभा, 1929)। परिणाम: सत्याग्रह और प्रदर्शन; कांग्रेस को ग्रामीण आधार मिला।
- दलमिया शुगर फैक्टरी आंदोलन (1938-39): श्रमिक शोषण के विरुद्ध। कारण: मजदूरों पर अत्याचार। नेता: किसान सभा। परिणाम: आंदोलन दबाया गया, लेकिन मजदूर जागृति।
- बिहार प्रांतीय किसान सभा (1929)- स्वामी सहजानंद सरस्वती की भूमिका: 1929 में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की। इसका गठन सारन जिले के सोनपुर मेले में हुआ था। इसके मुख्य लक्ष्य थे:-
- जमींदारी प्रथा का उन्मूलन
- किसानों के अधिकारों की सुरक्षा
- भू-राजस्व में कमी
- ऋण की संस्थागत व्यवस्था
किसान सभा के सम्मेलन:
- प्रथम सम्मेलन: 17 नवंबर 1929 को स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में सोनपुर में हुआ
- द्वितीय सम्मेलन: पुरुषोत्तम दास टंडन की अध्यक्षता में अगस्त 1934 में हुआ, जिसमें खान अब्दुल गफ्फार खान ने भी हिस्सा लिया
- तृतीय सम्मेलन: 26-27 नवंबर 1935 को हाजीपुर में स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में हुआ, जिसमें जमींदारी प्रथा को हटाने का प्रस्ताव पास किया गया
ये आंदोलन ब्रिटिश नीतियों (जैसे जमींदारी, रैयतवाड़ी) से उत्पन्न शोषण के विरुद्ध थे, जो किसानों को मजदूरों में बदल रहे थे। स्वतंत्रता के बाद भी (1950s में सीपीआई के नेतृत्व में) ये जारी रहे, लेकिन नक्सलवाद (1960s-70s) ने हिंसक रूप दिया।
चंपारण सत्याग्रह के कारण
- बिहार के चंपारण क्षेत्र के कई किसानों को ब्रिटिश शासन के दौरान अपनी ज़मीन पर नील की खेती करने के लिए मजबूर किया गया था, जिससे उन्हें बहुत दुःख हुआ। राजकुमार शुक्ला ही वह व्यक्ति थे जिन्होंने महात्मा गांधी को चंपारण आने के लिए राजी किया, जिसके बाद सत्याग्रह शुरू हुआ।
- 1916 में लखनऊ में हुए प्रथम कांग्रेस अधिवेशन में बिहार के कई राजनेताओं ने महात्मा गांधी को संबोधित करते हुए अनुरोध किया कि वे चंपारण में किसानों पर हो रहे अत्याचारों के विरुद्ध आंदोलन चलाएं। उन्होंने वादा किया कि वे उनसे मिलने ज़रूर जाएँगे। 10 अप्रैल, 1917 को वे पहली बार पटना पहुँचे और पाँच दिन बाद, मुज़फ़्फ़रपुर से चंपारण के ज़िला मुख्यालय मोतिहारी पहुँचे। 17 अप्रैल सत्याग्रह की तारीख़ थी। इसी दिन गांधीजी ने नील की खेती करने वाले किसानों की स्थिति सुधारने के लिए सत्याग्रह शुरू किया और ब्रिटिश प्रशासन के विरोध में भारत के पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की।
- गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में स्वीकार किया: “मुझे यह स्वीकार करना चाहिए कि तब मुझे चंपारण का नाम भी नहीं पता था, भौगोलिक स्थिति तो दूर की बात थी, और मुझे नील की खेती के बारे में भी शायद ही कोई जानकारी थी”
चंपारण सत्याग्रह के कारण –
- चंपारण और वास्तव में पूरे बिहार में भूमि लगान में भारी वृद्धि हुई।
- किसानों को नील की खेती करने के लिए मजबूर किया गया, जिससे अन्य फसलों की खेती करने की उनकी क्षमता सीमित हो गई।
- उनसे यह भी अपेक्षा की जाती थी कि वे अपना सारा समय और प्रयास जमींदार द्वारा चुनी गई फसलों पर लगाएं।
- किसानों को बहुत कम मज़दूरी दी जाती थी। उनके लिए इस मामूली मज़दूरी पर गुज़ारा करना बेहद मुश्किल था।
- किसानों को अपनी भूमि का सर्वोत्तम भाग जमींदारों की इच्छानुसार विशिष्ट फसलें उगाने में खर्च करने के लिए मजबूर किया जाता था।
गाँधी जी के हस्तक्षेप की प्रमुख विशेषताएँ:
- सत्याग्रह और अहिंसक प्रतिरोध का प्रारंभ: गाँधी जी ने 10 अप्रैल 1917 को मुजफ्फरपुर पहुँचकर स्थिति का सर्वेक्षण किया। 15 अप्रैल को चंपारण प्रवेश पर ब्रिटिश अधिकारियों ने निष्कासन आदेश दिया, लेकिन गाँधी जी ने इसे अस्वीकार कर पहली बार भारत में सविनय अवज्ञा का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, “मैं दंड भुगतने को तैयार हूँ, लेकिन आदेश मानने को नहीं।“ यह अहिंसक प्रतिरोध की नींव रखी, जो बाद के असहयोग, सविनय अवज्ञा और भारत छोड़ो आंदोलनों का आधार बनी।
- तथ्य-आधारित जाँच और दस्तावेजीकरण: गाँधी जी ने 850 गाँवों का दौरा कर 8,000 से अधिक किसानों के बयान दर्ज किए। उन्होंने बिहार प्लांटर्स एसोसिएशन और तिरहुत डिवीजन के आयुक्त को सूचित किया। सहयोगियों (जैसे राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, जे.बी. कृपलानी) के साथ उन्होंने शोषण के प्रमाण संग्रहित किए, जो आंदोलन को वैधता प्रदान किया।
- वार्ता और समिति गठन: जून 1917 में चंपारण कृषि जाँच समिति का गठन हुआ, जिसमें गाँधी जी सदस्य बने। समिति की सिफारिशों पर 25% अवैध वसूलियों की वापसी, तीनकठिया प्रथा का उन्मूलन और लगान वृद्धि सीमा तय हुई। 1918 का चंपारण कृषि अधिनियम पारित हुआ, जो किसानों को फसल चयन की स्वतंत्रता देता था।
- रचनात्मक कार्य और सामाजिक सुधार: आंदोलन केवल राजनीतिक नहीं था; गाँधी जी ने गाँवों में स्कूल, स्वच्छता और स्वास्थ्य सुविधाएँ स्थापित कीं। उन्होंने किसानों में आत्मविश्वास जगाया, भय हटाया और उन्हें संगठित किया। यह ‘सर्वोदय’ की अवधारणा का प्रारंभ था, जहाँ शोषण के साथ-साथ सामाजिक उत्थान पर जोर दिया गया।
- राष्ट्रीय प्रभाव: यह आंदोलन मध्यमार्गी (ब्रिटिश व्यवस्था में भागीदारी) और उग्रवादी (हिंसा) के बीच पुल का काम किया। इसने युवाओं को दिशा दी और गाँधी जी को राष्ट्रीय नेता बनाया। दस वर्षों में नील कारखाने बंद हो गए, और किसान अधिक साहसी बने।
- गाँधी जी का हस्तक्षेप विशेष रूप से इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि यह किसानों की स्थानीय शिकायत को राष्ट्रीय मुद्दे में बदल दिया, बिना हिंसा के सफलता प्राप्त की और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की दिशा निर्धारित की।
आंदोलन की सफलता और परिणाम-
- सरकारी समिति का गठन: गांधी जी के निरंतर दबाव और व्यापक जन समर्थन के कारण अंग्रेज सरकार को एक जांच आयोग नियुक्त करना पड़ा, जिसमें गांधी जी को भी सदस्य बनाया गया।
- तिनकठिया प्रणाली का अंत: आयोग की सिफारिशों के आधार पर कानून बनाकर तिनकठिया प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। 135 वर्षों से चली आ रही नील की जबरदस्ती खेती हमेशा के लिए बंद हो गई।
- किसानों को भूमि अधिकार: नीलहे किसान अब अपनी जमीन के वास्तविक मालिक बने।
अन्य महत्वपूर्ण तथ्य –
- चंपारण के एक कृषक राजकुमार शुक्ल अपने साथी किसानों की स्थिति देखकर दुखी थे। यूरोपीय बागान मालिकों ने तिनकठिया प्रथा लागू की थी, जिसके तहत किसानों को अपनी कुल ज़मीन के 3/20वें हिस्से पर नील की खेती करनी पड़ती थी। अठारहवीं सदी के अंत तक, जर्मनी से आने वाले कृत्रिम रंगों ने नील की जगह ले ली थी, और यूरोपीय बागान मालिक किसानों से भारी लगान और अवैध कर वसूल रहे थे।
- चंपारण में अस्थिरता का एक प्रमुख कारण लोगों की अमानवीय जीवनशैली थी। जब गांधीजी चंपारण आए, तो उन्हें किसानों की दयनीय गरीबी देखकर बहुत दुःख हुआ।
- गांधीजी और उनके वकीलों ने पूरे क्षेत्र के कई गांवों का दौरा किया, किसानों से मुलाकात की और जबरन नील उत्पादन के बारे में उनकी शिकायतें सुनीं।
- चंपारण पहुँचते ही अंग्रेज़ शासकों ने गांधीजी की गतिविधियों पर कड़ी नज़र रखनी शुरू कर दी। अंततः 15 अप्रैल को कमिश्नर ने उन्हें मोतिहारी में चंपारण छोड़ने की चेतावनी दे दी।
- गांधीजी ने कहा कि वह यहां से नहीं जाएंगे, लेकिन वह “सविनय अवज्ञा की सजा” भुगतने को तैयार हैं।
- यह स्पष्ट था कि गांधीजी को उनकी अवज्ञा के परिणामस्वरूप जेल जाना पड़ेगा। परिणामस्वरूप, चंपारण के काश्तकारों ने बड़ी संख्या में जेल, पुलिस थानों और अदालतों के बाहर प्रदर्शन किया।
- इस अभूतपूर्व प्रकार के अहिंसक प्रतिरोध से चिंतित होकर सरकार को गांधीजी को रिहा करने के लिए मजबूर होना पड़ा।
- लड़ाई जारी रही, और सविनय अवज्ञा भी जारी रही। विरोध प्रदर्शनों और भूख हड़तालों के परिणामस्वरूप अंततः तिनकठिया प्रथा, या नील की खेती, समाप्त कर दी गई।
- ब्रिटिश सरकार ने जमींदारों को एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया, जिससे किसानों को अन्य बातों के अलावा अपनी जमीन पर क्या खेती करनी है, इस पर अधिक विवेकाधिकार मिल गया।
- लेफ्टिनेंट गवर्नर की परिषद ने चंपारण की कृषि स्थितियों की जांच के लिए एक जांच समिति गठित करने का निर्णय लिया, जिसके सदस्यों में गांधीजी भी शामिल थे।
- 4 अक्टूबर 1917 को समिति ने सरकार के समक्ष अपने निष्कर्ष प्रस्तुत किये, जिसमें तिनकठिया प्रणाली को समाप्त करने और रैयतों को एक-चौथाई तावान की प्रतिपूर्ति का प्रस्ताव रखा गया।
- समिति ने अवैध उपकर (अबवाब) के संग्रह को समाप्त करने की सिफारिश की तथा नील की खेती के लिए स्वैच्छिक समझौतों की वकालत की, जिसमें अवधि को तीन वर्ष तक सीमित किया गया तथा किसानों को नील की खेती के लिए खेत चुनने का अधिकार दिया गया।
- सरकार ने समिति के अधिकांश सुझावों को स्वीकार कर लिया, जिसके परिणामस्वरूप 1918 में चंपारण कृषि अधिनियम पारित हुआ। परिणामस्वरूप, सदियों पुरानी तिनकठिया प्रथा समाप्त कर दी गई।
- चंपारण कृषि अधिनियम 1918, पर हस्ताक्षर किए गए उसी वर्ष 1 मई को भारत के गवर्नर जनरल द्वारा नियुक्त किया गया यह निर्णय किसानों के हितों की रक्षा करने वाले आंदोलन का एक महत्वपूर्ण परिणाम था।
- चंपारण आंदोलन को भारत के वामपंथी आंदोलन के नेता ईएमएस नंबूदरीपाद द्वारा राष्ट्रवाद के निर्माण में योगदान के रूप में देखा गया।
- कुछ शिक्षाविदों का मानना था कि चंपारण आंदोलन सफल नहीं था।
- यह आंदोलन किसानों के शोषण और भेदभाव के विरुद्ध आवाज उठाने में विफल रहा।
- उदाहरण के लिए, रमेश चंद्र दत्त ने तर्क दिया कि सरकार और किसानों के बीच हुए समझौतों में हमारे ग्रामीणों का ज़मींदारी शोषण शामिल नहीं था। उन्होंने यह भी कहा कि चंपारण में महात्मा गांधी के आंदोलन का परिणाम चंपारण के किसानों की भयानक गरीबी और दुर्दशा के प्रमुख कारणों, यानी अत्यधिक लगान और अत्यधिक कर्ज़ के विरुद्ध संघर्ष के रूप में नहीं निकला।
The peasant movements in Bihar were mainly related to indigo cultivation, against whose compulsion the peasants rebelled, especially in Champaran under the Tinkathia system where forced indigo farming was required. Gandhi intervened in Champaran at the insistence of Rajkumar Shukla, where through Satyagraha, he ended the Tinkathia system and protected the peasants’ rights. The peasant movements in Bihar were mainly centered in the British colonial period (19th-20th century), which were against the zamindari system, high rents, illegal exactions (abwabs), begar (forced labor), forced indigo cultivation, and land grabbing. Since Bihar’s economy was agriculture-based (about 96% of the population dependent on agriculture), these movements were inspired by rural exploitation, land inequality, and economic distress. Early movements were local and unorganized, but in the 20th century, they connected with national movements, making them more organized. These included tribal rebellions (such as Santhal and Munda), which became part of the peasant movements. These movements strengthened the freedom struggle and laid the foundation for land reforms (such as the abolition of zamindari).
Brief Description of Major Peasant Movements
The major peasant movements in Bihar include the following:
- Indigo Rebellion (1859-60): In the Champaran, Tirhut, and Saran regions of Bihar against forced indigo cultivation and low prices. Cause: Exploitation of peasants by British indigo factories. Leaders: Local peasants. Outcome: Formation of the Indigo Commission in 1860, but no complete success.
- Pandoul Rebellion (1866-67): The first peasant rebellion in Bihar occurred in 1866-67 in Pandoul village of Madhubani district. It fell under the Darbhanga Commissary and began in opposition to the increasing atrocities of zamindars.
- Santhal Rebellion (1855-56): In Santhal Pargana against zamindars, moneylenders, and outsider traders. Causes: Land grabbing and high interest. Leaders: Sidhu-Kanhu. Outcome: British suppression, but establishment of Santhal Pargana.
- Munda Rebellion (1899-1900): In Chotanagpur against land inequality and outsider interference. Causes: Violation of traditional land practices. Leader: Birsa Munda. Outcome: Suppression, but Chotanagpur Tenancy Act 1908.
- Movement Against Darbhanga Raj (1919-20): Against high land revenue by Darbhanga Raj. Causes: Economic pressure after World War I. Leader: Swami Vidyannand. Outcome: Widespread support, but limited success.
- Bakast Movement (1930s): Against bakast land (land re-grabbed from tenants) by zamindars. Causes: Land rehabilitation and begar. Leader: Swami Sahajanand Saraswati (Bihar Provincial Kisan Sabha, 1929). Outcome: Satyagraha and protests; Congress gained rural base.
- Dalmia Sugar Factory Movement (1938-39): Against labor exploitation. Causes: Atrocities on workers. Leader: Kisan Sabha. Outcome: Movement suppressed, but worker awakening.
- Bihar Provincial Kisan Sabha (1929) - Role of Swami Sahajanand Saraswati: In 1929, Swami Sahajanand Saraswati established the Bihar Provincial Kisan Sabha. It was formed at the Sonpur Mela in Saran district. Its main objectives were:
- Abolition of the zamindari system
- Protection of peasants’ rights
- Reduction in land revenue
- Institutional arrangement for loans
Kisan Sabha Conferences:
- First Conference: Held on November 17, 1929, under the chairmanship of Swami Sahajanand Saraswati in Sonpur
- Second Conference: Held in August 1934 under the chairmanship of Purushottam Das Tandon, in which Khan Abdul Ghaffar Khan also participated
- Third Conference: Held on November 26-27, 1935, in Hajipur under the chairmanship of Swami Sahajanand Saraswati, where a resolution to abolish the zamindari system was passed
- These movements were against British policies (such as zamindari and ryotwari) that were turning peasants into laborers. Even after independence (in the 1950s under CPI leadership), they continued, but Naxalism (1960s-70s) gave them a violent form.
Causes of Champaran Satyagraha
Many peasants in Bihar’s Champaran region were forced to cultivate indigo on their land during British rule, which caused them great suffering. Rajkumar Shukla was the person who convinced Mahatma Gandhi to come to Champaran, after which the Satyagraha began.
In 1916, at the First Congress Session in Lucknow, many politicians from Bihar addressed Mahatma Gandhi and requested him to launch a movement against the atrocities on peasants in Champaran. He promised that he would definitely meet them. On April 10, 1917, he arrived in Patna for the first time and five days later, reached the district headquarters Motihari in Champaran from Muzaffarpur. April 17 was the date of Satyagraha. On the same day, Gandhi started Satyagraha to improve the condition of peasants cultivating indigo and began India’s first civil disobedience movement against the British administration.
Gandhi acknowledged in his autobiography: “I must admit that I did not even know the name of Champaran at that time, let alone its geographical location, and I probably had little knowledge about indigo cultivation.”
Causes of Champaran Satyagraha –
- There was a heavy increase in land rent in Champaran and indeed throughout Bihar.
- Peasants were forced to cultivate indigo, which limited their ability to grow other crops.
- They were also expected to devote all their time and effort to the crops chosen by the zamindars.
- Peasants were given very low wages. It was extremely difficult for them to survive on this meager wage.
- Peasants were forced to spend the best part of their land on specific crops according to the wishes of the zamindars.
Key Features of Gandhi’s Intervention:
- Beginning of Satyagraha and Non-Violent Resistance: Gandhi arrived in Muzaffarpur on April 10, 1917, to survey the situation. On April 15, upon entering Champaran, British officials issued an expulsion order, but Gandhi refused it, setting the first example of civil disobedience in India. He said, “I am ready to suffer punishment, but not to obey the order.” This laid the foundation for non-violent resistance, which became the basis for later Non-Cooperation, Civil Disobedience, and Quit India Movements.
- Fact-Based Investigation and Documentation: Gandhi visited 850 villages and recorded statements from over 8,000 peasants. He informed the Bihar Planters Association and the Commissioner of Tirhut Division. With associates (such as Rajendra Prasad, Brajkishore Prasad, Anugrah Narayan Sinha, J.B. Kripalani), he collected evidence of exploitation, which gave legitimacy to the movement.
- Negotiation and Committee Formation: In June 1917, the Champaran Agrarian Inquiry Committee was formed, with Gandhi as a member. Based on the committee’s recommendations, 25% refund of illegal exactions, abolition of the Tinkathia system, and limits on rent increases were set. The Champaran Agrarian Act 1918 was passed, which gave peasants freedom to choose crops.
- Constructive Work and Social Reforms: The movement was not only political; Gandhi established schools, sanitation, and health facilities in villages. He instilled confidence in peasants, removed fear, and organized them. This was the beginning of the ‘Sarvodaya’ concept, where emphasis was placed on social upliftment along with ending exploitation.
- National Impact: This movement acted as a bridge between moderates (participation in British system) and extremists (violence). It gave direction to the youth and made Gandhi a national leader. Within ten years, indigo factories closed, and peasants became more courageous.
- Gandhi’s intervention was particularly important because it transformed a local peasant grievance into a national issue, achieved success without violence, and determined the direction of the Indian freedom struggle.
Success and Outcomes of the Movement –
- Formation of Government Committee: Due to Gandhi’s continuous pressure and widespread public support, the British government had to appoint an inquiry commission, in which Gandhi was also made a member.
- End of Tinkathia System: Based on the commission’s recommendations, a law was made to abolish the Tinkathia system. The forced indigo cultivation, which had been going on for 135 years, was permanently stopped.
- Land Rights to Peasants: Indigo peasants now became the real owners of their land.
Other Important Facts –
- A farmer from Champaran, Rajkumar Shukla, was distressed seeing the condition of his fellow peasants. European plantation owners had implemented the Tinkathia system, under which peasants had to cultivate indigo on 3/20th of their total land. By the end of the 18th century, artificial dyes from Germany had replaced indigo, and European plantation owners were collecting heavy rents and illegal taxes from peasants.
- A major cause of unrest in Champaran was the inhuman lifestyle of the people. When Gandhi came to Champaran, he was deeply saddened to see the miserable poverty of the peasants.
- Gandhi and his lawyers visited many villages in the entire region, met with peasants, and heard their complaints about forced indigo production.
- As soon as he reached Champaran, the British rulers began to keep a strict watch on Gandhi’s activities. Finally, on April 15, the commissioner warned him to leave Champaran in Motihari.
- Gandhi said that he would not go from here, but he was ready to “suffer the punishment of civil disobedience.”
- It was clear that Gandhi would have to go to jail as a result of his disobedience. As a result, a large number of Champaran tenants demonstrated outside jails, police stations, and courts.
- Disturbed by this unprecedented form of non-violent resistance, the government was forced to release Gandhi.
- The fight continued, and civil disobedience also continued. As a result of protest demonstrations and hunger strikes, the Tinkathia system, or indigo cultivation, was finally abolished.
- The British government was forced to make the zamindars sign an agreement, which gave peasants, among other things, greater discretion over what to cultivate on their land.
- The Lieutenant Governor’s Council decided to form an inquiry committee to investigate the agricultural conditions in Champaran, in which Gandhi was also included as a member.
- On October 4, 1917, the committee presented its findings to the government, proposing the abolition of the Tinkathia system and compensation of one-fourth to the ryots.
- The committee recommended the abolition of the collection of illegal cesses (abwabs) and advocated voluntary agreements for indigo cultivation, limiting the duration to three years and giving peasants the right to choose fields for indigo cultivation.
- The government accepted most of the committee’s suggestions, as a result of which the Champaran Agrarian Act 1918 was passed. Consequently, the age-old Tinkathia system was abolished.
- The Champaran Agrarian Act 1918 was signed on May 1 of the same year by the Governor General of India. This decision was an important outcome of the movement that protected the interests of the peasants.
- The Champaran Movement was seen by left-wing movement leader EMS Namboodiripad as a contribution to the construction of nationalism.
- Some academics believed that the Champaran Movement was not successful.
- It failed to raise a voice against the exploitation and discrimination of peasants.
- For example, Ramesh Chandra Dutt argued that the agreements between the government and peasants did not include zamindari exploitation of our villagers. He also said that the outcome of Mahatma Gandhi’s movement in Champaran did not emerge as a struggle against the main causes of the terrible poverty and misery of Champaran peasants, namely excessive rent and excessive debt.
2. ans.
पंचायती राज भारत की ग्रामीण स्थानीय स्वशासन व्यवस्था है, जो संवैधानिक रूप से 73वें संशोधन अधिनियम, 1992 के माध्यम से स्थापित की गई। यह व्यवस्था प्राचीन भारतीय परंपरा 'ग्राम स्वराज' से प्रेरित है, जिसका उद्देश्य सत्ता का विकेंद्रीकरण करना और ग्रामीण स्तर पर लोकतांत्रिक भागीदारी सुनिश्चित करना है। पंचायती राज को 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में प्रारंभिक रूप से शुरू किया गया था, लेकिन संवैधानिक मान्यता ने इसे पूरे देश में लागू किया। यह 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 विषयों (जैसे कृषि, सिंचाई, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि) पर कार्य करता है।भारत में, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन और विकास प्रणाली को पंचायती राज कहा जाता है। इसे भारत के सभी राज्यों में राज्य विधानमंडल अधिनियमों द्वारा जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया था।
भारत में, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन और विकास प्रणाली को पंचायती राज (panchayati raj in hindi) कहा जाता है। इसे भारत के सभी राज्यों में राज्य विधानमंडल अधिनियमों द्वारा जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया था। इसे 1992 के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में शामिल किया गया था।
पंचायती राज ग्रामीण भारत में स्थानीय स्वशासन की एक प्रणाली है। इसमें पंचायती राज संस्थाएँ (PRI) शामिल हैं जो गाँवों पर शासन करती हैं और सरकारी योजनाओं को लागू करती हैं। इस प्रणाली को भारतीय संविधान के भाग IX में परिभाषित किया गया है और यह विभिन्न स्तरों पर संचालित होती है। इसमें गाँव स्तर पर ग्राम पंचायतें, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद शामिल हैं। पंचायती राज का उद्देश्य आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय और जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को बढ़ावा देना है।
भारत में पंचायती राज का विकास -
- वैदिक साहित्य में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन संस्थाओं की संगठित प्रणाली के कई संदर्भ मिलते हैं। ग्रामीण स्थानीय निकाय किस प्रकार कार्य करते हैं, इसे सुसंगत रूप से समझाने के लिए विभिन्न संदर्भों को एक साथ बुनना चुनौतीपूर्ण है।
- वैदिक राज्य, जो एक ग्रामीण राज्य था, में गांव प्राथमिक प्रशासनिक इकाई के रूप में कार्य करता था।
- ग्रामिनी एक प्रमुख ग्राम अधिकारी का नाम था। वह राजा के राज्याभिषेक समारोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला एक सम्मानित अधिकारी था।
- रामायण और महाभारत जैसे प्रमुख महाकाव्यों में ग्राम संस्थाओं का प्रत्यक्ष उल्लेख बहुत कम मिलता है।
- चोल काल स्थानीय स्वशासन का सबसे सर्वोत्तम उदाहरण है।
- मुस्लिम काल में कुछ नई अवधारणाएँ भारतीय धरती पर आईं। नए शासकों ने नई प्रथाओं और मान्यताओं को अपनाया।
- मुक्कद्दम गांव का प्रशासन संभालता था, पटवारी राजस्व संग्रह का काम संभालता था, और चौधरी पंच के सहयोग से विवाद समाधान का काम संभालते थे।
- कराधान और भूमि प्रबंधन के संबंध में काफी मतभेद थे।
- जिला स्तर पर प्रशासन का नियंत्रण था। गांव के समुदाय कायम रहे।
- इन बस्तियों को अपनी सीमाओं के अंदर पर्याप्त स्वशासन का अधिकार प्राप्त था।
- ब्रिटिश शासन ने ग्राम समुदायों की दीर्घकालिक आर्थिक आत्मनिर्भरता को कमजोर कर दिया तथा सामुदायिक भावना को गंभीर क्षति पहुंची।
- गांव में उपभोग के लिए उत्पादन की जगह बाजार के लिए उत्पादन ने ले ली। गांव के कलाकारों और शिल्पकारों की प्रमुखता खत्म हो गई। उन्हें अच्छे वेतन वाली नौकरियों की तलाश में अपने गांव छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा।
- परिणामस्वरूप, ग्राम पंचायतों ने अपनी स्वतंत्रता और बस्तियों के बीच परस्पर सम्पर्क खो दिया।
- अंग्रेजों ने कुछ ऐसी प्रशासनिक पद्धतियां अपनाईं जिनसे ग्रामीण समुदायों का विनाश और तेज हो गया।
- वास्तव में, ये सभी उन समुदायों की विशेषताएं हैं जो प्रशासनिक ढांचे में ब्रिटिश संशोधनों के परिणामस्वरूप बुरी स्थिति में आ गए हैं।
- भारतीय गांवों में लंबे समय से प्रचलित पंचायती राज की गिरावट का कारण केन्द्रीकरण को माना जा सकता है।
स्वतंत्रता के बाद का युग-
- पंचायती राज व्यवस्था ने अपना वर्तमान स्वरूप पहली बार स्वतंत्रता के बाद 1959 में अपनाया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पंचायतों को लोगों के स्वामित्व वाली व्यवस्था माना जाता था। लोकतंत्र की सच्ची आवाज़ होने के कारण स्थानीय स्वशासन को आवश्यक माना जाता था।
- महात्मा गांधी ने विशेष रूप से कहा था कि स्वतंत्रता की शुरुआत जमीनी स्तर से होनी चाहिए। हर गांव एक गणतंत्र (ग्राम स्वराज) होना चाहिए, जिसमें एक पंचायत के पास पूरा अधिकार हो।
उद्देश्य:
- जमीनी लोकतंत्र को बढ़ावा देना: स्थानीय स्तर पर लोगों को सीधे शासन में भाग लेने और निर्णय लेने का अधिकार प्रदान करना।
- ग्रामीण समुदायों का सशक्तिकरण: ग्रामीणों को अपनी समस्याओं और जरूरतों का समाधान करने के लिए सशक्त बनाना।
- लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण: शक्ति और संसाधनों को केंद्र से स्थानीय स्तर पर वितरित करना, जिससे लोगों की भागीदारी बढ़े।
- सामाजिक-आर्थिक प्रगति: ग्रामीण क्षेत्रों में तीव्र सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना।
- न्याय प्रदान करना: स्थानीय स्तर पर निष्पक्ष न्याय और सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
गांधी जी के ग्राम स्वराज की अवधारणा -
- महात्मा गांधी का मानना था कि "भारत गांवों में बसता है" और वास्तविक स्वराज तभी आ सकता है जब हर गांव एक गणराज्य बने। उनके अनुसार:
- प्रत्येक ग्राम पंचायत के पास पूर्ण अधिकार होने चाहिए।
- ग्राम स्वराज से ही वास्तविक और शक्तिशाली लोकतंत्र की स्थापना हो सकती है।
- सत्ता का विकेंद्रीकरण ग्रामीण स्तर से राष्ट्रीय स्तर तक होना चाहिए।
व्यापक प्रभाव और महत्व -
- लोकतांत्रिक सशक्तिकरण- पंचायती राज ने ग्रामीण भारत में लोकतांत्रिक भागीदारी को बढ़ावा दिया है। विशेषकर महिलाओं की नेतृत्व क्षमता का विकास हुआ है।
- सामाजिक न्याय -कमजोर वर्गों, विशेषकर महिलाओं, दलितों और आदिवासियों की राजनीतिक भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
- विकास में जनभागीदारी - स्थानीय समुदाय अब अपने विकास की योजना बनाने और उसे लागू करने में प्रत्यक्ष भूमिका निभाता है।
- प्रशासनिक दक्षता- जमीनी स्तर पर समस्याओं की पहचान और समाधान में तेजी आई है, जिससे प्रशासनिक दक्षता में वृद्धि हुई है।
- पंचायती राज व्यवस्था ने भारतीय लोकतंत्र को मजबूत बनाने, ग्रामीण विकास को गति देने और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के सपने को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
पंचायती राज की प्रमुख विशेषताएं
संवैधानिक आधार-
भाग IX: संविधान में अनुच्छेद 243 से 243(O) तक के प्रावधान जोड़े गए।11वीं अनुसूची: पंचायतों के अधिकार क्षेत्र में 29 विषय शामिल किए गए।
उदाहरण के लिए - कृषि और कृषि विस्तार, भूमि विकास और भूमि सुधार, लघु सिंचाई और जल प्रबंधन, पशुपालन और डेयरी, इत्यादि।
त्रिस्तरीय संरचना-
- ग्राम स्तर: ग्राम पंचायत - प्रत्यक्ष चुनाव से गठित
- मध्यवर्ती स्तर: पंचायत समिति/क्षेत्र पंचायत - 20 लाख से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों के लिए
- जिला स्तर: जिला पंचायत - सभी राज्यों में अनिवार्य
ग्राम सभा की भूमिका- ग्राम सभा को लोकतांत्रिक व्यवस्था की आधारभूत इकाई माना गया है। इसमें पंचायत क्षेत्र के सभी पंजीकृत मतदाता शामिल होते हैं।
चुनावी व्यवस्था-
- प्रत्यक्ष चुनाव: सभी स्तरों पर सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है
- अप्रत्यक्ष चुनाव: मध्यवर्ती और जिला स्तर पर अध्यक्षों का चुनाव निर्वाचित सदस्यों में से
- राज्य निर्वाचन आयोग: स्वतंत्र चुनाव आयोग द्वारा चुनाव संचालन
आरक्षण प्रावधान -
- अनुसूचित जाति/जनजाति: जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण
- महिला आरक्षण: कुल सीटों में कम से कम एक तिहाई महिलाओं के लिए आरक्षित
- अध्यक्ष पदों का आरक्षण: सभी स्तरों पर अध्यक्ष पदों में भी आरक्षण
- कार्यकाल- प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित है। यदि किसी पंचायत को विघटित किया जाता है, तो 6 महीने के भीतर नए चुनाव कराना अनिवार्य है।
वित्तीय शक्तियां-
- कर लगाने का अधिकार: राज्य सरकार पंचायतों को उचित कर लगाने का अधिकार दे सकती है
- राज्य वित्त आयोग: प्रत्येक 5 वर्ष में पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए
- अनुदान: राज्य की संचित निधि से अनुदान प्राप्त करने का अधिकार
- न्यायिक सुरक्षा -चुनावी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप पर प्रतिबंध, केवल निर्दिष्ट प्राधिकरण के समक्ष ही चुनाव को चुनौती दी जा सकती है।
अन्य महत्वपूर्ण जानकारी -
73वें संशोधन अधिनियम के संवैधानिक प्रावधान
- 1992 में अधिनियम लागू होने से बहुत पहले ही भारत में ग्राम पंचायतें पहले से ही प्रचलन में थीं, लेकिन इस प्रणाली में कई खामियाँ थीं जो इसे लोगों की सरकार के रूप में काम करने या उनकी माँगों पर प्रतिक्रिया देने से रोकती थीं। इसके कई कारण थे, जिनमें फंडिंग की कमी, नियमित चुनावों का अभाव और महिलाओं और अनुसूचित जातियों और जनजातियों जैसे कमज़ोर समूहों का कम प्रतिनिधित्व शामिल था।
- भारतीय संविधान के राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुच्छेद 40 में यह प्रावधान है कि सरकार ग्राम पंचायतों के लिए खुद को स्थापित करना और प्रभावी ढंग से काम करना आसान बनाए। इन समस्याओं को हल करने और स्थानीय स्वशासन को बढ़ाने के लिए भारत की केंद्र सरकार ने 1992 में 73वां संशोधन अधिनियम पेश किया। दोनों सदनों ने कानून को मंजूरी दी और 24 अप्रैल, 1993 को लागू हुआ। पंचायतें एक नया अध्याय है जो इस अधिनियम के परिणामस्वरूप संविधान में जोड़ा गया।
73वें संविधान संशोधन अधिनियम का महत्व-
- इस अधिनियम द्वारा संविधान में ग्यारहवीं अनुसूची को जोड़ा गया, जिसमें पंचायतों के 29 कार्यात्मक विषय शामिल हैं, साथ ही भाग IX, "पंचायतें" को भी जोड़ा गया।
- संविधान के भाग IX में अनुच्छेद 243 से 243O तक शामिल हैं।
- संशोधन अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 40 (राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत) को अभिव्यक्ति प्रदान करता है, जिसमें राज्य से ग्राम पंचायतों की स्थापना करने तथा उन्हें स्वायत्तता प्रदान करने का आह्वान किया गया है, ताकि वे स्वशासी इकाइयों के रूप में कार्य कर सकें।
- अधिनियम के पारित होने के साथ ही, पंचायती राज व्यवस्था अब संविधान के न्यायोचित प्रावधानों द्वारा शासित होगी और प्रत्येक राज्य को इसे लागू करना होगा। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार की प्राथमिकताओं की परवाह किए बिना पंचायती राज संस्थाओं के लिए चुनाव कराए जा सकेंगे।
- अधिनियम दो भागों में विभाजित है: वैकल्पिक और अनिवार्य। राज्य के कानूनों में संशोधन करके अनिवार्य धाराएँ शामिल की जानी चाहिए, जिसमें नए पंचायती राज ढाँचे की स्थापना शामिल है। दूसरी ओर, राज्य सरकार के पास स्वैच्छिक प्रावधानों पर विवेकाधिकार है।
- अधिनियम के परिणामस्वरूप प्रतिनिधि लोकतंत्र का स्थान भागीदारी लोकतंत्र ने ले लिया है।
पेसा अधिनियम 1996
- 1996 का पेसा अधिनियम, पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 है। यह एक ऐसा कानून है जो भारत में पंचायती राज के प्रावधानों को अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तारित करता है।
- अनुसूचित क्षेत्र वे क्षेत्र हैं जहाँ मुख्य रूप से आदिवासी समुदाय निवास करते हैं। पेसा अधिनियम इन आदिवासी समुदायों को सशक्त बनाता है।
- यह उन्हें शासन और निर्णय लेने में स्वायत्तता प्रदान करता है। यह आदिवासी समुदायों के पारंपरिक रीति-रिवाजों और सामाजिक प्रथाओं को मान्यता देता है। यह उन्हें अपने संसाधनों का प्रबंधन करने, अपनी संस्कृति की रक्षा करने और अपने सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की अनुमति देता है।
- यह अधिनियम अपने क्षेत्रों में विकास कार्यक्रमों की योजना, कार्यान्वयन और निगरानी में जनजातीय समुदायों की भागीदारी पर जोर देता है।
- इसका उद्देश्य जनजातीय समुदायों के अधिकारों और हितों की रक्षा करना तथा उनका स्वशासन सुनिश्चित करना है।
पंचायती राज से संबंधित महत्वपूर्ण समितियाँ -
- पंचायती राज व्यवस्था के विकास, संरचना और सशक्तिकरण के लिए भारत सरकार ने समय-समय पर विभिन्न समितियों का गठन किया। ये समितियाँ ग्रामीण स्थानीय स्वशासन को मजबूत बनाने, विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देने और पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाईं। निम्नलिखित प्रमुख समितियाँ हैं, जो कालानुक्रमिक क्रम में वर्णित हैं:
- बलवंत राय मेहता समिति (1957):प्रथम राष्ट्रीय स्तर की समिति, जिसने पंचायती राज को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का आधार बनाया। प्रमुख सिफारिशें: तीन-स्तरीय संरचना (ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद), ग्राम सभा का गठन, पंचायतों को विकास कार्यों की जिम्मेदारी और नियमित चुनाव। इसकी सिफारिशों से 1959 में राजस्थान में पहली पंचायती राज व्यवस्था शुरू हुई।
- अशोक मेहता समिति (1977):पंचायती राज की कमजोरियों का मूल्यांकन करने के लिए गठित। प्रमुख सिफारिशें: दो-स्तरीय संरचना (जिला परिषद और मंडल पंचायत), राजनीतिक दलों की भागीदारी, पंचायतों को कर लगाने का अधिकार, ग्राम सभा को सशक्त बनाना और जिला स्तर पर कार्यकारी भूमिका। यह समिति पंचायतों को अधिक राजनीतिक स्वायत्तता देने पर जोर देती थी।
- जी.वी.के. राव समिति (1985):योजना आयोग द्वारा गठित, जो प्रशासनिक व्यवस्था की समीक्षा करती थी। प्रमुख सिफारिशें: जिला स्तर को विकास योजना का केंद्र बनाना, नियमित चुनाव सुनिश्चित करना, पंचायतों को वित्तीय स्वायत्तता प्रदान करना और प्रशासनिक दक्षता बढ़ाना। इसने 'जिला ग्राम स्वराज' की अवधारणा प्रस्तुत की।
- एल.एम. सिंहवी समिति (1986):पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने पर केंद्रित। प्रमुख सिफारिशें: पंचायतों को संवैधानिक मान्यता, राज्य पंचायत आयोग का गठन, ग्राम सभा को विधायी शक्ति, न्यायिक पंचायतों की स्थापना और प्रशिक्षण कार्यक्रम। इसकी सिफारिशों ने 73वें संवैधानिक संशोधन (1992) का आधार तैयार किया।
अन्य उल्लेखनीय समितियाँ-
- गड़गिल समिति (1959): पंचायती राज के वित्तीय संसाधनों पर सिफारिशें।
- सरकारिया आयोग (1988): संघ-राज्य संबंधों के संदर्भ में पंचायतों की भूमिका पर चर्चा।
- पी.के. थुंगन समिति (1989): नगरपालिका एवं पंचायती राज पर।
ये समितियाँ पंचायती राज को प्राचीन ग्राम स्वराज से आधुनिक लोकतांत्रिक संस्था तक विकसित करने में मील का पत्थर साबित हुईं, जिससे ग्रामीण भारत में सत्ता का विकेंद्रीकरण संभव हुआ।
Panchayati Raj is India's rural local self-governance system, constitutionally established through the 73rd Constitutional Amendment Act, 1992. This system is inspired by the ancient Indian tradition of 'Gram Swaraj', with the objective of decentralizing power and ensuring democratic participation at the rural level. Panchayati Raj was initially launched on October 2, 1959, in Nagaur district of Rajasthan, but constitutional recognition implemented it across the country. It operates on 29 subjects listed in the 11th Schedule (such as agriculture, irrigation, health, education, etc.). In India, the rural local self-governance and development system is called Panchayati Raj (panchayati raj in Hindi). It was established in all states of India through state legislative acts to promote democracy at the grassroots level.
In India, the rural local self-governance and development system is called Panchayati Raj (panchayati raj in Hindi). It was established in all states of India through state legislative acts to promote democracy at the grassroots level. It was incorporated into the Constitution through the 73rd Constitutional Amendment Act, 1992.
Panchayati Raj is a system of local self-governance in rural India. It includes Panchayati Raj Institutions (PRIs) that govern villages and implement government schemes. This system is defined in Part IX of the Indian Constitution and operates at various levels. It includes Gram Panchayats at the village level, Panchayat Samitis at the block level, and Zila Parishads at the district level. The objective of Panchayati Raj is to promote economic development, social justice, and democracy at the grassroots level.
Evolution of Panchayati Raj in India -
- References to organized systems of rural local self-governance institutions are found in Vedic literature. Weaving together various references to coherently explain how rural local bodies function is challenging.
- In Vedic states, which were rural states, the village functioned as the primary administrative unit.
- Gramini was the name of a prominent village official. He was a respected officer who played an important role in the king's coronation ceremony.
- Direct references to village institutions are very scarce in major epics like the Ramayana and Mahabharata.
- The Chola era is the best example of local self-governance.
- During the Muslim period, some new concepts arrived on Indian soil. The new rulers adopted new practices and beliefs.
- The Muqaddam handled village administration, the Patwari managed revenue collection, and the Chaudhary, with the help of the panch, handled dispute resolution.
- There were significant differences in taxation and land management.
- Administration was controlled at the district level. Village communities persisted.
- These settlements had sufficient rights to self-governance within their boundaries.
- British rule weakened the long-term economic self-reliance of village communities and caused serious damage to the sense of community.
- Production for village consumption was replaced by production for the market. The prominence of village artisans and craftsmen ended. They were forced to leave their villages in search of better-paying jobs.
- As a result, Gram Panchayats lost their independence and mutual connections between settlements.
- The British adopted certain administrative practices that accelerated the destruction of rural communities.
- In fact, all these are characteristics of communities that fell into dire straits as a result of British amendments in the administrative structure.
- The decline of the long-prevalent Panchayati Raj in Indian villages can be attributed to centralization.
Post-Independence Era -
- The Panchayati Raj system (panchayati raj vyavastha) adopted its current form for the first time after independence in 1959. The Indian National Congress considered panchayats as a people-owned system. Local self-governance was considered essential as the true voice of democracy.
- Mahatma Gandhi specifically stated that the beginning of freedom should be from the grassroots level. Every village should be a republic (Gram Swaraj), with a panchayat having full authority.
Objectives:
- Promoting Grassroots Democracy: Providing local people the right to directly participate in governance and decision-making.
- Empowering Rural Communities: Empowering villagers to resolve their problems and needs.
- Democratic Decentralization: Distributing power and resources from the center to the local level, thereby increasing people's participation.
- Socio-Economic Progress: Promoting rapid social and economic development in rural areas.
- Providing Justice: Ensuring fair justice and availability of services at the local level.
Gandhi's Concept of Gram Swaraj -
- Mahatma Gandhi believed that "India lives in its villages" and true Swaraj could only come when every village becomes a republic. According to him:
- Each Gram Panchayat should have full authority.
- Only through Gram Swaraj can a real and powerful democracy be established.
- Decentralization of power should occur from the rural level to the national level.
Broader Impact and Significance -
- Democratic Empowerment: Panchayati Raj has promoted democratic participation in rural India. Particularly, women's leadership capacity has developed.
- Social Justice: There has been a remarkable increase in the political participation of weaker sections, especially women, Dalits, and tribals.
- Public Participation in Development: Local communities now play a direct role in planning and implementing their development.
- Administrative Efficiency: There has been faster identification and resolution of problems at the grassroots level, leading to increased administrative efficiency.
- The Panchayati Raj system has played an important role in strengthening Indian democracy, accelerating rural development, and promoting social justice. It is an important step towards realizing Mahatma Gandhi's dream of Gram Swaraj.
Key Features of Panchayati Raj
Constitutional Basis -
Part IX: Provisions from Articles 243 to 243(O) were added to the Constitution. 11th Schedule: 29 subjects were included in the jurisdiction of panchayats.
For example - Agriculture and agricultural extension, land development and land reforms, minor irrigation and water management, animal husbandry and dairy, etc.
Three-Tier Structure -
- Village Level: Gram Panchayat - Formed through direct elections
- Intermediate Level: Panchayat Samiti/Mandal Panchayat - For states with more than 20 lakh population
- District Level: Zila Panchayat - Mandatory in all states
Role of Gram Sabha - The Gram Sabha is considered the foundational unit of the democratic system. It includes all registered voters in the panchayat area.
Electoral System -
- Direct Elections: Members at all levels are elected directly
- Indirect Elections: Chairpersons at intermediate and district levels are elected from among elected members
- State Election Commission: Elections conducted by an independent election commission
Reservation Provisions -
- Scheduled Castes/Tribes: Reservations proportional to population
- Women's Reservation: At least one-third of total seats reserved for women
- Reservation for Chairperson Positions: Reservations in chairperson positions at all levels
- Tenure - The tenure of each panchayat is fixed at 5 years. If any panchayat is dissolved, it is mandatory to hold new elections within 6 months.
Financial Powers -
- Right to Levy Taxes: State governments can grant panchayats the right to levy appropriate taxes
- State Finance Commission: For reviewing the financial status of panchayats every 5 years
- Grants: Right to receive grants from the state's consolidated fund
- Judicial Protection - Restriction on court interference in election matters; elections can only be challenged before specified authorities.
Other Important Information -
- Constitutional Provisions of the 73rd Amendment Act
- Long before the Act was implemented in 1992, Gram Panchayats were already in practice in India, but this system had many flaws that prevented it from functioning as a people's government or responding to their demands. There were several reasons, including lack of funding, absence of regular elections, and low representation of weaker groups like women and Scheduled Castes and Tribes.
- Article 40 of the Directive Principles of State Policy in the Indian Constitution provides that the government should establish Gram Panchayats for itself and facilitate their effective functioning. To address these problems and strengthen local self-governance, the Government of India introduced the 73rd Amendment Act in 1992. Both houses approved the law, and it came into effect on April 24, 1993. Panchayats are a new chapter added to the Constitution as a result of this Act.
Importance of the 73rd Constitutional Amendment Act -
- Through this Act, the Eleventh Schedule was added to the Constitution, including 29 functional subjects for panchayats, along with Part IX, "Panchayats".
- Part IX of the Constitution includes Articles 243 to 243O.
- The Amendment Act gives expression to Article 40 of the Constitution (Directive Principles of State Policy), which calls upon the state to establish Gram Panchayats and grant them autonomy so that they can function as self-governing units.
- With the passage of the Act, the Panchayati Raj system will now be governed by constitutional provisions, and every state will have to implement it. Additionally, elections for Panchayati Raj Institutions can be held irrespective of state government priorities.
- The Act is divided into two parts: optional and mandatory. Mandatory provisions must be incorporated into state laws through amendments, including the establishment of a new Panchayati Raj framework. On the other hand, the state government has discretion over voluntary provisions.
- As a result of the Act, representative democracy has been replaced by participatory democracy.
PESA Act 1996
- The PESA Act 1996, the Panchayats (Extension to Scheduled Areas) Act, 1996, is a law that extends the provisions of Panchayati Raj in India to Scheduled Areas.
- Scheduled Areas are those regions where tribal communities primarily reside. The PESA Act empowers these tribal communities.
- It provides them autonomy in governance and decision-making. It recognizes the traditional customs and social practices of tribal communities. It allows them to manage their resources, protect their culture, and promote their socio-economic development.
- The Act emphasizes the participation of tribal communities in planning, implementation, and monitoring of development programs in their areas.
- Its objective is to protect the rights and interests of tribal communities and ensure their self-governance.
Important Committees Related to Panchayati Raj -
- The Government of India has formed various committees from time to time for the development, structure, and empowerment of the Panchayati Raj system. These committees have played an important role in strengthening rural local self-governance, promoting decentralization, and granting constitutional status to panchayats. The following are the major committees, described in chronological order:
- Balwant Rai Mehta Committee (1957): The first national-level committee, which made Panchayati Raj the basis of democratic decentralization. Major recommendations: Three-tier structure (Gram Panchayat, Panchayat Samiti, Zila Parishad), formation of Gram Sabha, responsibility of panchayats for development works, and regular elections. Its recommendations led to the launch of the first Panchayati Raj system in Rajasthan in 1959.
- Ashok Mehta Committee (1977): Formed to evaluate the weaknesses of Panchayati Raj. Major recommendations: Two-tier structure (Zila Parishad and Mandal Panchayat), participation of political parties, right of panchayats to levy taxes, empowering Gram Sabha, and executive role at the district level. This committee emphasized greater political autonomy for panchayats.
- G.V.K. Rao Committee (1985): Formed by the Planning Commission to review administrative arrangements. Major recommendations: Making the district level the center of development planning, ensuring regular elections, providing financial autonomy to panchayats, and increasing administrative efficiency. It presented the concept of 'District Gram Swaraj'.
- L.M. Singhvi Committee (1986): Focused on granting constitutional status to Panchayati Raj Institutions. Major recommendations: Constitutional recognition for panchayats, formation of State Panchayat Commission, legislative powers to Gram Sabha, establishment of Nyaya Panchayats, and training programs. Its recommendations laid the foundation for the 73rd Constitutional Amendment (1992).
Other Notable Committees -
- Gadgil Committee (1959): Recommendations on financial resources for Panchayati Raj.
- Sarkaria Commission (1988): Discussion on the role of panchayats in the context of center-state relations.
- P.K. Thungan Committee (1989): On municipalities and Panchayati Raj.
- These committees proved to be milestones in developing Panchayati Raj from ancient Gram Swaraj to a modern democratic institution, making decentralization of power possible in rural India.
3(a) ans.-
‘तकनीकी स्तर’ का अर्थ:-तकनीकी स्तर से तात्पर्य उस देश या क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के विकास स्तर से है। इसमें उपलब्ध तकनीकी साधन, नवाचार और उपकरण शामिल होते हैं। उदाहरण के लिए, उन्नत देशों में संचार उपकरण, अंतरिक्ष एवं नाभिकीय प्रौद्योगिकियाँ, एवं उच्च स्तरीय चिकित्सा उपकरण पाए जाते हैं, जो उनके उच्च तकनीकी स्तर को इंगित करते हैं। इसी प्रकार, किसी क्षेत्र के तकनीकी स्तर को देखकर उसके समग्र विकास स्तर का आकलन होता है।
मुख्य तत्व:
- उत्पादन तकनीक: श्रम-प्रधान या पूंजी-प्रधान विधियों का चुनाव
- नवाचार क्षमता: नई तकनीकों का विकास और अनुकूलन
- तकनीकी दक्षता: न्यूनतम इनपुट से अधिकतम आउटपुट प्राप्त करना
- डिजिटल परिपक्वता: AI, IoT और स्वचालन का एकीकरण
तकनीकी प्रगति एवं विकास :-
इतिहास में तकनीकी प्रगति औद्योगिक क्रांतियों के साथ बदलती रही है। 18वीं–19वीं शताब्दी में फैक्ट्रियों में मशीनों के आने से कताई-उद्योग के लुडाइट्स ने इनके विरोध में मशीनें नष्ट कीं, क्योंकि इससे उनकी नौकरियाँ खतरे में थीं। हाल के युग में चौथी औद्योगिक क्रांति के अंतर्गत कृत्रिम बुद्धिमत्ता, उन्नत रोबोटिक्स, ऑटोमेशन और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी तकनीकें उद्योगों और समाज को पुनर्परिभाषित कर रही हैं। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT) ने डिजिटल युग की नींव रखी है। उदाहरण के तौर पर, कोविड-19 महामारी के दौरान भारत में ऑनलाइन शिक्षा, ई-न्याय व्यवस्था, टेलीमेडिसिन और अन्य सरकारी सेवाएं सूचना-प्रौद्योगिकी आधारित माध्यमों से बिना अवरोध जारी रहीं।
तकनीकी विकास के सकारात्मक पक्ष:-
तकनीकी विकास ने उत्पादकता एवं नवाचार को बढ़ावा दिया है। वैश्विक दृष्टि से देखा जाए तो शोधों के अनुसार प्रौद्योगिकी सुधारों ने अर्थव्यवस्था में भारी वृद्धि की है – एक McKinsey रिपोर्ट के अनुसार केवल कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) ही 2030 तक वैश्विक GDP में 13 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान कर सकती है। तकनीकी नवाचारों ने स्वास्थ्य, कृषि और शिक्षा जैसी बुनियादी जरूरतों में भी सुधार किया है। उदाहरण के लिए, चिकित्सा तकनीकों ने बाल मृत्यु दर घटाई और जीवन प्रत्याशा बढ़ाई है; उन्नत कृषि तकनीकों ने फसल उत्पादन बढ़ाकर भूखमरी को कम किया है। साथ ही, बिजली, साफ़ पानी और इंटरनेट जैसी सुविधाओं की पहुँच ने अरबों लोगों के जीवन स्तर में सुधार किया है।
सेवा क्षेत्र में भी विकास हुआ है – डिजिटल स्वास्थ्य कार्यक्रमों ने ग्रामीण-शहरी असमानता घटाई है। भारत की आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन जैसी पहल ने दूरदराज क्षेत्रों में टेलीमेडिसिन और ईएचआर की सुविधा दी है। महामारी में ऑनलाइन शिक्षा और इंटरनेट आधारित सामाजिक संपर्क ने लोगों को जुड़े रहने में मदद की। विश्व आर्थिक मंच (WEF) की रिपोर्ट अनुमान है कि AI और ऑटोमेशन से 2025 तक 97 मिलियन नए रोजगार सृजित हो सकते हैं, जो विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को फायदा पहुँचा सकते हैं। कुल मिलाकर, तकनीकी विकास से उद्योगों की दक्षता बढ़ी, नवाचार को प्रोत्साहन मिला और सेवाओं का व्यापकरण हुआ है।
उत्पादकता और आर्थिक वृद्धि: प्रौद्योगिकी से उत्पादन लागत कम होती है और आउटपुट बढ़ता है। विश्व आर्थिक मंच (WEF) की 2025 रिपोर्ट के अनुसार, AI और सूचना प्रसंस्करण जैसी तकनीकें 86% क्षेत्रों में उत्पादकता बढ़ाएंगी, जबकि रोबोटिक्स और ऑटोमेशन 58% में योगदान देंगे। इससे वैश्विक GDP में वृद्धि होगी, जैसे कि AI से 2030 तक 15.7 ट्रिलियन डॉलर का योगदान अनुमानित है।
- नई नौकरियों का सृजन: तकनीक न केवल पुरानी नौकरियां समाप्त करती है, बल्कि नई विकसित करती है। अमेरिकी श्रम सांख्यिकी ब्यूरो (BLS) के अनुसार, 2023-2033 के बीच सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की नौकरियां 17.9% बढ़ेंगी, जो औसत से कहीं अधिक है। PwC की 2025 AI जॉब्स बारोमीटर रिपोर्ट बताती है कि AI से उच्च ऑटोमेशन वाले क्षेत्रों में भी कर्मचारियों की मूल्यवत्ता बढ़ती है, न कि घटती। उदाहरण के लिए, 2028 तक AI से 69 मिलियन नई नौकरियां सृजित होंगी।
- सामाजिक-आर्थिक लाभ: तकनीक बेहतर कार्य स्थितियां प्रदान करती है, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण क्षेत्रों में। विकासशील देशों में, यह कृषि और विनिर्माण को आधुनिक बनाकर गरीबी कम करती है।
तकनीकी विकास के नकारात्मक पक्ष:-
हालाँकि, तकनीकी विकास के साथ ही मशीनीकरण से पारंपरिक श्रम संकट में पड़ा है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के अध्ययन के अनुसार कई नई तकनीकें मानव श्रम को प्रतिस्थापित कर रही हैं, पर उत्पादकता में अपेक्षित वृद्धि नहीं ला रही हैं। भारत में युवाओं में बेरोज़गारी की समस्या पहले से है, और शोध दिखाते हैं कि रोबोटिक व स्वचालन तकनीकों के चलते निम्न-कुशल श्रमिक नौकरियाँ कम हुई हैं। उदाहरणतः एक सेमिनार में तकनीकी शिक्षा विशेषज्ञों ने मशीनीकरण को बढ़ती बेरोज़गारी का प्रमुख कारण बताया था। इन सब से स्पष्ट होता है कि अल्पकाल में मशीनीकरण से कुछ क्षेत्रों में नौकरियाँ घटने का जोखिम रहता है।
- वर्तमान प्रभाव: AI से उच्च जोखिम वाले व्यवसायों में बेरोजगारी दर 2022-2025 के बीच बढ़ी है। सेंट लुइस फेड की 2025 रिपोर्ट के अनुसार, AI एक्सपोजर वाले क्षेत्रों में बेरोजगारी 0.5% अधिक बढ़ी। गोल्डमैन सैक्स अनुमानित करता है कि AI ट्रांजिशन में बेरोजगारी आधी प्रतिशत बढ़ेगी। विनिर्माण में 2030 तक 20 मिलियन नौकरियां रोबोट्स से खो सकती हैं।
- क्षेत्रीय असर: ड्राइवर, रिटेल वर्कर्स और स्वास्थ्य कर्मचारियों जैसे क्षेत्र प्रभावित हो रहे हैं। ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट बताती है कि नई ऑटोमेशन से लाखों नौकरियां विलुप्त हो सकती हैं। हालांकि, कुछ अध्ययन (जैसे साइंसडायरेक्ट) दिखाते हैं कि रोबोट्स से बेरोजगारी कम भी हो सकती है (1% रोबोट वृद्धि से 0.037% बेरोजगारी कमी), लेकिन यह अल्पकालिक है।
- भविष्य के रुझान: मैकिंसे की 2017 (अपडेटेड) रिपोर्ट के अनुसार, 2030 तक ऑटोमेशन से 85 मिलियन नौकरियां कम होंगी, लेकिन 97 मिलियन नई सृजित होंगी। ILO की 2024 रिपोर्ट में जेनरेटिव AI से 2.3% रोजगार (75 मिलियन नौकरियां) जोखिम में हैं। उच्च आय वाले देशों में यह अधिक प्रभावी होगा, जबकि विकासशील देशों में कौशल अंतर से समस्या बढ़ेगी। इतिहास (औद्योगिक क्रांति) दिखाता है कि अल्पकालिक बेरोजगारी बढ़ती है, लेकिन दीर्घकालिक में नेट जॉब क्रिएशन होता है।
विकासशील देशों पर सामाजिक–आर्थिक प्रभाव :-
विकासशील देशों में तकनीकी विकास का प्रभाव जटिल है। एक ओर यह आर्थिक विकास और सेवाओं में सुधार को बढ़ावा देता है, तो दूसरी ओर ‘डिजिटल विभाजन’ जैसी चुनौतियाँ सामने आती हैं। वैश्विक रिपोर्टों के अनुसार कई विकासशील क्षेत्रों में इंटरनेट व स्मार्टफोन की पहुँच सीमित है, जिससे उनकी बड़ी आबादी तकनीकी लाभों से वंचित रहती है। भारत में भी सरकार मानती है कि देश का बड़ा तबका अभी भी डिजिटल उपकरणों से जुड़ नहीं पाया है। डिजिटल स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी पहलें इन असमानताओं को कम करने में सहायक हैं। उदाहरणार्थ, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ने स्वास्थ्य सेवाओं को ग्रामीण-शहरी दोनों क्षेत्रों में डिजिटल माध्यम से उपलब्ध कराया है। इस तरह, तकनीकी प्रगति विकास की कड़ी को मज़बूत करती है, पर साथ ही सुनिश्चित करना होता है कि इसके लाभ सभी तक पहुँचे।
अतः तकनीकी स्तर में बढ़ोत्तरी समग्र विकास के लिए लाभदायक सिद्ध होती है, लेकिन इसके साथ दीर्घकालिक सामाजिक चुनौतियाँ भी आती हैं। संतुलित दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है। विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि तकनीकी परिवर्तन के साथ श्रमिकों का पुनः कौशल विकास, ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटलीकरण के प्रयास और उद्योगों को कर्मचारियों के पुन:नियोजन के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए। इसी से तकनीकी प्रगति के दुष्प्रभाव कम होंगे और विकास निरंतर एवं समावेशी रहेगा।
अन्य महत्वपूर्ण तथ्य –
भविष्य की रणनीति के लिए आवश्यक कार्य –
कौशल विकास:-
AI, प्रोग्रामिंग, डेटा एनालिटिक्स में प्रशिक्षण
निरंतर शिक्षा और रीस्किलिंग कार्यक्रम
नीतिगत सुधार:-
श्रम सब्सिडी पर जोर (पूंजी सब्सिडी के बजाय)
लचीली सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था
तकनीकी समावेशन को बढ़ावा
डिजिटल विभाजन को पाटना:-
ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट पहुंच
डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम
किफायती तकनीकी उपकरण
सकारात्मक संकेत:-
रोजगार दर में सुधार (बेरोजगारी 6% से घटकर 3.2%)
नई तकनीकी नौकरियों का सृजन
युवा बेरोजगारी में कमी (17.8% से 10.2%)
आगे की चुनौतियां:-
पारंपरिक नौकरियों का नुकसान
कौशल अंतर की समस्या
डिजिटल विभाजन
Meaning of ‘Technical Level’:
Technical level refers to the level of technological development in a country or region. It includes available technological resources, innovations, and tools. For example, advanced countries have communication equipment, space and nuclear technologies, and high-level medical devices, which indicate their high technical level. Similarly, the technical level of a region allows for an assessment of its overall development level.
Main Elements:
- Production Technology: Choice between labor-intensive or capital-intensive methods
- Innovation Capacity: Development and adaptation of new technologies
- Technical Efficiency: Achieving maximum output with minimum input
- Digital Maturity: Integration of AI, IoT, and automation
Technological Progress and Development:
Throughout history, technological progress has evolved with industrial revolutions. In the 18th–19th centuries, the introduction of machines in factories led the Luddites in the weaving industry to destroy machines in protest, as it threatened their jobs. In recent times, under the Fourth Industrial Revolution, technologies like artificial intelligence, advanced robotics, automation, and the Internet of Things are redefining industries and society. Information and Communication Technology (ICT) has laid the foundation for the digital age. For instance, during the COVID-19 pandemic, online education, e-courts, telemedicine, and other government services in India continued uninterrupted through ICT-based mediums.
Positive Aspects of Technological Development:
Technological development has boosted productivity and innovation. From a global perspective, studies show that technological improvements have led to massive economic growth—a McKinsey report states that artificial intelligence (AI) alone could contribute $13 trillion to global GDP by 2030. Technological innovations have also improved basic needs like health, agriculture, and education. For example, medical technologies have reduced infant mortality and increased life expectancy; advanced agricultural techniques have increased crop yields and reduced famine. Additionally, access to electricity, clean water, and the internet has improved the living standards of billions.
In the service sector too, development has occurred—digital health programs have reduced rural-urban disparities. Initiatives like India’s Ayushman Bharat Digital Mission have provided telemedicine and Electronic Health Records (HER) in remote areas. During the pandemic, online education and internet-based social connections helped people stay connected. The World Economic Forum (WEF) report estimates that AI and automation could create 97 million new jobs by 2025, benefiting developing economies. Overall, technological development has increased industrial efficiency, encouraged innovation, and expanded services.
- Productivity and Economic Growth: Technology reduces production costs and increases output. According to the World Economic Forum (WEF) 2025 report, technologies like AI and information processing will boost productivity in 86% of sectors, while robotics and automation will contribute in 58%. This will lead to global GDP growth, such as an estimated $15.7 trillion contribution from AI by 2030.
- Creation of New Jobs: Technology not only eliminates old jobs but also creates new ones. According to the U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS), software developer jobs will grow by 17.9% between 2023-2033, far above average. PwC’s 2025 AI Jobs Barometer report indicates that even in highly automated sectors, employee value increases rather than decreases due to AI. For example, AI will create 69 million new jobs by 2028.
- Socio-Economic Benefits:Technology provides better working conditions, such as in health, education, and environmental sectors. In developing countries, it modernizes agriculture and manufacturing, reducing poverty.
Negative Aspects of Technological Development:
However, alongside technological development, mechanization has put traditional labor in crisis. According to studies by the International Labour Organization (ILO), many new technologies are replacing human labor but not bringing the expected increase in productivity. In India, youth unemployment is already a problem, and research shows that robotics and automation technologies have reduced low-skilled labor jobs. For instance, in a seminar, technical education experts identified mechanization as a major cause of rising unemployment. All this clearly indicates that in the short term, mechanization poses a risk of job losses in certain sectors.
- Current Impact:Unemployment rates have risen in high-risk occupations due to AI between 2022-2025. According to the St. Louis Fed’s 2025 report, unemployment increased by 0.5% more in AI-exposed sectors. Goldman Sachs estimates that the AI transition will increase unemployment by half a percent. In manufacturing, 20 million jobs could be lost to robots by 2030.
- Regional Impact: Sectors like drivers, retail workers, and health staff are being affected. The Brookings Institution report states that new automation could eliminate millions of jobs. However, some studies (like ScienceDirect) show that robots could reduce unemployment (1% robot growth leads to 0.037% unemployment decrease), but this is short-term.
- Future Trends:McKinsey’s 2017 (updated) report estimates that automation will eliminate 85 million jobs by 2030, but create 97 million new ones. The ILO’s 2024 report indicates that generative AI puts 2.3% of employment (75 million jobs) at risk. This will be more pronounced in high-income countries, while in developing countries, the skills gap will exacerbate the problem. History (Industrial Revolution) shows short-term unemployment rises, but long-term net job creation occurs.
Socio-Economic Impact on Developing Countries:
The impact of technological development in developing countries is complex. On one hand, it promotes economic growth and service improvements; on the other, challenges like the ‘digital divide’ emerge. According to global reports, internet and smartphone access is limited in many developing regions, leaving large populations deprived of technological benefits. In India too, the government acknowledges that a significant section of the population is still not connected to digital devices. Initiatives like digital health and education are helping reduce these inequalities. For example, the Ayushman Bharat Digital Mission has made health services available digitally in both rural and urban areas. Thus, technological progress strengthens the chain of development, but it must be ensured that its benefits reach everyone.
Therefore, an increase in technical level proves beneficial for overall development, but it also brings long-term social challenges. A balanced approach is essential. Experts advise reskilling workers alongside technological change, efforts to digitize rural areas, and incentives for industries to re-employ employees. This will mitigate the adverse effects of technological progress and ensure development remains continuous and inclusive.
Other Important Facts -
Necessary Actions for Future Strategy -
Skill Development:
- Training in AI, programming, data analytics
- Continuous education and reskilling programs
Policy Reforms:
- Emphasis on labor subsidies (instead of capital subsidies)
- Flexible social security system
- Promoting technological inclusion
*Bridging the Digital Divide:**
- Internet access in rural areas
- Digital literacy programs
- Affordable technological devices
Positive Signs:
- Improvement in employment rate (unemployment down from 6% to 3.2%)
- Creation of new technological jobs
- Reduction in youth unemployment (from 17.8% to 10.2%)
Future Challenges:
- Loss of traditional jobs
- Skills gap problem
- Digital divide
2. (b) ans.-
प्रवृत्ति का विश्लेषण: पिछले दशक से भारतीय सिनेमा (बॉलीवुड और क्षेत्रीय) में हिंसा और यौन सामग्री का चित्रण स्पष्ट रूप से बढ़ा है। कुछ विश्लेषकों ने पाया है कि नेट मूवीज में सेक्स सीन अब 40% कम हो गए हैं, जबकि हिंसा और नशीली वस्तुओं के दृश्य बढ़े हैं। दक्षिण भारत की पैन-इंडिया फिल्मों जैसे KGF, RRR, पुष्पा ने भारी बजट की हिंसात्मक एक्शन से दर्शक वर्ग में धूम मचाई है। इन फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर साबित किया कि भारतीय दर्शकों में ‘एक्शन/हिंसा’ की मांग बढ़ी है। मुंबई और उपनगरीय सिनेमा में भी “एनिमल”, “किल”, “सेक्टर 36”, “युध्द” जैसी फिल्मों में अत्यधिक वीभत्स हिंसा दिख रही है। साथ ही कुछ नेटफ्लिक्स/ओटीटी श्रृंखलाओं में यौन चित्रण पहले की अपेक्षा आम होने लगा है (उदाहरणतः Sacred Games में नग्न दृश्य)। इन प्रवृत्तियों का कारण निर्देशक और निर्माता बताते हैं कि दर्शक इनका स्वीकार कर रहे हैं, और बड़े बजट वाले प्रोजेक्ट्स में यथार्थवाद व तेज रफ्तार कहानी-निर्माण के लिए हिंसा-नग्नता आवश्यक हो गए हैं। जैसा कि विद्वान बताते हैं, आज एक्शन के दौर में निर्माता उसी के पीछे भाग रहे हैं जो हिट हो।
पक्ष में तर्क
यथार्थवाद और कथा-प्रभाव: कई फिल्मकारों का कहना है कि हिंसा और नग्नता कथा को यथार्थतः देता है। (पी.डब्ल्यू.आई.ए.एस. के विश्लेषण के अनुसार) “फिल्मकारों का तर्क है कि हिंसा एक वैध कलात्मक उपकरण है, जो यथार्थवाद और कथा-वाचन के लिए आवश्यक है, और इसे सीमित करना रचनात्मकता को दबाता है”। सुधीर मिश्रा जैसे निर्देशकों ने भी कहा है, जब तक फ़िल्में असंवैधानिक हिंसा या नफरत नहीं फैला रही हैं, तब तक सभी विषयों को स्वतंत्र रूप से दिखाना चाहिए। उदाहरण के लिए, आमिर खान ने फ़िल्म PK में एलियन किरदार को वास्तविक बनाने के लिए सम्पूर्ण रूप से नग्न होने का साहसिक निर्णय लिया। राजकुमार राव जैसे अभिनेताओं ने भी कच्चे यथार्थ दिखाने के विश्वास पर “लव सेक्स और धोखा” जैसी फिल्मों में बिंदास नग्नता के दृश्यों को स्वीकार किया। रंजित देसपांडे ने “Sacred Games” में अपने नग्न दृश्य इसलिए किए क्योंकि कहानी की मांग थी, और वह निर्देशक पर भरोसा करके बिना हिचकिचाहट ‘हाँ’ कह गईं।
कलात्मक स्वतंत्रता एवं वैश्विक प्रतिस्पर्धा: आधुनिक भारतीय सिनेमा ग्लोबल मार्केट में बोल रहा है। “पैन-इंडिया” फिल्मों ने यह दिखाया कि हिन्सा-आधारित एक्शन बड़े बजट, डबिंग और व्यापक प्रचार के जरिये अंतरराष्ट्रीय दर्शकों को भी आकर्षित करता है। क्षेत्रीय फिल्में (साउथ सिनेमा) सिर्फ लोकल ही नहीं, विदेशों में भी ऊँचे कलेक्शन कर रहीं हैं। निर्माताओं का तर्क है कि वैश्विक मंच पर कदम रखने के लिए उन्हें बारीक बयानों और विजुअल्स के साथ प्रयोग करना पड़ता है; नग्नता और हिंसा को यथासंभव रचनात्मक रूप देना चाहिए। इसके अलावा, यौन स्वतंत्रता विषय (जैसे महिला स्वतंत्रता, सेक्सुअलिटी) पर फिल्में बनना भी नए सामाजिक विमर्श में योगदान है।
विकसित हो रहे दर्शकों की अभिरुचि: डिजिटल प्लेटफार्मों के कारण अब भारतीय दर्शक भी विविध सामग्री देखने लगे हैं। ‘स्थानीय-छत्र’ फिल्में और वेब-सीरीज दर्शकों को नया कंटेंट दे रही हैं, जिस कारण मेनस्ट्रीम भी इसी तरह के “ग्रे सूट” (या एडल्ट) विषयों की ओर आकर्षित हो रहा है। कई ओटीटी और इंडी फिल्मकारों ने पाया है कि कंप्टीशन बढ़ने पर फिल्में प्रामाणिक अनुभव देने की कोशिश कर रही हैं। इस दृष्टि से, यौन चित्रण और हिंसा एक हद तक दर्शकों को हॉलीवुड जैसी मुक्त अभिव्यक्ति का स्वाद देते हैं, जिससे भारतीय सिनेमा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगी बना रहता है।
विपक्ष में तर्क
विरोधी दावा करते हैं कि अनावश्यक हिंसा और नग्नता दर्शकों को असंवेदनशील बनाती है, रूढ़ियों को बनाए रखती है और सामाजिक हानियों को बढ़ाती है, जो पदार्थ के बजाय झटके मूल्य को प्राथमिकता देती है।
युवाओं और समाज पर प्रतिकूल प्रभाव: भारतीय सिनेमा की विशाल पहुंच—1.5 अरब से अधिक दर्शक—इसके प्रभाव को बढ़ाती है, विशेष रूप से प्रभावशाली युवाओं पर। अध्ययनों से पता चलता है कि हिंसक दृश्यों के बार-बार संपर्क आक्रामक व्यवहार से जुड़े होते हैं, क्योंकि बच्चे संदर्भ को समझे बिना ऑन-स्क्रीन क्रूरता की नकल करते हैं। 2020 के ऑक्सफैम रिपोर्ट में हाइलाइट किया गया है कि सिनेमाई उत्पीड़न की महिमामंडनी महिलाओं के खिलाफ अपराधों में वृद्धि से जुड़ी हुई है, जिसमें 2016 में बलात्कारों में 12% की वृद्धि का आंशिक श्रेय सामान्यीकृत पितृसत्तात्मक रूढ़ियों को दिया गया है। इसी प्रकार, कबीर सिंह जैसी फिल्मों में स्पष्ट कामुकता विषाक्तता को रोमांटिक बनाती है, कथा और वास्तविक जीवन की हकदारी के बीच की रेखाओं को धुंधला करती है। किशोरों (17-21 वर्ष की आयु) के लिए, वेब सीरीज़ की अनफ़िल्टर्ड सामग्री संबंधों के विकृत दृष्टिकोणों के जोखिमों को बढ़ाती है, जो विचारपूर्ण चित्रणों में “सेक्स मंदी” में योगदान देती है जबकि अश्लीलता बढ़ रही है।
सांस्कृतिक क्षरण और सनसनीवाद: आलोचक लियो जैसी तमिल फिल्मों या बॉलीवुड की पठान में “बेवकूफीपूर्ण हिंसा” की ओर बदलाव की निंदा करते हैं, जहाँ खूनखराबा बिना कथानक वाले रोमांच के लिए सेवा करता है, जो संयम और सहानुभूति के सांस्कृतिक मूल्यों को क्षीण करता है। नग्नता अक्सर वस्तुकरण में बदल जाती है, सशक्तिकरण के बजाय पुरुष दृष्टि को मजबूत करती है, जैसा कि आइटम गानों में देखा जाता है जो महिलाओं को वस्तु बनाते हैं। यह न केवल संवेदनशीलताओं को आहत करता है बल्कि असामाजिक दृष्टिकोणों को ईंधन प्रदान करता है, जिसमें फिल्में महिलाओं के खिलाफ हिंसा (वीएडब्ल्यूजी) को पितृसत्तात्मक लेंस से वैध बनाती हैं।
नैतिक चिंताएँ: भारत जैसे विविध राष्ट्र में, अनियंत्रित सामग्री समुदायों को अलग-थलग करने, सांप्रदायिक तनाव भड़काने या आघात को तुच्छ बनाने का जोखिम उठाती है, जैसा कि सामान्य दर्शक फिल्मों में बलात्कार महिमामंडनी के खिलाफ प्रतिक्रिया में देखा गया है।
सेंसर बोर्ड की भूमिका: आलोचनाएँ, सुधार और चुनौतियाँ
भारतीय फिल्मों की समीक्षा मुख्यतः केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) करता है, जो 1952 की सिनेमैटोग्राफ अधिनियम के तहत काम करता है। बोर्ड का काम समाज के अनुरूप फ़िल्मों को प्रमाणित करना है, लेकिन इसके निर्णय अक्सर विवादों में घिरे रहते हैं। उदाहरण के लिए, अगस्त 2025 में आई हॉलीवुड फिल्म Superman से रोमांटिक चुंबन के दृश्यों को CBFC ने “अत्यधिक कामुक” कहकर कट कर दिया, जबकि उसके बाद ट्विटर पर लोगों ने सवाल उठाया कि बोर्ड हिंसक या बलात्कारी सीन को आसानी से मंजूरी दे देता है लेकिन एक सामान्य चुंबन को नहीं। इसी तरह, निर्देशक कंगना रनौत ने आरोप लगाया कि उनके ऐतिहासिक फिल्म Emergency पर सेंसरशिप लगाई जा रही है, जबकि “हिंसा और नग्नता” पर कोई रोक नहीं है।
- हाल के विवाद: कई बड़े प्रोजेक्ट्स को प्रमाणन के लिए कटौती या देरी झेलनी पड़ी है। Emergency को U/A मिलते हुए 13 कट्स करने पड़े थे, जिन्हें विभिन्न धार्मिक समूहों ने मांगा। जबकि Baby Girl जैसी फिल्म को ‘A’ (वयस्क) प्रमाणपत्र मिलने पर भी उसमें 3+ मिनट की अभद्र भाषा और अंतरंग दृश्यों की कटौती कर दी गई। कभी-कभी CBFC के फैसलों को राजनैतिक रंग भी दिया जाता है; उदाहरणतः Donald Trump: The Apprentice बायोपिक को निर्देशक की आपत्ति पर रोक दी गई थी। इस तरह की घटनाएँ लगातार खिंचाव दर्शाती हैं कि सेंसरशिप अब कानूनी-नैतिक विमर्श से बढ़कर सामाजिक-अभिभावकीय दबाव का विषय बन गई है।
- सुधार और चुनौतियाँ: मार्च 2024 में सिनेमैटोग्राफ (प्रमाणीकरण) नियम, 2024 लागू किए गए। इन नियमों के तहत प्रमाणन के लिए ऑनलाइन “ई-सिनेप्रमाण” पोर्टल बनाया गया है, और बोर्ड में सदस्य नियुक्ति में महिलाओं को कम से कम एक-तिहाई (आदर्श रूप से आधे) बनाए रखने का प्रावधान जोड़ा गया। ये कदम आधुनिककरण की दिशा में हैं। फिर भी बड़ी चुनौतियाँ बरकरार हैं: सेंसर बोर्ड की सीमाएँ अस्पष्ट हैं, और कई बार राजनीतिक-धार्मिक दबाव के चलते निर्णय असंगत होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बीobby Art Int. बनाम भारत संघ (1996) में कहा था कि किसी सामाजिक कुरीति को यथार्थ में दिखाना फ़िल्म की अंतर्निहित संदेश का हिस्सा है और केवल इसके आपत्तिजनक होने पर इसे नहीं हटाना चाहिए। इसी तरह K.A. Abbas बनाम यूनियन ऑफ़ इंडिया (1971) ने फिल्मों को कला माना और कहा कि सीमित पूर्व-सेंसरसिप को यथोचित होना चाहिए। तथापि, वर्तमान में सेंसर बोर्ड अक्सर इन सिद्धांतों के बीच जूझ रहा है कि कहाँ तक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो और कहाँ से “सामाजिक हित” की रक्षा की जाए।
आवश्यक सुधार और सुझाव
- CBFC में संरचनात्मक सुधार-
- श्याम बेनेगल समिति की सिफारिशें: CBFC की भूमिका केवल वर्गीकरण तक सीमित करना, काट-छांट की शक्ति कम करना
- स्पष्ट और निष्पक्ष दिशा-निर्देशों का निर्माण
- संतुलित दृष्टिकोण-
- कलात्मक स्वतंत्रता और सामाजिक जिम्मेदारी के बीच संतुलन
- सामुदायिक परामर्श और जन भागीदारी को बढ़ावा
- डिजिटल युग की चुनौतियों का समाधान-
- OTT प्लेटफॉर्म के लिए स्पष्ट नियम और age verification की मजबूत व्यवस्था
- अभिभावकों और शिक्षकों के लिए मीडिया साक्षरता कार्यक्रम
भारतीय सिनेमा में हिंसा और नग्नता के बढ़ते चित्रण ने एक द्वन्द्वपूर्ण बहस छेड़ दी है। इसे समर्थकों का कहना है कि यथार्थपरक और आधुनिक फिल्म-कथा के लिए फिल्मकारों को स्वतन्त्रता मिलनी चाहिए, ताकि भारत के दर्शकों को वैश्विक स्तर की विविध सामग्री मिले। वहीं विरोधियों की चिंता है कि पारिवारिक और सांस्कृतिक मूल्यों पर कुठाराघात न हो, तथा युवा मन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। सेंसर बोर्ड इन दोनों धाराओं के बीच संतुलन बनाने का प्रयास करता रहा है, पर नीतियाँ अक्सर विवादों में उलझी रहीं। व्यक्तिगत रूप से, ऐसा लगता है कि भारतीय फ़िल्मों को यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाने का हक़ है, लेकिन उसी समय एक जिम्मेदार रुख़ भी जरूरी है। मौजूदा कानूनी एवं तकनीकी सुधार—जैसे सर्टिफिकेशन के नवाचार नियम और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वयं-नियमन—ने थोड़ी राहत दी है, मगर अन्ततः निर्णय दर्शकों और समाज की सहिष्णुता पर निर्भर करेगा। भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के साथ तालमेल रखते हुए नई अभिव्यक्ति को ग्रहण करने तथा सुझाव के लिए खुले दिमाग से चर्चा जारी रहना आवश्यक है।
Analysis of the Trend: In the last decade, violence and sexual content in Indian cinema (Bollywood and regional) have clearly increased. Some analysts have found that sex scenes in Netflix movies have decreased by 40%, while depictions of violence and narcotics have risen. Pan-India films from South India like *KGF* *Pushpa* have created a sensation among audiences with high-budget violent action. These films have proven at the box office that there is growing demand for 'action/violence' among Indian viewers. In Mumbai and suburban cinema as well, films like *Animal*, *Kill*, *Sector 36*, and *Yuddha* are showing extreme grotesque violence. At the same time, sexual depictions have become more common than before in some Netflix/OTT series (e.g., nude scenes in Sacred Games). Directors and producers attribute these trends to the fact that audiences are accepting them, and in big-budget projects, violence and nudity have become essential for realism and fast-paced storytelling. As scholars point out, in today's action era, producers are chasing whatever hits.
Arguments in Favor
Realism and Narrative Impact: Many filmmakers argue that violence and nudity provide authenticity to the narrative. (According to P.W.I.A.S. analysis) "Filmmakers contend that violence is a valid artistic tool necessary for realism and storytelling, and restricting it suppresses creativity." Directors like Sudhir Mishra have also stated that as long as films do not promote unconstitutional violence or hatred, all subjects should be depicted freely. For example, Aamir Khan boldly decided to appear completely nude in the film PK to make the alien character realistic. Actors like Rajkummar Rao have also accepted uninhibited nudity scenes in films like Love, Sex aur Dhokha based on the belief in showing raw reality. Ranjeet Deshpande performed her nude scenes in Sacred Games because the story demanded it, and she trusted the director enough to say 'yes' without hesitation.
Artistic Freedom and Global Competition: Modern Indian cinema is speaking to the global market. "Pan-India" films have shown that violence-based action, with big budgets, dubbing, and wide promotion, attracts international audiences as well. Regional films (South cinema) are not only collecting high earnings locally but also abroad. Producers argue that to step onto the global stage, they must experiment with nuanced expressions and visuals; nudity and violence should be given as creative a form as possible. Additionally, making films on themes of sexual freedom (such as women's independence, sexuality) also contributes to new social discourse.
Evolving Audience Preferences: Due to digital platforms, Indian audiences have started watching diverse content. 'Local-global' films and web series are providing new content to viewers, which is drawing mainstream cinema toward similar "grey suit" (or adult) themes. Many OTT and indie filmmakers have found that as competition increases, films are trying to provide authentic experiences. From this perspective, sexual depictions and violence, to some extent, give Indian audiences a taste of the free expression seen in Hollywood, keeping Indian cinema competitive on the international stage.
Arguments Against
Opponents claim that unnecessary violence and nudity desensitize audiences, perpetuate stereotypes, and exacerbate social harms, prioritizing shock value over substance.
Adverse Impact on Youth and Society: The vast reach of Indian cinema—with over 1.5 billion viewers—amplifies its influence, especially on impressionable youth. Studies show that repeated exposure to violent scenes is linked to aggressive behavior, as children mimic on-screen brutality without understanding context. The 2020 Oxfam report highlights that the glorification of cinematic harassment is connected to rising crimes against women, with a partial attribution to a 12% increase in rapes in 2016 due to normalized patriarchal stereotypes. Similarly, films like *Kabir Singh* romanticize explicit toxicity, blurring lines between cinematic and real-life entitlement. For adolescents (ages 17-21), unfiltered web series content heightens risks of distorted views on relationships, contributing to a "sex recession" amid rising pornography, where thoughtful depictions are lacking.
Cultural Erosion and Sensationalism: - Critics condemn the shift toward "mindless violence" in films like the Tamil *Leo* or Bollywood's *Pathaan*, where bloodshed serves thrill without plot, eroding cultural values of restraint and empathy. Nudity often devolves into objectification, reinforcing the male gaze rather than empowerment, as seen in item songs that commodify women. This not only offends sensitivities but fuels antisocial attitudes, with films validating violence against women (VAWG) through a patriarchal lens.
Ethical Concerns: In a diverse nation like India, unchecked content risks alienating communities, inciting communal tensions, or trivializing trauma, as seen in backlash against mainstream films that glorify rape.
Role of the Censor Board: Criticisms, Reforms, and Challenges -
The review of Indian films is primarily done by the Central Board of Film Certification (CBFC), which operates under the Cinematograph Act, 1952. The Board's role is to certify films in accordance with societal norms, but its decisions often remain embroiled in controversies. For example, in August 2025, the Hollywood film *Superman* had its romantic kissing scenes cut by the CBFC, calling them "excessively sensual," while people on Twitter questioned why the Board easily approves violent or rape scenes but not a normal kiss. Similarly, director Kangana Ranaut alleged that censorship was being imposed on her historical film Emergency , while there is no restriction on "violence and nudity."
Recent Controversies: Many major projects have faced cuts or delays for certification.
Emergency had to make 13 cuts to receive a U/A rating, as demanded by various religious groups. While films like Baby Girl received an 'A' (adult) certificate, they still had cuts for 3+ minutes of abusive language and intimate scenes. Sometimes, CBFC decisions are given a political color; for instance, the biopic *Donald Trump: The Apprentice* was halted due to the director's objection. Such incidents consistently show that censorship has become more a matter of social-parental pressure than legal-ethical discourse.
Reforms and Challenges: In March 2024, the Cinematograph (Certification) Rules, 2024 were implemented. Under these rules, an online "e-Cinepraman" portal has been created for certification, and provisions have been added to maintain at least one-third (ideally half) women in Board appointments. These steps are in the direction of modernization. However, major challenges persist: The CBFC's limitations are unclear, and decisions are often inconsistent due to political-religious pressures. The Supreme Court in *Bobby Art International v. Union of India* (1996) stated that depicting a social evil realistically is part of the film's inherent message and should not be removed merely for being objectionable. Similarly, in *K.A. Abbas v. Union of India* (1971), films were considered art, and limited pre-censorship was deemed reasonable. Nevertheless, currently, the Censor Board is grappling between the principles of freedom of expression and protecting "public interest."
Necessary Reforms and Suggestions
1.Structural Reforms in CBFC-
- Shyam Benegal Committee Recommendations: Limit CBFC's role to classification only, reduce power to cut
- Develop clear and impartial guidelines
2. Balanced Approach-
- Balance between artistic freedom and social responsibility
- Promote community consultation and public participation
3. Addressing Challenges of the Digital Age -
- Clear rules for OTT platforms and strong age verification systems
- Media literacy programs for parents and teachers
The increasing depiction of violence and nudity in Indian cinema has sparked a contentious debate. Supporters argue that filmmakers should have the freedom to adopt realistic and modern film narratives, so that Indian audiences get diverse content on a global scale. On the other hand, opponents' concerns are that there should be no assault on family and cultural values, and adverse effects on young minds. The Censor Board has been trying to strike a balance between these two streams, but policies have often remained entangled in controversies. Personally, it seems that Indian films have the right to adopt a realistic approach, but at the same time, a responsible stance is necessary. Existing legal and technical reforms—such as innovative certification rules and self-regulation on digital platforms—have provided some relief, but ultimately, the decision will depend on the tolerance of audiences and society. It is essential to continue discussions with an open mind to embrace new expressions while aligning with India's rich cultural heritage and suggestions.
|