BPSC PYQ Mains Answer Writing,Day -3
By - Gurumantra Civil Class
At - 2025-09-23 17:36:33
|
BPSC PYQ Mains Program Answer Writing
Session I – Polity + Bihar + Special + Current(IR) Day – 3
1. नीचे दिए गए प्रश्नों को सौ से डेढ़ सौ शब्दों में लिखे । Write down the following questions in a hundred to one hundred and fifty words. (a) भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार में 'आजाद दस्ता' की क्या भूमिका थी ? What role did the 'azad dasta' play in bihar during the quit india movement? (b) मौर्यकालीन मूर्ति कला के विशिष्ट लक्षण क्या हैं? What are the distinctive features of mauryan sculpture?
2.नीचे दिए गए प्रश्नों को सौ से डेढ़ सौ शब्दों में लिखे । Write down the following questions in a hundred to one hundred and fifty words. (a) एक बहुसदस्य निर्वाचन आयोग में मुख्य चुनाव आयोग की स्थिति का समीक्षा कीजिए एवं फोटो पहचान पत्र के संबंध में अपने विचार दीजिए। Examine the position of the chief election Commissioner in a multi member election commissioner and state your view regarding photo identity card. (b) भारत में राजनीति के अपराधिकरण की समस्या का समाधान हेतु वोहरा कमिटी के मुख्य सुझावों को बताएं। State the main recommendations of Vohra Committee for the resolution of the problems of criminalization of politics in india. 3. भारत- नेपाल संबंध की वर्तमान स्थिति का विश्लेषण कीजिये।दोनों देशों के बीच विवाद की बुनियादी बातें क्या है ? Discuss the present position of the indo- Nepal relations.What are the basic points of dispute between the two countries.(In 250 Words ) 📚 BPSC Mains Writing Practice – 40 Days Program (39th - 70th BPSC Mains PYQ – Complete Writing Practice)
⚡ 40 दिन का दमदार राइटिंग प्रोग्राम – सफलता की गारंटी की ओर पहला कदम! ⚡
✨ अब तैयारी होगी और भी सटीक ✨ 👉 विशेष रूप से 71st & 72nd BPSC Mains के लिए 👉 Offline + Online Mode में सुविधा 👉 साथ में Answer Module भी उपलब्ध
📅 Batch Start: 18 September 2025
📞 Admission Helpline: 9135904639 | 7250380187
App.- Gurumantra.online
🏛️ Offline Centre: Parwati Market, West Boring Canal Road, Beside Power Substation, Patna – 01
1(a) Ans.- ‘भारत छोड़ो आंदोलन‘ की शुरुआत 8 अगस्त 1942 में महात्मा गाँधी के द्वारा की गई थी। यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का अंतिम एवं व्यापक जन आंदोलन था, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की परिस्थितियां तथा क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद भारतीयों में निराशा के फलस्वरूप उत्तपन हुआ। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराना था। जुलाई 1942 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में गांधीजी ने आंदोलन चलाने की अनुमति मांगी, लेकिन इस बार कई नेताओं ने गांधीजी का तीव्र विरोध किया। इस समय गांधीजी सामरिक, आर्थिक तथा राजनीतिक परिस्थितियों के कारण काफी दुखी थें तथा कांग्रेस को चेतावनी देते हुए उन्होंने कह डाला कि “देश के मुट्ठी भर बालू से कांग्रेस से बड़ी संगठन खड़ा कर दूंगा”। बाद में कांग्रेस ने उन्हें आंदोलन करने की इजाजत दे दी। 8 अगस्त 1942 को गांधीजी ग्वालिया वाला टैंक मैदान बंबई में सभा आयोजित किया। जिसमें लाखों की भीड़ के सामने सरकार की तीखी आलोचना करते हुए “करो या मरो” का नारा दिया। इसके साथ ही ‘भारत छोड़ो आंदोलन’ पूरे देश में फैल गया। भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार की काफी महत्वपूर्ण भूमिका रही। 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित होते ही कांग्रेस के अधिकतर नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। इस गिरफ्तारी के बाद संपूर्ण देश में आंदोलन तीव्र हो गया। 9 अगस्त 1942 को राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तारी कर बांकीपुर सेंट्रल जेल भेज दिया गया। राजेंद्र प्रसाद की गिरफ्तारी का छात्रों द्वारा प्रबल विरोध किया गया। सभी शैक्षणिक केंद्रों पर हड़ताल रही इसी क्रम में 11 अगस्त को विद्यार्थियों के एक जुलूस ने सचिवालय भवन पर झंडा फहराने का प्रयास किया। जिसमें पटना के जिला कलेक्टर डब्लू.जी.आर्चर के आदेश पर देशभक्त छात्रों पर गोली चलाई गई जिसमें सात छात्र मारे गए। इस पूरी घटना को “सचिवालय गोलीकांड” के नाम से जाना जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1942 में ‘जयप्रकाश नारायण’ को गिरफ्तार कर हजारीबाग जेल में डाल दिया गया। लेकिन जयप्रकाश नारायण अपने चार साथियों सूर्य नारायण सिंह, योगेंद्र शुक्ल, शालिग्राम सिंह एवं गुलाली प्रसाद के साथ जेल से भाग निकले और नेपाल की तराई छेत्र में शरण ली। जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में नेपाल में युवकों को छापामार युद्ध का प्रशिक्षण देने के लिए ‘आजाद दस्ता’ का गठन किया गया। आजाद दस्ता का मुख्य उद्देश्य सरकार के विरुद्ध तोड़फोड़ करना था। 1943 तक आजाद दस्ता सक्रिय रूप से आंदोलन करता रहा परंतु नेपाल सरकार के सहयोग से ब्रिटिश सरकार द्वारा जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, अरुणा आसफ अली, शालिग्राम जी को गिरफ्तार कर लिया गया। जिसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन में जयप्रकाश नारायण इस समय भूमिगत गतिविधियों में सक्रिय रहें।
9 नवंबर 1942 को दीपावली की रात, वे अपने साथियों रामनंदन मिश्र, योगेंद्र शुक्ल और सूरज नारायण सिंह के साथ हजारीबाग सेंट्रल जेल से भाग निकले । इसके बाद उन्होंने ब्रिटिश शासन से लड़ने के लिए नेपाल की तराई के राजबिलास जंगल में 'आजाद दस्ता' नामक एक सशस्त्र गुरिल्ला बल की स्थापना की । इस दस्ते के प्रमुख उद्देश्य थे:- ब्रिटिश संपत्ति को नुकसान पहुंचाना । सरकार के खिलाफ तोड़फोड़ की कार्रवाइयों को अंजाम देना । छापामार युद्ध के माध्यम से विदेशी शासन को पंगु बनाना ।
प्रमुख गतिविधियाँ-
प्रमुख भूमिकाएँ:
दस्ते की मुख्य गतिविधियों में शामिल थे:- संचार साधनों को बाधित करना: टेलीफोन और तार सेवाओं को ठप कर दिया गया । यातायात को रोकना: रेल की पटरियां उखाड़ दी गईं । सरकारी इमारतों पर हमला: डाकघर, रेलवे स्टेशन, और थानों जैसी सरकारी इमारतों में आगजनी की गई ।
बिहार में प्रांतीय 'आजाद दस्ता' का नेतृत्व सूरज नारायण सिंह कर रहे थे । इस दस्ते का प्रभाव भागलपुर, मुंगेर, किशनगंज, पूर्णिया जैसे कई जिलों में फैला हुआ था ।
दमन और अंत- 'आजाद दस्ता' की बढ़ती गतिविधियों ने ब्रिटिश सरकार को चिंतित कर दिया। ब्रिटिश सरकार के दबाव में, नेपाल सरकार ने मई 1943 में जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, और अन्य नेताओं को गिरफ्तार कर लिया । इन गिरफ्तारियों के बावजूद, दस्ता 1943 तक सक्रिय रहा ।'आजाद दस्ता' के अलावा, बिहार में सियाराम दल जैसे अन्य गुप्त क्रांतिकारी संगठन भी सक्रिय थे, जिनका नेतृत्व सियाराम सिंह कर रहे थे और उनका प्रभाव भी कई जिलों में था । इन संगठनों ने आंदोलन को उस समय भी जीवित रखा जब अधिकांश बड़े नेता जेल में थे, और बिहार में आंदोलन को एक उग्र रूप प्रदान किया ।
(b) Ans.- मौर्य कला और वास्तुकला चौथी और दूसरी शताब्दी के बीच फली-फूली। यह राजवंश 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक चला। मौर्य साम्राज्य की कला और वास्तुकला स्तंभों, स्तूपों और विहारों के निर्माण की विशेषता थी। स्तंभ बलुआ पत्थर से बने थे। यह मौर्य कला और वास्तुकला की खासियतों में से एक थी। इन स्तंभों पर सम्राट अशोक के शिलालेख अंकित थे। स्तूप बड़े गुंबद के आकार की संरचनाएँ थीं जिनका उपयोग बौद्ध मंदिरों के रूप में किया जाता था। विहार बौद्ध भिक्षुओं के लिए आवासीय भवन थे। मौर्य कला को मुख्य रूप से मूर्तिकला के माध्यम से दर्शाया गया था। यह काल पत्थर की नक्काशी की कला के विकास के लिए जाना जाता है।
मौर्य कला और वास्तुकला की पृष्ठभूमि – मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 321 ईसा पूर्व में की थी। भारतीय इतिहास में यह एक महत्वपूर्ण समय था। हड़प्पा और मौर्यों के बीच के काल में पत्थरों से बनी इमारतों में गिरावट देखी गई।
मौर्यकालीन मूर्तिकला की सबसे प्रमुख विशेषता पॉलिशदार या चमकदार सतह वाले बलुआ पत्थर का उपयोग और कला का राजकीय (दरबारी) एवं लोक कला में विभाजन है । यह कला भारतीय मूर्तिकला के इतिहास में लकड़ी से पत्थर के उपयोग की ओर एक महत्वपूर्ण परिवर्तन दर्शाती है ।
मौर्यकालीन मूर्तिकला के विशिष्ट लक्षण निम्नलिखित हैं: चमकदार पॉलिश (ओपदार सतह): मौर्यकालीन मूर्तियों और स्तंभों पर एक विशेष प्रकार की पॉलिश की जाती थी, जो उन्हें शीशे की तरह चमकदार बनाती थी । यह तकनीक इतनी उन्नत थी कि आज भी सारनाथ जैसे स्तंभों पर यह चमक देखी जा सकती है । इसे “नर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर” (NBPW) संस्कृति की चमक के समान माना जाता है । पत्थर का व्यापक प्रयोग: इस काल में मूर्तिकला के लिए बड़े पैमाने पर पत्थर, विशेषकर चुनार के बलुआ पत्थर का उपयोग शुरू हुआ । इससे पहले वास्तुकला और मूर्तिकला में लकड़ी का अधिक प्रयोग होता था ।
कला का वर्गीकरण: मौर्यकालीन मूर्तिकला को दो मुख्य भागों में बांटा जा सकता है:
यथार्थवादी और स्वाभाविक चित्रण: मौर्यकालीन मूर्तिकारों ने पशुओं और मनुष्यों का अत्यंत स्वाभाविक और यथार्थवादी चित्रण किया है । सारनाथ के सिंह शीर्ष पर शेरों की उभरी हुई नसें, उनके शरीर का भारीपन और गतिशील मुद्रा उनके सजीव चित्रण को दर्शाते हैं ।
स्तंभों की विशिष्ट संरचना: अशोक के स्तंभों की अपनी विशेष संरचना है । स्तंभ यष्टि: यह नीचे से ऊपर की ओर पतली होती जाती है । शीर्ष भाग: यष्टि के ऊपर शीर्ष भाग होता है, जिसमें उल्टे कमल के आकार का घंटा, एक गोल या चौकोर चौकी (abacus), और चौकी पर स्थापित पशु-आकृति होती है । पशु आकृतियाँ: चौकी पर हाथी, घोड़ा, बैल और सिंह जैसी आकृतियाँ उकेरी गई हैं । स्तंभ के शिखर पर भी सिंह, बैल या हाथी जैसे पशुओं की भव्य मूर्तियाँ स्थापित हैं ।
प्रतीकात्मकता का प्रयोग: मौर्यकालीन मूर्तिकला में प्रतीकों का गहरा प्रयोग है। उदाहरण के लिए, सारनाथ स्तंभ के शीर्ष पर बना चक्र ‘धम्मचक्र’ का प्रतीक है, जो बुद्ध के पहले उपदेश (धर्म-चक्र-प्रवर्तन) को दर्शाता है । पशुओं का अंकन भी विभिन्न दिशाओं और जीवन के चरणों का प्रतीक माना जाता है ।
प्रमुख सामग्री- चुनार (वाराणसी के निकट) के बलुआ पत्थर: राजकीय मूर्तिकला खासकर अशोक स्तंभ, सिंह शीर्ष, यक्ष-यक्षिणी जैसी मूर्तियाँ इससे बनाई जाती थीं । चट्टान: गुफा निर्माण जैसे बाराबर, नागार्जुन की गुफाएँ भी चट्टान को काटकर बनाई गई थीं, जिनमें भी सतह की चमकीली पालिश दिखाई देती है । टेराकोटा (मृत्तिका): लोक कला और धार्मिक मूर्तियों में टेराकोटा का प्रयोग भी मिलता है, लेकिन राजकीय मूर्तियों में पत्थर ही प्रमुख था । लकड़ी: मौर्यकाल के प्रारंभिक निर्माण कार्य, जैसे पाटलिपुत्र के महल, मुख्यतः लकड़ी से बने थे, लेकिन मूर्तिकला में पत्थर का प्रयोग मौर्यकालीन नवाचार है ।
2(A) Ans.- भारत एक समाजवादी, धर्म निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य एवं विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। आधुनिक भारतीय राष्ट्र राज्य 15 अगस्त, 1947 को अस्तित्व में आया था। तब से संविधान में प्रतिस्थापित सिद्धान्तों, निर्वाचन विधियों तथा पद्धति के अनुसार नियमित अन्तराल पर स्वतंत्र तथा निष्पक्ष निर्वाचनों का संचालन किया गया है। भारत के संविधान ने संसद और प्रत्येक राज्य के विधान मंडल तथा भारत के राष्ट्रपति और उप राष्ट्रपति के पदों के निर्वाचनों के संचालन की पूरी प्रक्रिया का अधीक्षण, निदेशन तथा नियंत्रण का उत्तरदायित्व भारत निर्वाचन आयोग को सौंपा है।भारत निर्वाचन आयोग एक स्थायी संवैधानिक निकाय है। संविधान के अनुसार निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी, 1950 को की गई थी। प्रारम्भ में, आयोग में केवल एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। वर्तमान में इसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और दो निर्वाचन आयुक्त हैं। 16 अक्तूबर, 1989 को पहली बार दो अतिरिक्त आयुक्तों की नियुक्ति की गई थी परन्तु उनका कार्यकाल बहुत कम था जो 01 जनवरी, 1990 तक चला। तत्पश्चात, 01 अक्तूबर, 1993 को दो अतिरिक्त निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की गई थी। तब से आयोग की बहु-सदस्यीय अवधारणा प्रचलन में है, जिसमें निर्णय बहुमत के आधार पर लिया जाता है।
आयुक्तों की नियुक्ति एवं कार्यकाल- मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उनका कार्यकाल 6 वर्ष, या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, तक होता है। उनका दर्जा भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का होता है तथा उन्हें उनके समतुल्य ही वेतन और अनुलाभ मिलते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पद से केवल संसद द्वारा महाभियोग के माध्यम से ही हटाया जा सकता है। आयोग अपने कार्यों का निष्पादन, नियमित बैठकों के आयोजन और दस्तावेजों के परिचालन द्वारा भी करता है। आयोग द्वारा निर्णय लेने की प्रक्रिया में सभी निर्वाचन आयुक्तों के पास समान अधिकार होते हैं। समय-समय पर आयोग अपने सचिवालय में अपने अधिकारियों को कुछ कार्यकारी प्रकार्यों का प्रत्यायोजन करता है। भारतीय निर्वाचन आयोग (Election Commission of India - ECI) संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है, जो भारत में संघीय और राज्य स्तर पर चुनावों का संचालन करता है।
बहुसदस्य निर्वाचन आयोग में मुख्य चुनाव आयोग की स्थिति- भारत में निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त (Chief Election Commissioner - CEC) और दो अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। आयोग तीन सदस्यीय है, जिसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1989 को हुई। मुख्य चुनाव आयुक्त इस आयोग का प्रमुख होता है और उसके निर्णयों को अहम माना जाता है।चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और उनका कार्यकाल 6 वर्ष या उम्र 65 वर्ष (जो पहले हो) तक होता है। उन्हें भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान सम्मान और वेतन प्राप्त होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त को केवल संसद के महाभियोग के माध्यम से ही पद से हटाया जा सकता है, जबकि अन्य आयुक्तों को राष्ट्रपति हटा सकते हैं। इसका मतलब है कि मुख्य चुनाव आयुक्त की स्वतंत्रता और उच्च दर्जा सुनिश्चित होता है। बहुसदस्य आयोग में निर्णय लेने की प्रक्रिया में मतभेद होने पर मुख्य चुनाव आयुक्त की राय को प्राथमिकता दी जाती है, जिससे उनका नेतृत्व सुनिश्चित रहता है। आयोग का कार्य देश में चुनावों का स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं पारदर्शी आयोजन सुनिश्चित करना है, जिसमें संसद, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव शामिल हैं। एस.एस. धनोआ बनाम भारत संघ (1991) और टी.एन. शेषन बनाम भारत संघ (1995) जैसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि CEC और अन्य आयुक्तों की शक्तियां समान हैं, लेकिन CEC को प्रशासनिक प्रमुख की भूमिका दी गई है।2024 में सुप्रीम कोर्ट ने अनंत कुमार हेगड़े बनाम भारत संघ मामले में आयोग की स्वतंत्रता को मजबूत करने पर जोर दिया। बहुसदस्यीय ढांचा निर्णयों में संतुलन लाता है, लेकिन CEC की स्थिति को कमजोर करने का आरोप लगता है, क्योंकि पहले एकल सदस्यीय आयोग में CEC की शक्तियां अधिक केंद्रित थीं।
फोटो पहचान पत्र (EPIC) के संबंध में विचार- फोटो पहचान पत्र, जिसे इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड (EPIC) या मतदाता पहचान पत्र कहा जाता है, चुनाव आयोग द्वारा जारी किया जाता है और मतदाताओं की पहचान सुनिश्चित करने का प्रमुख साधन है। यह 1993 से लागू हुआ और अब डिजिटल रूप (e-EPIC) में भी उपलब्ध है।
सकारात्मक पहलू: धोखाधड़ी की रोकथाम: EPIC मतदान केंद्र पर पहचान साबित करता है, जिससे डुप्लिकेट वोटिंग या फर्जी मतदान कम होता है। इससे चुनाव प्रक्रिया पारदर्शी और विश्वसनीय बनती है। समावेशिता और गौरव: यह मतदाताओं को नागरिकता का प्रतीक प्रदान करता है, विशेषकर ग्रामीण और गरीब वर्गों में, जहां यह पहली आधिकारिक पहचान हो सकती है। डिजिटल e-EPIC मोबाइल ऐप के माध्यम से आसान पहुंच प्रदान करता है, जो पेपरलेस और पर्यावरण-अनुकूल है। बहुपयोगी: मतदान के अलावा, यह बैंक खाता खोलने, सरकारी योजनाओं और अन्य पहचान प्रमाण के रूप में काम करता है, जिससे नागरिकों की सुविधा बढ़ती है। आधार से लिंकिंग (वैकल्पिक) से मतदाता सूची की शुद्धता बढ़ सकती है।
नकारात्मक पहलू: पहुंच और लागत: ग्रामीण क्षेत्रों में EPIC प्राप्त करना मुश्किल हो सकता है, विशेषकर महिलाओं और अल्पसंख्यकों के लिए। डिजिटल संस्करण के लिए स्मार्टफोन और इंटरनेट की आवश्यकता से डिजिटल डिवाइड बढ़ता है। गोपनीयता और सुरक्षा: आधार से लिंकिंग से डेटा लीक का खतरा है, जो मतदाताओं की गोपनीयता भंग कर सकता है। कुछ मामलों में, EPIC का दुरुपयोग पहचान चोरी के लिए होता है। प्रशासनिक चुनौतियां: EPIC के बिना वैकल्पिक पहचान (जैसे पासपोर्ट) की अनुमति है, लेकिन इससे असंगति आती है। साथ ही, अपडेट और वितरण में देरी चुनावी भागीदारी प्रभावित करती है।
अतः EPIC चुनावी अखंडता के लिए आवश्यक है, लेकिन इसे अधिक समावेशी बनाने के लिए ऑफलाइन वितरण को मजबूत करना और डेटा सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहिए। डिजिटल संक्रमण सकारात्मक है, परंतु सभी वर्गों की पहुंच पर ध्यान देना जरूरी है।
2(b) Ans.- राजनीति का अपराधीकरण राजनीतिक क्षेत्र में आपराधिक तत्वों के उलझाव को दर्शाता है। यह चुनावी प्रक्रियाओं, राजनीतिक दलों और शासन में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों की सक्रिय भागीदारी और भागीदारी को दर्शाता है। ऐसे व्यक्तियों को आपराधिक अपराधों के लिए दोषी ठहराया जा सकता है, वे अवैध गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं या आपराधिक नेटवर्क से जुड़े हो सकते हैं। राजनीति के अपराधीकरण में न केवल राजनीति में उनकी भागीदारी शामिल है, बल्कि भ्रष्टाचार, प्रभाव-व्यापार और लोकतांत्रिक मूल्यों का क्षरण भी शामिल है।
भारत में राजनीति के अपराधीकरण के प्रमुख कारण –
वोहरा समिति की स्थापना की पृष्ठभूमि- केंद्रीय गृह सचिव एन.एन. वोहरा की अध्यक्षता में 9 जुलाई 1993 को बनी इस उच्चस्तरीय समिति की पहली बैठक 15 जुलाई 1993 को हुई। समिति का गठन मुख्यतः मार्च 1993 के मुंबई बम विस्फोट के बाद दाऊद इब्राहिम गिरोह तथा अन्य संगठित अपराधियों के राजनैतिक और नौकरशाही संरक्षण के संदेहास्पद संबंधों की जांच के लिए किया गया था। समिति की टर्म में गृह मंत्रालय के अलावा रॉ, आईबी, सीबीआई और विशेष सुरक्षा विभाग के शीर्ष अधिकारी शामिल थे। जैसा कि दृष्टि संस्थान बताता है, इस समिति का उद्देश्य “राजनीतिक-आपराधिक गठजोड़ की सीमा की पहचान करने और राजनीति के अपराधीकरण से प्रभावी ढंग से निपटने के तरीकों की सिफारिश करने” था।
आपराधिकरण पर समिति की मुख्य टिप्पणियाँ- वोहरा समिति की रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया कि देश में अपराधी गिरोह एक प्रकार से “समानांतर सरकार” की तरह कार्य कर रहे हैं और राजनेता इन गिरोहों के संरक्षक बन चुके हैं। रिपोर्ट में दाऊद इब्राहिम, इकबाल मिर्ची, मेमन बंधु आदि के नाम लिए गए और बताया गया कि इन माफियाओं ने वसूली, अवैध जमीन अतिक्रमण, हवलाखोरी जैसी आय के स्रोतों से राजनीतिक व नौकरशाही संपर्क बनाए। भारत के कई राज्यों (जैसे बिहार, यूपी, हरियाणा) में स्थानीय सशस्त्र गिरोहों को पार्टियों की आड़ मिली और अपराधी चुनाव जीतकर विधानसभा/संसद पहुँचे। उच्चतम न्यायालय ने भी 2018 में इस रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि इन एजेंसियों ने सर्वसम्मति से माना कि अपराधी-राजनेता-नौकरशाह गठजोड़ देश में कानून-व्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित कर रहा है। कोर्ट ने कहा कि समग्रतः पिछले दशक में स्थानीय निकायों, विधानसभाओं और संसद में कई अपराधी निर्वाचित हो चुके हैं।
समिति की प्रमुख सिफारिशें-
वोहरा समिति ने आपराधिक-राजनीतिक गठजोड़ से निपटने के लिए अनेक ठोस सुझाव दिए। मुख्य सुझावों में शामिल थे:
वोहरा समिति की रिपोर्ट सरकारी रिकॉर्ड में गुप्त रखी गई है और उसे सार्वजनिक नहीं किया गया। इसके बावजूद समय-समय पर अदालतों और आयोगों ने समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए कुछ कदम उठाए हैं:
सुझाव/उपाय - सरकारी कार्रवाई/स्थिति
अन्य महत्वपूर्ण तथ्य – एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) के आंकड़ों के अनुसार, 2004 से भारतीय संसद में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है। 2004 की लोकसभा में, 24% सांसदों पर आपराधिक मामले चल रहे थे, जो 2019 में बढ़कर 43% हो गए। फरवरी 2023 में दायर एक याचिका में 2009 से घोषित आपराधिक मामलों वाले सांसदों में 44% की वृद्धि पर प्रकाश डाला गया। 2019 के चुनावों के दौरान, 159 सांसदों पर बलात्कार, हत्या, हत्या के प्रयास, अपहरण और महिलाओं के खिलाफ अपराध जैसे गंभीर आरोप पाए गए। हाल ही में निर्वाचित 18वीं लोकसभा (2024) में, ADR ने बताया कि 43% सांसदों ने आपराधिक मामले घोषित किए हैं, जिनमें से 29% पर गंभीर आपराधिक आरोप हैं। यह प्रवृत्ति भारत में राजनीति के अपराधीकरण के बढ़ते सामान्यीकरण को रेखांकित करती है। पार्टीवार तौर पर देखें तो भाजपा में आपराधिक मामलों वाले सांसदों की संख्या सबसे अधिक है, उसके बाद कांग्रेस का स्थान है, सभी प्रमुख पार्टियां लंबित आरोपों वाले उम्मीदवारों को मैदान में उतारती हैं, तथा अक्सर स्वच्छ रिकॉर्ड की तुलना में “जीतने की संभावना” को प्राथमिकता देती हैं।
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गए आदेश के प्रमुख बिंदु –
सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार, राजनीतिक दलों (केंद्र व राज्य स्तर पर) को अपने चयनित उम्मीदवारों पर चल रहे आपराधिक मामलों की विस्तृत जानकारी अपने वेबसाइट पर साझा करनी होगी। इसमें अपराध की प्रकृति, चार्टशीट, संबंधित न्यायालय का नाम और केस नंबर आदि जानकारियाँ शामिल हैं। आदेश के अनुसार, प्रत्याशी पर दर्ज मामलों की विस्तृत जानकारी को एक राष्ट्रीय और एक स्थानीय भाषा के अखबार में प्रकाशित करने के साथ दल के आधिकारिक सोशल मीडिया खातों जैसे-फेसबुक, ट्विटर आदि पर भी साझा करना होगा। यह अनिवार्य रूप से उम्मीदवारों के चयन के 48 घंटे के भीतर या नामांकन दाखिल करने की पहली तारीख के दो सप्ताह से कम समय में (जो भी पहले हो) प्रकाशित किया जाना चाहिये। सर्वोच्च न्यायालय ने राजनीतिक दलों को आदेश दिया कि वे भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) के सामने 72 घंटे के भीतर अदालती कार्रवाई की अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करें अन्यथा उन दलों पर न्यायालय की अवमानना से संबंधित कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही राजनीतिक दलों को संबंधित प्रत्याशी के चयन का कारण बताना होगा और यह भी बताना होगा कि संबंधित प्रत्याशी के स्थान पर बिना आपराधिक पृष्ठभूमि वाले किसी अन्य व्यक्ति का चयन क्यों नहीं किया जा सका। न्यायालय ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया है कि प्रत्याशी के रूप में चयन का कारण व्यक्ति की योग्यता, उपलब्धियों आदि के संदर्भ में होना चाहिये न कि उसकी चुनाव जीतने की क्षमता (Winnability) के संदर्भ में।
राजनीति के अपराधीकरण का प्रभाव – देश की राजनीति और कानून निर्माण प्रक्रिया में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों की उपस्थिति का लोकतंत्र की गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। राजनीति के अपराधीकरण के कारण चुनावी प्रक्रिया में काले धन का प्रयोग काफी अधिक बढ़ जाता है। राजनीति के अपराधीकरण का देश की न्यायिक प्रक्रिया पर भी प्रभाव देखने को मिलता है और अपराधियों के विरुद्ध जाँच प्रक्रिया धीमी हो जाती है। राजनीति में प्रवेश करने वाले अपराधी सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं और नौकरशाही, कार्यपालिका, विधायिका तथा न्यायपालिका सहित अन्य संस्थानों पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। राजनीति का अपराधीकरण समाज में हिंसा की संस्कृति को प्रोत्साहित करता है और भावी जनप्रतिनिधियों के लिये एक गलत उदाहरण प्रस्तुत करता है।
भारतीय चुनावी तंत्र में सुधार के पूर्व प्रयास – 1. दिनेश गोस्वामी समिति (1990): समिति ने अपनी रिपोर्ट में चुनावी खर्च पर नियंत्रण, कंपनियों द्वारा दिये गए चंदे पर रोक, चुनावों में राज्य की भूमिका और इसके साथ ही चुनावों के अन्य पहलुओं जैसे- प्रचार का समय, आयु सीमा, चुनाव आयोग के अधिकार आदि के संबंध में निगरानी और प्रावधानों की सिफारिश की। 2. वोहरा समिति (1993): वोहरा समिति ने राजनीति में बढ़ते अपराधीकरण और उनके राजनीतिक संरक्षण पर चिंता व्यक्त करते हुए इस समस्या के समाधान के लिये विभिन्न अपराध नियंत्रण संस्थाओं (सीबीआई, इनकम टैक्स, नारकोटिक्स आदि) की सहायता लेने की सलाह दी। 3. इन्द्रजीत गुप्ता समिति (1998): गुप्ता समिति ने अपनी रिपोर्ट में राजनीति में भ्रष्टाचार और अपराध को कम करने के लिये राज्य द्वारा चुनावी खर्च वहन किये जाने की सिफारिश की। 4. विधि आयोग रिपोर्ट (1999): वर्ष 1999 में विधि आयोग ने अपनी 170वीं रिपोर्ट में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनावों को एक साथ कराने का समर्थन किया था। 5. एमएन वैंकट चलैया समिति (2000-02)- विधि आयोग, चुनाव आयोग, संविधान की समीक्षा के लिये राष्ट्रीय आयोग की रिपोर्ट। 6. वांचू समिति (प्रत्यक्ष कर जाँच समिति)- वांचू समिति ने राजनीतिक चंदे के विनियमन के साथ राजनीतिक दलों की अन्य आर्थिक गतिविधियों पर अपनी रिपोर्ट जारी की।
चुनाव सुधार पर सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका –
अक्तूबर 1974 में सर्वोच्च न्यायालय ने कँवर लाल गुप्ता बनाम अमर नाथ चावला व अन्य मामले में प्रत्याशी के प्रचार पर होने वाले किसी भी प्रकार के खर्च (पार्टी प्रायोजक या किसी समर्थक द्वारा) को प्रत्याशी के लिये निर्धारित सीमा में जोड़ने का निर्देश दिया। वर्ष 2002 में सर्वोच्च न्यायालय ने भारत सरकार बनाम एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफाॅर्म वाद में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा कि संसद, राज्य विधानसभाओं या नगर निगम के लिये चुनाव लड़ने वाले प्रत्येक उम्मीदवार को अपनी आपराधिक, वित्तीय और शैक्षिक पृष्ठभूमि की घोषणा करनी होगी। वर्ष 2005 में रमेश दलाल बनाम भारत सरकार वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एक संसद सदस्य (सांसद) या राज्य विधानमंडल के सदस्य (विधायक) को दोषी ठहराए जाने पर चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहराया जाएगा और उसे अदालत द्वारा 2 वर्ष से कम कारावास की सज़ा नहीं दी जाएगी। वर्ष 2017 के एक महत्त्वपूर्ण फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रत्याशियों के लिये अपनी आपराधिक पृष्ठभूमि से संबंधित जानकारी सार्वजानिक करने की अनिवार्यता को दोहराते हुए, राजनीतिज्ञों पर चल रहे आपराधिक मामलों की सुनवाई के लिये फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना करने का आदेश दिया।
आलोचनात्मक विश्लेषण – वोहरा समिति की सिफारिशें संस्था एवं विधि सुधार की दिशा में व्यावहारिक थीं, लेकिन उन्हें लागू करने में अनेक अड़चनें आईं। रिपोर्ट गोपनीय रखने के चलते उस पर भरोसेमंद कार्रवाई बाधित रही। सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी की कि सरकार द्वारा गठित नोडल एजेंसी असंतोषजनक थी और उसमें स्वतंत्रता का अभाव था। राष्ट्रीय इच्छाशक्ति की कमी एवं राजनीतिक प्रतिरोध के कारण कई सुझाव धरातल पर नहीं उतर सके। दूसरी ओर, अर्धनिष्पादित बदलाव हुए हैं: निर्वाचन आयोग और अदालतों ने कई सुधार लागू किए, जैसे प्रत्याशियों को अपराधी अतीत घोषित करना अनिवार्य किया, दोषी सांसदों को अयोग्य ठहराया (एलिली थॉमस), और उम्मीदवारों की जानकारी सार्वजनिक करने का आदेश दिया। फिर भी, इनके बावजूद भारत की राजनीति में अपराधीकरण पूरी तरह रुक नहीं पाया है। राजनीतिक दल अब भी अपराधियों को टिकट देते हैं, क्योंकि वे धनबल और बाहुबल से वोट बैंक प्रभावित करते हैं। कुल मिलाकर, समिति ने अपराधी-राजनेता-नौकरशाह गठजोड़ पर गहरी चिन्ता जताई और सुधार के ठोस उपाय बताए, पर इनका अधिकांश हिस्सा अवलंबित रहा। विस्तृत प्रगति असाधारण तर्क और कानूनी बाधाओं (जैसे म्यूनिसिपल चुनावों में उच्चतम न्यायालय का कहना कि आरोप मात्र पर अयोग्यता नहीं) के चलते अधूरी रह गई है। परिणामतः, नीति-निर्माता और न्यायिक हस्तक्षेपों के बावजूद राजनीति का अपराधीकरण की समस्या बनी हुई है। यह संकेत है कि व्यापक सुधार के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति, पारदर्शिता और संस्थागत मजबूती आवश्यक है।
क्या कहता है जन-प्रतिनिधित्व अधिनियम? जन-प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 दोषी राजनेताओं को चुनाव लड़ने से रोकती है। लेकिन ऐसे नेता जिन पर केवल मुकदमा चल रहा है, वे चुनाव लड़ने के लिये स्वतंत्र हैं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन पर लगा आरोप कितना गंभीर है। इस अधिनियम की धारा 8(1) और 8(2) के अंतर्गत प्रावधान है कि यदि कोई विधायिका सदस्य (सांसद अथवा विधायक) हत्या, बलात्कार, अस्पृश्यता, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के उल्लंघन; धर्म, भाषा या क्षेत्र के आधार पर शत्रुता पैदा करना, भारतीय संविधान का अपमान करना, प्रतिबंधित वस्तुओं का आयात या निर्यात करना, आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होना जैसे अपराधों में लिप्त होता है, तो उसे इस धारा के अंतर्गत अयोग्य माना जाएगा एवं 6 वर्ष की अवधि के लिये अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। वहीं, इस अधिनियम की धारा 8(3) में प्रावधान है कि उपर्युक्त अपराधों के अलावा किसी भी अन्य अपराध के लिये दोषी ठहराए जाने वाले किसी भी विधायिका सदस्य को यदि दो वर्ष से अधिक के कारावास की सज़ा सुनाई जाती है तो उसे दोषी ठहराए जाने की तिथि से आयोग्य माना जाएगा। ऐसे व्यक्ति को सज़ा पूरी किये जाने की तिथि से 6 वर्ष तक चुनाव लड़ने के लिये अयोग्य माना जाएगा।
चुनौतियाँ – सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में राजनीति में शामिल आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों पर प्रत्यक्ष कार्रवाई के बजाय यह निर्णय राजनीतिक दलों और जनता के विवेक पर छोड़ दिया है। ऐसे में न्यायालय के आदेश से राजनीति में जल्दी बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं की जा सकती। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश में चुनाव आयोग को आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों पर कार्रवाई के स्थान पर उनकी निगरानी करने और इस संबंध में नियमानुसार न्यायालय को सूचित करने के निर्देश दिये गए हैं। यह व्यवस्था राजनीतिक अपराधियों को लेकर पहले से ही लंबी न्यायिक प्रक्रिया पर समाधान प्रदान करने की बजाय उसे और अधिक जटिल बनाती है। राजनैतिक पारदर्शिता के संदर्भ में न्यायालय का यह आदेश तभी प्रभावी हो सकता है जब राजनैतिक दल इस संदर्भ में नियमों का सही पालन करें और जनहित का ध्यान रखते हुए सही जानकारी दें। परंतु गलत/झूठे समाचारों (Fake News) के इस दौर में जनता तक सही जानकारी को पहुँचाना बहुत ही कठिन है, अतः न्यायालय के आदेश से राजनीति में बड़े सुधारों की उम्मीद नहीं की जा सकती।
निष्कर्ष- देश की राजनीति में अपराधियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए यह आवश्यक हो गया है कि संसद ऐसा कानून लाए ताकि अपराधी राजनीति से दूर रहें। जन प्रतिनिधि के रूप में चुने जाने वाले लोग अपराध की राजनीति से ऊपर हों। राष्ट्र को संसद द्वारा कानून बनाए जाने का इंतजार है। भारत की दूषित हो चुकी राजनीति को साफ करने के लिये बड़ा प्रयास किये जाने की आवश्यकता है।
भारत और नेपाल के बीच संबंध ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और भौगोलिक रूप से गहरे जुड़े हुए हैं। दोनों देशों के बीच 1,751 किलोमीटर लंबी खुली सीमा है, जो सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों से लगती है। 1950 की शांति और मैत्री संधि इन संबंधों का आधार है, जो दोनों देशों को एक-दूसरे के नागरिकों को समान अधिकार प्रदान करती है। हालांकि, 2025 में संबंधों की स्थिति मिश्रित है—एक ओर मजबूत आर्थिक सहयोग और सांस्कृतिक बंधन हैं, वहीं दूसरी ओर राजनीतिक अस्थिरता, सीमा विवाद और बाहरी शक्तियों (जैसे चीन और अमेरिका) का प्रभाव चुनौतियां पैदा कर रहा है। सकारात्मक पहलू: 1. आर्थिक सहयोग: भारत नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, जो नेपाल के कुल विदेशी व्यापार का लगभग 64% हिस्सा रखता है। 2025 में द्विपक्षीय व्यापार 8 अरब डॉलर से अधिक पहुंच गया है। भारत नेपाल को ईंधन, दवाएं और अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करता है। ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ा है, जैसे नेपाल से भारत को बिजली निर्यात। इसके अलावा, भारतीय निवेश नेपाल में 35% से अधिक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) का हिस्सा है। 2. सांस्कृतिक और मानवीय संबंध: लाखों नेपाली भारत में काम करते हैं (करीब 6 लाख), और भारतीय पर्यटक नेपाल की अर्थव्यवस्था को समर्थन देते हैं। 2025 में दोनों देशों के बीच संयुक्त परियोजना निगरानी समिति की बैठकें हुईं, जो विकास परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करती हैं। 3. रणनीतिक सुधार: अगस्त 2025 में नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को भारत यात्रा का निमंत्रण मिला, जो संबंधों में सुधार का संकेत है। पहले ओली की चीन-समर्थक नीतियां विवादास्पद रहीं, लेकिन अब संवाद बढ़ रहा है।
नकारात्मक पहलू और चुनौतियां:- 1. नेपाल की राजनीतिक अस्थिरता: सितंबर 2025 में नेपाल में बड़े पैमाने पर युवा-प्रेरित प्रदर्शन हुए, जिससे सरकार गिर गई और अंतरिम सरकार बनी। ये प्रदर्शन भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध (जैसे सोशल मीडिया बैन) के खिलाफ थे। भारत ने इस पर सतर्कता बरती, भारतीय नागरिकों को सावधानी बरतने की सलाह दी और सीमा पर जांच बढ़ाई। यह अस्थिरता भारत की पड़ोसी नीति को प्रभावित कर रही है, क्योंकि नेपाल तीसरा ऐसा पड़ोसी देश बन गया है जहां हाल के वर्षों में हिंसक उथल-पुथल से सरकार बदली (श्रीलंका और बांग्लादेश के बाद)। 2. बाहरी प्रभाव: चीन और अमेरिका दोनों नेपाल की स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। ओली ने लिपुलेख मुद्दे पर चीन से मदद मांगी, लेकिन चीन ने इसे द्विपक्षीय मुद्दा बताकर हस्तक्षेप से इनकार कर दिया। वहीं, कुछ विश्लेषणों में कहा गया है कि अमेरिका नेपाल को भारत के खिलाफ सीमा विवाद को हथियार बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकता है, विशेषकर भारत-पाकिस्तान तनाव के संदर्भ में। यह भारत की क्षेत्रीय सुरक्षा को प्रभावित कर सकता है।
समग्र विश्लेषण: 2025 में संबंध स्थिर लेकिन तनावपूर्ण हैं। नेपाल की आंतरिक अशांति से भारत को शरणार्थी प्रवाह, सीमा तस्करी और निवेश जोखिम का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि, दोनों देशों के बीच सहयोग जारी है, और भारत नेपाल की संप्रभुता का सम्मान करते हुए संवाद पर जोर दे रहा है। भविष्य में, अगर नेपाल की नई सरकार भारत-अनुकूल साबित होती है, तो संबंध मजबूत हो सकते हैं, लेकिन चीन का प्रभाव और सीमा विवाद बाधा बने रहेंगे।
दोनों देशों के बीच विवाद की बुनियादी बातें- भारत और नेपाल के बीच विवाद मुख्य रूप से सीमा, आर्थिक निर्भरता और राजनीतिक मुद्दों पर केंद्रित हैं। ये विवाद 1816 की सुगौली संधि से उपजे हैं, जो ब्रिटिश भारत और नेपाल के बीच सीमा निर्धारित करती है। मुख्य बुनियादी बातें निम्नलिखित हैं:
हाल ही में भारतीय प्रधान मंत्री ने बुद्ध के जन्मस्थान, लुंबिनी, नेपाल का दौरा किया, जहाँ उन्होंने नेपाल के प्रधान मंत्री के साथ भारतीय सहायता से बनाए जा रहे बौद्ध विहार के लिये आधारशिला रखी। जुलाई, 2021 में शपथ लेने के बाद नेपाल के प्रधान मंत्री ने भारत की अपनी पहली द्विपक्षीय यात्रा भी की। यह यात्रा कनेक्टिविटी परियोजनाओं को शुरू करने और समझौता ज्ञापन (MOU) पर हस्ताक्षर करने के मामले में सफल रही।
ऐतिहासिक संबंध – नेपाल भारत का एक महत्त्वपूर्ण पड़ोसी है और सदियों से चले आ रहे भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों / संबंधों के कारण अपनी विदेश नीति में एक विशेष महत्त्व रखता है। भारत और नेपाल हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म के संदर्भ में बुद्ध के जन्मस्थान लुंबिनी के साथ समान संबंध साझा करते हैं जो वर्तमान नेपाल में स्थित है।दोनों देश न केवल एक खुली सीमा और लोगों की निर्बाध आवाजाही साझा करते हैं, बल्कि विवाह और पारिवारिक संबंधों के माध्यम से भी उनके बीच घनिष्ठ संबंध हैं, जिन्हें रोटी-बेटी का रिश्ता के नाम से जाना जाता है।वर्ष 1950 की शांति और मित्रता की भारत-नेपाल संधि भारत और नेपाल के बीच मौजूद विशेष संबंधों का आधार है।
वर्ष 1950 की शांति और मित्रता की संधि – यह संधि दोनों देशों में निवास, संपत्ति, व्यापार और आवाजाही में भारतीय और नेपाली नागरिकों के पारस्परिक व्यवहार के बारे में बताती है। यह भारतीय और नेपाली दोनों व्यवसायों के लिये राष्ट्रीय व्यवहार भी स्थापित करता है (अर्थात, एक बार आयात किये जाने के बाद, विदेशी वस्तुओं को घरेलू सामानों से अलग नहीं माना जाएगा)। यह भारत द्वारा नेपाल को हथियारों तक पहुँच भी सुनिश्चित करता है।
भारत के लिये नेपाल का महत्त्व –
दोनों देशों के बीच सहयोग के क्षेत्र – व्यापार और अर्थव्यवस्था: बाकी दुनिया से व्यापार के लिये पारगमन प्रदान करने के अलावा, भारत नेपाल का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार और विदेशी निवेश का सबसे बड़ा स्रोत है। वर्ष 2018-19 में कुल द्विपक्षीय व्यापार 57,858 करोड़ रुपए (8.27 अरब अमेरिकी डॉलर) तक पहुँच गया। वर्ष 2018-19 में, जबकि भारत में नेपाल का निर्यात 3558 करोड़ रुपए (US$508 मिलियन) था, नेपाल को भारत का निर्यात 54,300 करोड़ रुपए (7.76 बिलियन अमेरिकी डॉलर) था। विनिर्माण, सेवाओं (बैंकिंग, बीमा, शुष्क बंदरगाह), बिजली क्षेत्र और पर्यटन उद्योग आदि में लगी भारतीय फर्में।
कनेक्टिविटी: नेपाल एक भू-आबद्ध देश होने के कारण तीन तरफ से भारत से घिरा हुआ है और एक तरफ तिब्बत की ओर खुला है जहाँ बहुत सीमित वाहनों की पहुँच है।भारत-नेपाल ने लोगों से लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिये विभिन्न संपर्क कार्यक्रम शुरू किये हैं।भारत में काठमांडू को रक्सौल से जोड़ने वाला इलेक्ट्रिक रेल ट्रैक बिछाने के लिये दोनों सरकारों के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गए हैं।भारत व्यापार और पारगमन व्यवस्था के ढांचे के भीतर कार्गो की आवाजाही के लिये अंतर्देशीय जलमार्ग विकसित करना चाहता है, नेपाल को सागर (हिंद महासागर) के साथ सागरमाथा (माउंट एवरेस्ट) को जोड़ने के लिये समुद्र तक अतिरिक्त पहुँच प्रदान करता है।
विकास सहायता: भारत सरकार जमीनी स्तर पर बुनियादी ढाँचे के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करते हुए, नेपाल को विकास सहायता प्रदान करती है।सहायता के क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य, जल संसाधन और शिक्षा और ग्रामीण और सामुदायिक विकास शामिल हैं।
रक्षा सहयोग: द्विपक्षीय रक्षा सहयोग में उपकरण और प्रशिक्षण के प्रावधान के माध्यम से नेपाली सेना को उसके आधुनिकीकरण में सहायता देना शामिल है। भारतीय सेना की गोरखा रेजीमेंटों का गठन आंशिक रूप से नेपाल के पहाड़ी ज़िलों से भर्ती करके किया जाता है।भारत वर्ष 2011 से हर साल नेपाल के साथ एक संयुक्त सैन्य अभ्यास करता है जिसे ‘सूर्य किरण’ के नाम से जाना जाता है। सांस्कृतिक: नेपाल के विभिन्न स्थानीय निकायों के साथ कला और संस्कृति, शिक्षाविदों और मीडिया के क्षेत्र में लोगों से लोगों के संपर्क को बढ़ावा देने की पहल की गई है। भारत ने काठमांडू-वाराणसी, लुंबिनी-बोधगया और जनकपुर-अयोध्या को जोड़ने के लिये तीन सिस्टर-सिटी समझौतों पर हस्ताक्षर किये हैं।
मानवीय सहायता: नेपाल संवेदनशील पारिस्थितिक नाजुक क्षेत्र में स्थित है, जो भूकंप और बाढ़ से ग्रस्त है, जिससे जीवन और धन दोनों को भारी नुकसान होता है, जिससे यह भारत की मानवीय सहायता का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बना रहता है। भारतीय समुदाय: नेपाल में बड़ी संख्या में भारतीय रहते हैं, इनमें व्यवसायी, व्यापारी, डॉक्टर, इंजीनियर और मजदूर (निर्माण क्षेत्र में मौसमी/प्रवासी सहित) शामिल हैं।
बहुपक्षीय साझेदारी: भारत और नेपाल बीबीआईएन (बांग्लादेश, भूटान, भारत और नेपाल), बिम्सटेक (बहु क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिये बंगाल की खाड़ी पहल), गुटनिरपेक्ष आंदोलन, और सार्क (क्षेत्रीय सहयोग के लिये दक्षिण एशियाई संघ) जैसे कई बहुपक्षीय मंचों को साझा करते हैं। आदि। हाल के घटनाक्रम क्या हैं? अरुण -3 जल विद्युत परियोजना: वर्ष 2019 में कैबिनेट ने अरुण -3 पनबिजली परियोजना के लिये ₹1236 करोड़ के निवेश को भी मंजूरी दी।अरुण -3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना (900 मेगावाट) पूर्वी नेपाल में अरुण नदी पर स्थित एक रन-ऑफ-रिवर है। बिल्ड ऑन ऑपरेट एंड ट्रांसफर (BOOT): वर्ष 2008 में परियोजना के लिये नेपाल सरकार और सतलुज जल विकास निगम (SJVN) लिमिटेड के बीच पांच साल की नर्म अवधि सहित 30 साल की अवधि के लिये बिल्ड ओन ऑपरेट एंड ट्रांसफर (BOOT) आधार पर निष्पादन के लिये एक समझौता ज्ञापन (MOU) पर हस्ताक्षर किये गए थे।
बौद्ध संस्कृति और विरासत के लिये अंतर्राष्ट्रीय केंद्र:भारत के प्रधान मंत्री की यात्रा के दौरान, उन्होंने लुंबिनी मठ क्षेत्र में भारत अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्कृति और विरासत केंद्र के निर्माण का शुभारंभ करने के लिये ‘शिलान्यास’ समारोह किया। बौद्ध धर्म के आध्यात्मिक पहलुओं के सार का आनंद लेने के लिये दुनिया भर से तीर्थयात्रियों और पर्यटकों का स्वागत करने के लिये यह केंद्र एक विश्व स्तरीय सुविधा प्रदान करेगी। इस सुविधा का उद्देश्य दुनिया भर के उन विद्वानों और बौद्ध तीर्थयात्रियों के लिये खानपान का प्रबंध करना है जो लुंबिनी आते हैं।
जल विद्युत परियोजनाएँ: दोनों नेताओं ने 490.2 मेगावाट अरुण-4 जलविद्युत परियोजना के विकास और कार्यान्वयन के लिये सतलुज जल विद्युत निगम (SJVN) लिमिटेड और नेपाल विद्युत प्राधिकरण (NEA) के बीच पांच समझौतों पर हस्ताक्षर किये। नेपाल ने भारतीय कंपनियों को नेपाल में पश्चिम सेती जलविद्युत परियोजना में निवेश करने के लिये भी आमंत्रित किया।
सैटेलाइट कैंपस की स्थापना: भारत ने रूपन्देही में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) का एक उपग्रह परिसर स्थापित करने की पेशकश की है और भारतीय और नेपाली विश्वविद्यालयों के बीच हस्ताक्षर करने के लिये कुछ मसौदा समझौता ज्ञापन भेजा है।
पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना: नेपाल ने कुछ लंबित परियोजनाओं पर चर्चा की, जैसे पंचेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना, 1996 में नेपाल और भारत के बीच हस्ताक्षरित महाकाली संधि की एक महत्त्वपूर्ण शाखा, और पश्चिम सेती जलविद्युत परियोजना, एक जलाशय-प्रकार की परियोजना, जिसकी अनुमानित क्षमता 1,200 मेगावाट है।
सीमा पार रेल लिंक: जयनगर (बिहार) से कुर्था (नेपाल) तक 35 किलोमीटर के क्रॉस-बॉर्डर रेल लिंक के संचालन को आगे बिजलपुरा और बर्दीबास तक बढ़ाया जाएगा।
डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन: एक अन्य परियोजना में 90 किमी लंबी 132 केवी डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन शामिल है जो टीला (सोलुखुम्बु) को भारतीय सीमा के करीब मिरचैया (सिराहा) से जोड़ती है।
बहुपक्षीय परियोजनाएँ: इसके अतिरिक्त, रेलवे क्षेत्र में तकनीकी सहयोग प्रदान करने वाले समझौतों, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में नेपाल के शामिल होने और पेट्रोलियम उत्पादों की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिये इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और नेपाल ऑयल कॉरपोरेशन के बीच भी समझौतों पर हस्ताक्षर किये गए।
प्रमुख चुनौतियाँ – प्रादेशिक विवाद: भारत-नेपाल संबंधों में मुख्य चुनौतियों में से एक कालापानी सीमा मुद्दा है। इन सीमाओं को वर्ष 1816 में अंग्रेजों द्वारा तय किया गया था और भारत को वे क्षेत्र विरासत में मिले थे जिन पर अंग्रेजों ने वर्ष 1947 में क्षेत्रीय नियंत्रण का प्रयोग किया था। जबकि भारत-नेपाल सीमा का 98% सीमांकन किया गया था, दो क्षेत्र, सुस्ता और कालापानी का निर्णय अधर में था। वर्ष 2019 में नेपाल ने उत्तराखंड के कालापानी, लिंपियाधुरा और लिपुलेख और सुस्ता (पश्चिम चंपारण जिला, बिहार) के क्षेत्र को नेपाल के क्षेत्र के हिस्से के रूप में दावा करते हुए एक नया राजनीतिक मानचित्र जारी किया।
शांति और मैत्री संधि के मुद्दे: वर्ष 1950 में शांति और मित्रता की संधि नेपाली अधिकारियों द्वारा वर्ष 1949 में ब्रिटिश भारत के साथ उनके विशेष संबंधों को जारी रखने और उन्हें एक खुली सीमा और भारत में काम करने का अधिकार प्रदान करने के लिये मांगी गई थी। लेकिन आज इसे एक असमान संबंध और भारतीय प्रभाव थोपने के एक संकेत के रूप में देखा जाता है। इसे बेहतर करने का विचार वर्ष 1990 के दशक के मध्य से संयुक्त वक्तव्यों में किया गया लेकिन छिटपुट और अपमानजनक तरीके से।
विमुद्रीकरण के कारण अड़चन: नवंबर 2016 में भारत ने उच्च मूल्य के 15.44 ट्रिलियन रुपये (1,000 रुपये और 500 रुपये) के नोट वापस ले लिये । आज 15.3 ट्रिलियन रुपये से अधिक की वापसी हुई है। फिर भी कई नेपाली नागरिक जो कानूनी रूप से 25,000 रुपये की भारतीय मुद्रा रखने के हकदार थे (यह देखते हुए कि नेपाली रुपया भारतीय रुपये के लिये आंका गया है) उन्हें लाचार छोड़ दिया गया। नेपाल राष्ट्र बैंक (सेंट्रल बैंक ऑफ नेपाल) के पास 7 करोड़ रुपये हैं और सार्वजनिक होल्डिंग का अनुमान 500 करोड़ रुपये है। नेपाल राष्ट्र बैंक के पास विमुद्रीकृत बिलों को स्वीकार करने से भारत द्वारा इनकार और प्रतिष्ठित व्यक्तियों के समूह (EPG) द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर लंबित निर्णय ने नेपाल में भारत की एक बेहतर छवि हासिल करने में मदद नहीं की है।
चीन का हस्तक्षेप:
अन्य महत्वपूर्ण तथ्य –
भविष्य के लिए महत्वपूर्ण कदम –
नेपाल में हालिया राजनीतिक विवाद- 2025 में नेपाल में बड़े पैमाने पर राजनीतिक उथल-पुथल देखी गई, जो मुख्य रूप से सितंबर में शुरू हुई Gen Z (जेनरेशन Z) युवा-प्रेरित विरोध प्रदर्शनों से उपजी है। ये प्रदर्शन नेपाल की राजधानी काठमांडू सहित पूरे देश में फैले और सरकार को गिराने में सफल रहे। मुख्य कारण और घटनाक्रम निम्नलिखित हैं: प्रदर्शनों का ट्रिगर: प्रदर्शन मुख्य रूप से भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, आर्थिक असमानता, नेपोटिज्म (परिवारवाद) और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध के खिलाफ थे। सरकार द्वारा लगाए गए सोशल मीडिया बैन ने आग में घी का काम किया, जो युवाओं के लिए संचार और अभिव्यक्ति का प्रमुख माध्यम था। ये प्रदर्शन छात्रों और युवा नागरिकों द्वारा आयोजित किए गए, जो दशकों से जमा सिस्टेमिक रोट (प्रणालीगत सड़ांध) से तंग आ चुके थे। घटनाक्रम और हिंसा: प्रदर्शन 48 घंटों में तेजी से बढ़े, जिसमें पुलिस के साथ संघर्ष हुए। कम से कम 72 लोगों की मौत हुई (जिनमें 21 नागरिक और 3 पुलिसकर्मी शामिल हैं) और 1,300 से अधिक घायल हुए। प्रदर्शनकारियों ने संसद, सुप्रीम कोर्ट, सरकारी इमारतों और राजनीतिक नेताओं के घरों में आग लगा दी। जेल ब्रेक से सैकड़ों कैदी भाग निकले, जिससे सुरक्षा संकट बढ़ गया। नेपाल की सेना ने काठमांडू और प्रमुख शहरों में कर्फ्यू लगा दिया और नियंत्रण संभाला। मुख्य अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बंद रहा और उड़ानें डायवर्ट की गईं। सरकार का पतन और नई व्यवस्था: प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया और सैन्य छावनी में चले गए। संसद भंग कर दी गई। प्रदर्शनकारियों के दबाव में पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया, जो नेपाल की पहली महिला PM हैं। वे एंटी-करप्शन स्टैंड के लिए जानी जाती हैं और युवाओं ने उन्हें डिस्कॉर्ड वोट से नामित किया। चुनाव मार्च 2026 में होने वाले हैं। ये विवाद नेपाल की राजनीति में एक नई पीढ़ी के उदय को दर्शाते हैं, लेकिन इसमें फेक प्रोफाइल्स और डिसइनफॉर्मेशन का भी रोल देखा गया, जो विरोध को बढ़ावा दे सकता है।
भारत पर प्रभाव- नेपाल भारत का निकटतम पड़ोसी है, जहां 1,751 किमी की खुली सीमा है। इस उथल-पुथल का भारत पर सीधा और अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा है: सुरक्षा और सीमा प्रभाव: भारत-नेपाल सीमा पर हाई अलर्ट घोषित किया गया, विशेषकर बिहार के जोगबनी में। बाजार बंद हो गए, और भारतीय परिवारों (मुख्य रूप से बिजनेस हाउस) पर हमले, लूटपाट और उनके घरों-दफ्तरों में आग लगाई गई। एक भारतीय मॉल भी जलाया गया। भारत ने अपने नागरिकों को सावधानी बरतने की सलाह दी। अस्थिरता से शरणार्थी प्रवाह, तस्करी और सीमा सुरक्षा खतरे बढ़ सकते हैं। आर्थिक प्रभाव: नेपाल भारत का प्रमुख व्यापारिक साझेदार है, लेकिन उथल-पुथल से व्यापार प्रभावित हुआ। अनुमानित 21 अरब डॉलर का आर्थिक नुकसान नेपाल को प्रभावित करेगा, जो भारत के निर्यात (ईंधन, दवाएं) पर निर्भर है। भारतीय निवेश और प्रवासी नेपाली (भारत में काम करने वाले) प्रभावित होंगे। भू-राजनीतिक प्रभाव: नेपाल भारत और चीन के बीच स्थित है, इसलिए अस्थिरता से दोनों शक्तियां प्रभाव बढ़ाने की कोशिश करेंगी। कुछ विश्लेषणों में अमेरिकी प्रभाव (NED जैसे संगठनों से) का जिक्र है, जो भारत-नेपाल संबंधों को कमजोर कर सकता है। नेपाल तीसरा पड़ोसी देश है जहां हालिया वर्षों में उथल-पुथल से सरकार गिरी (श्रीलंका और बांग्लादेश के बाद), जो भारत की पड़ोसी डिप्लोमेसी पर दबाव डालता है। सीमा विवाद (लिपुलेख, कालापानी) फिर उभर सकते हैं। कुल मिलाकर, ये घटनाएं नेपाल की राजनीति में परिवर्तन का संकेत हैं, लेकिन भारत के लिए सुरक्षा, आर्थिक और रणनीतिक चुनौतियां पैदा करती हैं। भारत ने शांति की कामना की है और संवाद पर जोर दिया है।
Answer to 1(a)
The Quit India Movement was launched on August 8, 1942, by Mahatma Gandhi. It was the final and most widespread mass movement of the Indian freedom struggle, arising from the frustrations among Indians due to the post-World War II circumstances and the failure of the Cripps Mission. The main objective of this movement was to free India from British rule. In July 1942, during a meeting of the Congress Working Committee, Gandhiji sought permission to launch the movement, but this time several leaders strongly opposed him. At that time, Gandhiji was quite distressed due to the strategic, economic, and political situations and, while warning the Congress, he declared, “I will build an organization bigger than the Congress from a handful of sand in the country.” Later, the Congress granted him permission to proceed with the movement. On August 8, 1942, Gandhiji organized a meeting at Gowalia Tank Maidan in Bombay, where, in front of a crowd of lakhs, he sharply criticized the government and gave the slogan “Do or Die.” With this, the Quit India Movement spread across the entire country.
Bihar played a very important role in the Quit India Movement. As soon as the Quit India resolution was passed on August 8, most Congress leaders were arrested. After these arrests, the movement intensified throughout the country. On September 9, 1942, Rajendra Prasad was arrested and sent to Bankipur Central Jail. Students strongly protested Rajendra Prasad’s arrest. There was a strike at all educational institutions; in this sequence, on August 11, a procession of students attempted to hoist the flag at the Secretariat building. On the orders of Patna’s District Collector W.G. Archer, bullets were fired on the patriotic students, in which seven students were killed. This entire incident is known as the “Secretariat Shooting.”
During the Quit India Movement in 1942, Jayaprakash Narayan was arrested and imprisoned in Hazaribagh Jail. However, Jayaprakash Narayan escaped from jail along with four companions—Surya Narayan Singh, Yogendra Shukla, Shaligram Singh, and Gulali Prasad—and took shelter in the Terai region of Nepal. Under Jayaprakash Narayan’s leadership, the ‘Azad Dasta’ was formed in Nepal to train young men in guerrilla warfare. The main objective of the Azad Dasta was to carry out sabotage against the government. The Azad Dasta remained actively involved in the movement until 1943, but with the cooperation of the Nepal government, the British government arrested Jayaprakash Narayan, Ram Manohar Lohia, Aruna Asaf Ali, and Shaligram ji. After this, during the Quit India Movement, Jayaprakash Narayan remained active in underground activities at that time.
On November 9, 1942, on the night of Diwali, he escaped from Hazaribagh Central Jail along with his companions Ramanandan Mishra, Yogendra Shukla, and Suraj Narayan Singh. After this, to fight against British rule, he established an armed guerrilla force called ‘Azad Dasta’ in the Rajbilas jungle in the Terai region of Nepal.
The main objectives of this squad were: - To damage British property. - To carry out sabotage actions against the government. - To paralyze foreign rule through guerrilla warfare.
Major Activities: The ‘Azad Dasta’ was the first secret activity carried out by revolutionaries during the Quit India Movement. Its members were trained in guerrilla warfare and sabotage. In March 1943, a guerrilla training center was also established in Rajbilas, Nepal, to train youth.
Major Roles: Guerrilla Warfare Training and Armed Resistance: The Azad Dasta provided guerrilla warfare training to youth in the forests of Nepal so that armed struggle against British rule could continue. Its aim was to uproot British imperialism. Sabotage and Resistance Activities: In the rural areas of Bihar, attacks, sabotage, and destructive actions were carried out on British property (such as railways, post offices, police stations). This squad traveled from village to village, garnering support from farmers and villagers. Continuing the Movement: After the arrest of leaders, it became a means to keep the movement alive through underground methods. It was connected to Congress Socialist Groups and expanded the movement to the rural level. Participation of the General Public: Considering the intensity of the movement in Bihar, this squad helped in organizing local people and countering British repression.
The squad’s main activities included: - Disrupting communication means: Telephone and telegraph services were shut down. - Halting transportation: Railway tracks were uprooted. - Attacks on government buildings: Arson was committed in government buildings like post offices, railway stations, and police stations.
In Bihar, the provincial ‘Azad Dasta’ was led by Suraj Narayan Singh. The influence of this squad extended to several districts such as Bhagalpur, Munger, Kishanganj, Purnia.
Suppression and End: The increasing activities of the ‘Azad Dasta’ worried the British government. Under pressure from the British government, the Nepal government arrested Jayaprakash Narayan, Ram Manohar Lohia, and other leaders in May 1943. Despite these arrests, the squad remained active until 1943. Besides the ‘Azad Dasta’, other secret revolutionary organizations like the Siyaram Dal were also active in Bihar, led by Siyaram Singh, and their influence was in several districts. These organizations kept the movement alive even when most major leaders were in jail and gave the movement in Bihar a militant form.
Answer to (b)
Mauryan art and architecture flourished between the fourth and second centuries BCE. This dynasty lasted from 322 BCE to 185 BCE. The art and architecture of the Mauryan Empire were characterized by the construction of pillars, stupas, and viharas. The pillars were made of sandstone. This was one of the special features of Mauryan art and architecture. These pillars bore the rock edicts of Emperor Ashoka. Stupas were large dome-shaped structures used as Buddhist temples. Viharas were residential buildings for Buddhist monks. Mauryan art was primarily represented through sculpture. This period is known for the development of stone carving art.
Background of Mauryan Art and Architecture - The Mauryan Empire was founded by Chandragupta Maurya in 321 BCE. This was an important time in Indian history. Between the Harappan and Mauryan periods, there was a decline in stone-built structures.
The most prominent feature of Mauryan sculpture is the use of polished or glossy sandstone surfaces and the division of art into royal (courtly) and folk art. This art represents an important transition in the history of Indian sculpture from wood to stone.
The distinct characteristics of Mauryan sculpture are as follows:
Glossy Polish (Opdar Surface): A special type of polish was applied to Mauryan sculptures and pillars, making them shine like glass. This technique was so advanced that even today, this shine can be seen on pillars like those at Sarnath. It is considered similar to the shine of the "Northern Black Polished Ware" (NBPW) culture. Extensive Use of Stone: During this period, stone was used on a large scale for sculpture, especially Chunar sandstone. Before this, wood was more commonly used in architecture and sculpture.
Classification of Art: Mauryan sculpture can be divided into two main parts: 1. Royal or Courtly Art: - This includes the massive monolithic (single stone) pillars commissioned by Emperor Ashoka. These pillars are the finest examples of Mauryan art. 2. Folk Art: This includes large statues of Yakshas and Yakshinis, which reflect local folk beliefs and religious traditions. The statue of the Yakshini from Didarganj is a famous example of this.
Realistic and Natural Depiction: Mauryan sculptors depicted animals and humans with extreme naturalism and realism. On the lion capital at Sarnath, the protruding veins of the lions, the heaviness of their bodies, and their dynamic postures demonstrate their lifelike portrayal. Distinct Structure of Pillars: Ashoka's pillars have their own unique structure. Pillar Shaft: It tapers from bottom to top. Capital Part: Above the shaft is the capital, which includes an inverted bell-shaped lotus, a round or square abacus, and an animal figure mounted on the abacus. Animal Figures: Figures such as elephants, horses, bulls, and lions are carved on the abacus. Grand statues of animals like lions, bulls, or elephants are also installed at the top of the pillars.
Use of Symbolism: There is a deep use of symbols in Mauryan sculpture. For example, the wheel on the top of the Sarnath pillar symbolizes the 'Dharmachakra', representing Buddha's first sermon (Dharmachakra Pravartan). The depiction of animals is also considered symbolic of various directions and stages of life.
Major Materials -
Answer to 2(A)
India is a socialist, secular, democratic republic and the world’s largest democracy. The modern Indian nation-state came into existence on August 15, 1947. Since then, free and fair elections have been conducted at regular intervals in accordance with the principles enshrined in the Constitution, electoral methods, and procedures. The Constitution of India has entrusted the Election Commission of India with the superintendence, direction, and control of the entire process for the conduct of elections to Parliament, the State Legislatures, and the offices of the President and Vice-President of India. The Election Commission of India is a permanent constitutional body. According to the Constitution, the Election Commission was established on January 25, 1950.
Initially, the Commission consisted of only one Chief Election Commissioner. Currently, it comprises one Chief Election Commissioner and two Election Commissioners.
On October 16, 1989, two additional Commissioners were appointed for the first time, but their tenure was very short, lasting until January 1, 1990. Subsequently, on October 1, 1993, two additional Election Commissioners were appointed. Since then, the multi-member concept of the Commission has been in practice, with decisions taken by majority.
Appointment and Tenure of Commissioners -
Positive Aspects:
Negative Aspects:
Thus, EPIC is essential for electoral integrity, but to make it more inclusive, offline distribution should be strengthened and data security ensured. The digital transition is positive, but attention must be paid to accessibility for all sections.
Answer to 2(B)
The criminalization of politics refers to the entanglement of criminal elements in the political sphere. It indicates the active participation and involvement of individuals with criminal backgrounds in electoral processes, political parties, and governance. Such individuals may have been convicted of criminal offenses, may be involved in illegal activities, or may be connected to criminal networks. The criminalization of politics includes not only their participation in politics but also corruption, influence peddling, and the erosion of democratic values.
Major Causes of the Criminalization of Politics in India -
Background of the Establishment of the Vohra Committee - The high-level committee, chaired by Central Home Secretary N.N. Vohra, was formed on July 9, 1993, with its first meeting held on July 15, 1993. The committee was primarily constituted to investigate the suspicious connections between the Dawood Ibrahim gang and other organized criminals with political and bureaucratic patronage following the March 1993 Mumbai bomb blasts. In addition to the Home Ministry, the committee included top officials from RAW, IB, CBI, and the Special Security Division. As stated by Vision IAS, the objective of this committee was to “identify the extent of the politico-criminal nexus and recommend ways to effectively deal with the criminalization of politics.”
Main Observations of the Committee on Criminalization - The Vohra Committee report clearly stated that criminal gangs in the country are functioning like a “parallel government” in a way, and politicians have become patrons of these gangs. The report named Dawood Ibrahim, Iqbal Mirchi, Memon brothers, etc., and explained that these mafias had built political and bureaucratic contacts through sources of income such as extortion, illegal land encroachment, and hawala. In several states of India (such as Bihar, UP, Haryana), local armed gangs received cover from parties, and criminals reached assemblies/parliaments by winning elections. The Supreme Court also, in 2018, referred to this report and stated that these agencies have unanimously acknowledged that the criminal-politician-bureaucrat nexus is severely affecting law and order in the country. The court said that overall, many criminals have been elected to local bodies, assemblies, and Parliament in the last decade.
Major Recommendations of the Committee -
The Vohra Committee made several concrete suggestions to deal with the criminal-political nexus. The main suggestions included:
| Suggestions/Measures | Government Action/Status |
Other Important Facts - According to data from the Association for Democratic Reforms (ADR), the number of elected representatives with criminal backgrounds in the Indian Parliament has been steadily increasing since 2004. In the 2004 Lok Sabha, 24% of MPs had criminal cases pending, which rose to 43% in 2019. A petition filed in February 2023 highlighted a 44% increase in MPs with declared criminal cases since 2009. During the 2019 elections, 159 MPs were found to have serious charges such as rape, murder, attempt to murder, kidnapping, and crimes against women. In the recently elected 18th Lok Sabha (2024), ADR reported that 43% of MPs have declared criminal cases, of which 29% have serious criminal charges. This trend underscores the growing normalization of the criminalization of politics in India. On a party-wise basis, the BJP has the highest number of MPs with criminal cases, followed by Congress; all major parties field candidates with pending charges and often prioritize “winnability” over clean records.
Key Points of the Supreme Court Order -
Impact of the Criminalization of Politics -
Previous Efforts at Reforms in the Indian Electoral System -
1. Dinesh Goswami Committee (1990): The committee recommended in its report controls on electoral expenditure, a ban on donations from companies, the role of the state in elections, and monitoring and provisions related to other aspects of elections such as campaign time, age limit, powers of the Election Commission, etc. 2. Vohra Committee (1993): The Vohra Committee expressed concern over the increasing criminalization in politics and their political patronage, advising the assistance of various crime control institutions (CBI, Income Tax, Narcotics, etc.) to solve this problem. 3. Indrajit Gupta Committee (1998): The Gupta Committee recommended in its report that the state bear electoral expenditure to reduce corruption and crime in politics. 4. Law Commission Report (1999): In its 170th report in 1999, the Law Commission supported holding Lok Sabha and Assembly elections simultaneously. 5. MN Venkatchaliah Committee (2000-02) – Reports of the Law Commission, Election Commission, National Commission for Review of the Constitution. 6. Wanchoo Committee (Direct Taxes Enquiry Committee) – The Wanchoo Committee released its report on the regulation of political donations along with other economic activities of political parties.
Role of the Supreme Court in Electoral Reforms -
In October 1974, the Supreme Court in Kanwar Lal Gupta v. Amar Nath Chawla and Others directed that any expenditure on the candidate’s campaign (whether party-sponsored or by any supporter) be added to the prescribed limit for the candidate. In 2002, in the historic case of Union of India v. Association for Democratic Reforms, the Supreme Court ruled that every candidate contesting elections for Parliament, State Assemblies, or Municipal Corporations must declare their criminal, financial, and educational background. In 2005, in the Ramesh Dalal v. Union of India case, the Supreme Court stated that a Member of Parliament (MP) or State Legislature member (MLA) will be disqualified from contesting elections upon conviction and will not be sentenced to less than 2 years’ imprisonment by the court. In an important 2017 decision, the Supreme Court reiterated the mandatory public disclosure of candidates’ criminal backgrounds and ordered the establishment of fast-track courts for the trial of ongoing criminal cases against politicians.
Critical Analysis - The Vohra Committee’s recommendations were practical in the direction of institutional and legal reforms, but there were many obstacles in their implementation. Due to the report being kept confidential, reliable action on it was hindered. The Supreme Court also commented that the nodal agency formed by the government was unsatisfactory and lacked independence. Due to a lack of national will and political resistance, many suggestions could not be implemented on the ground. On the other hand, semi-implemented changes have occurred: The Election Commission and courts have implemented several reforms, such as making it mandatory for candidates to declare their criminal past, disqualifying convicted MPs (Lily Thomas), and ordering the public disclosure of candidate information. However, despite these, criminalization in Indian politics has not stopped completely. Political parties still give tickets to criminals because they influence vote banks through money and muscle power. Overall, the committee expressed deep concern over the criminal-politician-bureaucrat nexus and suggested concrete measures for reform, but most of it remains pending. Detailed progress has remained incomplete due to extraordinary logic and legal hurdles (such as the Supreme Court’s statement in municipal elections that disqualification cannot be based solely on charges). Consequently, despite policy-makers and judicial interventions, the problem of criminalization of politics persists. This indicates that broad reforms require political will, transparency, and institutional strengthening.
What Does the Representation of the People Act Say? Section 8 of the Representation of the People Act, 1951, bars convicted politicians from contesting elections. However, leaders who only have pending cases against them are free to contest elections. It does not matter how serious the charges against them are. Under Sections 8(1) and 8(2) of this Act, provisions state that if a legislature member (MP or MLA) is involved in crimes such as murder, rape, untouchability, violation of the Foreign Exchange Regulation Act; promoting enmity on the basis of religion, language, or region, insulting the Indian Constitution, importing or exporting prohibited goods, or involvement in terrorist activities, then under this section, he will be considered disqualified and declared disqualified for a period of 6 years. On the other hand, Section 8(3) of this Act provides that any legislature member convicted of any other offense besides the above, if sentenced to imprisonment of more than two years, will be considered disqualified from the date of conviction. Such a person will be considered disqualified from contesting elections for 6 years from the date of completion of the sentence.
Challenges - In its order, the Supreme Court has left the decision on people with criminal backgrounds involved in politics to the discretion of political parties and the public instead of direct action. In such a case, big changes in politics cannot be expected soon from the court’s order. In the Supreme Court order, instead of directing action against individuals with criminal backgrounds, the Election Commission has been instructed to monitor them and inform the court accordingly as per rules. This arrangement, rather than providing a solution to the already lengthy judicial process regarding political criminals, makes it even more complex. In the context of political transparency, the court’s order can be effective only if political parties follow the rules in this regard and provide correct information keeping public interest in mind. However, in this era of fake news, reaching accurate information to the public is very difficult; therefore, big reforms in politics cannot be expected from the court’s order.
Conclusion - Given the increasing number of criminals in the country’s politics, it has become necessary for Parliament to enact a law so that criminals stay away from politics. People elected as public representatives should be above the politics of crime. The nation awaits a law to be made by Parliament. A major effort needs to be made to clean up India’s tainted politics.
Answer to 3
The relations between India and Nepal are deeply intertwined historically, culturally, economically, and geographically. The two countries share a 1,751-kilometer open border, which adjoins the states of Sikkim, West Bengal, Bihar, Uttar Pradesh, and Uttarakhand. The 1950 Treaty of Peace and Friendship forms the basis of these relations, providing equal rights to citizens of both countries in each other's territories. However, the state of relations in 2025 is mixed—one side features strong economic cooperation and cultural bonds, while the other involves political instability, border disputes, and the influence of external powers (such as China and the United States) creating challenges.
Positive Aspects: 1. Economic Cooperation: India is Nepal's largest trading partner, accounting for about 64% of Nepal's total foreign trade. In 2025, bilateral trade has exceeded 8 billion dollars. India supplies fuel, medicines, and other essential goods to Nepal. Cooperation in the energy sector has increased, such as Nepal's electricity exports to India. Additionally, Indian investment accounts for more than 35% of foreign direct investment (FDI) in Nepal. 2. Cultural and Humanitarian Ties: Around 600,000 Nepalis work in India, and Indian tourists support Nepal's economy. In 2025, joint project monitoring committee meetings between the two countries focused on development projects. 3. Strategic Improvements: In August 2025, Nepal's Prime Minister KP Sharma Oli received an invitation for a visit to India, signaling an improvement in relations. Previously, Oli's China-friendly policies had been controversial, but dialogue is now increasing.
Negative Aspects and Challenges: 1. Nepal's Political Instability: In September 2025, large-scale youth-led protests occurred in Nepal, leading to the fall of the government and the formation of an interim government. These protests were against corruption, unemployment, and restrictions on freedom of expression (such as social media bans). India exercised caution, advising its citizens to be careful and increasing checks at the border. This instability is affecting India's neighborhood policy, as Nepal has become the third neighboring country where violent upheaval has changed the government in recent years (after Sri Lanka and Bangladesh). 2. External Influences: Both China and the United States are keeping an eye on Nepal's situation. Oli sought help from China on the Lipulekh issue, but China refused intervention, calling it a bilateral matter. Meanwhile, some analyses suggest that the United States might use Nepal to weaponize border disputes against India, especially in the context of India-Pakistan tensions. This could impact India's regional security.
Overall Analysis: In 2025, relations are stable but tense. Nepal's internal unrest could lead to refugee influx, border smuggling, and investment risks for India. However, cooperation between the two countries continues, and India is emphasizing dialogue while respecting Nepal's sovereignty. In the future, if Nepal's new government proves India-friendly, relations could strengthen, but China's influence and border disputes will remain obstacles.
Basic Facts of Disputes Between the Two Countries - The disputes between India and Nepal are primarily centered on borders, economic dependence, and political issues. These disputes stem from the 1816 Treaty of Sugauli, which defined the border between British India and Nepal. The main basic facts are as follows:
These disputes require resolution through dialogue, but external influences complicate them. Overall, building trust and bilateral talks are crucial for strengthening relations.
Recently, the Indian Prime Minister visited Buddha's birthplace, Lumbini, Nepal, where he laid the foundation stone for a Buddhist monastery being built with Indian assistance, along with the Nepalese Prime Minister. After taking oath in July 2021, the Nepalese Prime Minister also made his first bilateral visit to India. This visit was successful in initiating connectivity projects and signing Memorandums of Understanding (MoUs).
Historical Relations - Nepal is an important neighbor of India and holds special importance in its foreign policy due to centuries-old geographical, historical, cultural, and economic ties/relations. India and Nepal share common ties with Buddha's birthplace Lumbini in the context of Hinduism and Buddhism, which is located in present-day Nepal. Both countries not only share an open border and unimpeded movement of people but also have close relations through marriages and family ties, known as the "roti-beti" relationship. The 1950 India-Nepal Treaty of Peace and Friendship forms the basis of the special relations existing between India and Nepal.
1950 Treaty of Peace and Friendship - This treaty outlines the reciprocal treatment of Indian and Nepali citizens regarding residence, property, trade, and movement in both countries. It also establishes national treatment for both Indian and Nepali businesses (i.e., once imported, foreign goods will not be treated differently from domestic goods). It also ensures India's access to arms for Nepal.
Importance of Nepal for India - Nepal shares a border with five Indian states—Uttarakhand, Uttar Pradesh, West Bengal, Sikkim, and Bihar. Therefore, it is an important hub for cultural and economic exchange. The importance of Nepal for India can be studied from two different angles: Their strategic importance for India's national security. Their place in India's role in international politics. Nepal is right in the middle of India's "Himalayan borders" and, along with Bhutan, acts as a northern "buffer" and serves as buffer states against any potential invasion from China. The rivers originating in Nepal nourish India's perennial river systems in terms of ecology and hydropower potential. Many Hindu and Buddhist religious sites are in Nepal, making it an important pilgrimage site for a large number of Indians.
Areas of Cooperation Between the Two Countries - Trade and Economy: In addition to providing transit for trade with the rest of the world, India is Nepal's largest trading partner and the biggest source of foreign investment. In 2018-19, total bilateral trade reached 57,858 crore rupees (8.27 billion US dollars). In 2018-19, while Nepal's exports to India were 3,558 crore rupees (US$508 million), India's exports to Nepal were 54,300 crore rupees (7.76 billion US dollars). Indian firms engaged in manufacturing, services (banking, insurance, dry ports), power sector, and tourism industry, etc.
Connectivity: As a landlocked country, Nepal is surrounded by India on three sides and opens toward Tibet on one side, where vehicle access is very limited. India and Nepal have initiated various connectivity programs to enhance people-to-people contact and promote economic development. An MoU has been signed between the two governments to lay an electric rail track connecting Kathmandu to Raxaul in India. India wants to develop inland waterways for cargo movement within the framework of trade and transit arrangements, providing Nepal with additional access to the sea (Indian Ocean), connecting Sagarmatha (Mount Everest) to the sea.
Development Assistance: The Government of India provides development assistance to Nepal, focusing on building infrastructure at the grassroots level. Assistance areas include infrastructure, health, water resources, education, and rural and community development.
Defense Cooperation: Bilateral defense cooperation includes assisting the Nepalese Army in its modernization through the provision of equipment and training. The Indian Army's Gorkha Regiments are partially formed by recruitment from Nepal's hill districts. India conducts a joint military exercise with Nepal every year since 2011, known as 'Surya Kiran'. Cultural: Initiatives have been taken to promote people-to-people contact in the fields of art and culture, academics, and media with various local bodies of Nepal. India has signed three sister-city agreements connecting Kathmandu-Varanasi, Lumbini-Bodh Gaya, and Janakpur-Ayodhya.
Humanitarian Assistance: Nepal is located in a sensitive ecologically fragile area prone to earthquakes and floods, causing heavy loss of life and property, making it the largest recipient of India's humanitarian assistance. Indian Community: A large number of Indians live in Nepal, including businessmen, traders, doctors, engineers, and laborers (including seasonal/migrant in the construction sector).
Multilateral Partnership: India and Nepal share several multilateral forums such as BBIN (Bangladesh, Bhutan, India, and Nepal), BIMSTEC (Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation), Non-Aligned Movement, and SAARC (South Asian Association for Regional Cooperation), etc.
What Are the Recent Developments? Arun-3 Hydropower Project: In 2019, the Cabinet also approved an investment of ₹1,236 crore for the Arun-3 hydropower project. Arun-3 Hydro Electric Project (900 MW) is a run-of-the-river located on the Arun River in eastern Nepal. Build Operate and Transfer (BOOT): In 2008, an MoU was signed between the Nepal government and Satluj Jal Vidyut Nigam (SJVN) Limited for execution on a Build Own Operate and Transfer (BOOT) basis for a period of 30 years including a 5-year moratorium period.
International Center for Buddhist Culture and Heritage: During the Indian Prime Minister's visit, he performed the 'Shilanyas' ceremony to inaugurate the construction of the India International Buddhist Culture and Heritage Center in the Lumbini monastic zone. This center will provide a world-class facility to welcome pilgrims and tourists from around the world to experience the essence of Buddhism's spiritual aspects. The facility aims to provide boarding for scholars and Buddhist pilgrims from around the world who come to Lumbini.
Hydropower Projects: The two leaders signed five agreements between Satluj Jal Vidyut Nigam (SJVN) Limited and Nepal Electricity Authority (NEA) for the development and implementation of the 490.2 MW Arun-4 hydropower project. Nepal has also invited Indian companies to invest in the West Seti Hydropower Project in Nepal.
Establishment of Satellite Campus: India has offered to establish a satellite campus of the Indian Institute of Technology (IIT) in Rupandehi and has sent some draft MoUs for signing between Indian and Nepali universities.
Panchheshwar Multipurpose Project: Nepal discussed some pending projects, such as the Panchheshwar Multipurpose Project, an important branch of the Mahakali Treaty signed between Nepal and India in 1996, and the West Seti Hydropower Project, a reservoir-type project with an estimated capacity of 1,200 MW.
Cross-Border Rail Link: The operation of the 35-kilometer cross-border rail link from Jaynagar (Bihar) to Kurtha (Nepal) will be extended further to Bijalpura and Bardibas.
Double Circuit Transmission Line: Another project includes a 90 km long 132 kV double circuit transmission line connecting Tila (Solukhumbu) to Mirchaiya (Siraaha) near the Indian border.
Multilateral Projects: Additionally, agreements were signed for technical cooperation in the railway sector, Nepal's joining the International Solar Alliance, and between Indian Oil Corporation and Nepal Oil Corporation to ensure regular supply of petroleum products.
Major Challenges - Territorial Disputes: One of the main challenges in India-Nepal relations is the Kalapani border issue. These borders were determined by the British in 1816, and India inherited the areas over which the British exercised territorial control in 1947. While 98% of the India-Nepal border has been demarcated, two areas—Susta and Kalapani—remain undecided. In 2019, Nepal issued a new political map claiming the areas of Kalapani, Limpiyadhura, and Lipulekh in Uttarakhand, and Susta (West Champaran district, Bihar) as part of Nepal's territory.
Issues with the Peace and Friendship Treaty: The 1950 Peace and Friendship Treaty was sought by Nepali officials in 1949 to continue their special relations with British India and provide them with an open border and the right to work in India. But today, it is seen as a marker of unequal relations and imposing Indian influence. The idea of improving it has been mentioned in joint statements since the mid-1990s but in a sporadic and insulting manner.
Hiccups Due to Demonetization: In November 2016, India withdrew high-value notes of 15.44 trillion rupees (1,000 rupees and 500 rupees). Today, more than 15.3 trillion rupees have been returned. Yet many Nepali citizens who were legally entitled to hold 25,000 rupees in Indian currency (given that the Nepali rupee is pegged to the Indian rupee) were left helpless. The Nepal Rastra Bank (Central Bank of Nepal) has 70 million rupees, and public holdings are estimated at 500 crore rupees. The refusal by India to accept demonetized bills at the Nepal Rastra Bank and the pending decision on the report presented by the Eminent Persons' Group (EPG) have not helped in gaining a better image of India in Nepal.
China's Intervention: In recent years, Nepal has moved away from Indian influence, and China has gradually filled this space with investments, aid, and loans. China considers Nepal a key partner in its Belt and Road Initiative (BRI) and wants to invest in Nepal's infrastructure as part of its grand plans to promote global trade. Nepal and China's growing cooperation could weaken Nepal's role as a buffer state between India and China. On the other hand, China wants to avoid the formation of any anti-China stance by Tibetans living in Nepal. Internal Security: This is a major concern for India because the India-Nepal border is virtually open, used by terrorist organizations and insurgent groups in India's Northeast for supplying trained cadres and fake Indian currency. Trust and Ethical Differences: Delays in the implementation of various projects have widened the trust deficit between India and Nepal. There is anti-India sentiment among some ethnic groups in Nepal, arising from the perception that India is too involved in Nepal and tampers with their political sovereignty.
Other Important Facts -
Steps Important for the Future -
Recent Political Unrest in Nepal -
Impact on India - Nepal is India's closest neighbor, with a 1,751 km open border. This upheaval has had direct and indirect effects on India: Security and Border Impact: High alert was declared on the India-Nepal border, especially at Jogbani in Bihar. Markets shut down, and attacks, looting, and arson on Indian families (mainly business houses) and their homes/offices occurred. An Indian mall was also burned. India advised its citizens to exercise caution. Instability could increase refugee influx, smuggling, and border security threats. Economic Impact: Nepal is India's major trading partner, but the upheaval affected trade. The estimated 21 billion dollar economic loss to Nepal will impact India's exports (fuel, medicines). Indian investments and migrant Nepalis (working in India) will be affected. Geopolitical Impact: Nepal is situated between India and China, so instability will lead both powers to try to increase influence. Some analyses mention US influence (from organizations like NED), which could weaken India-Nepal relations. Nepal is the third neighboring country where upheaval has toppled the government in recent years (after Sri Lanka and Bangladesh), putting pressure on India's neighborhood diplomacy. Border disputes (Lipulekh, Kalapani) could resurface. Overall, these events signal change in Nepal's politics but pose security, economic, and strategic challenges for India. India has wished for peace and emphasized dialogue.
|
Comments
Releted Blogs
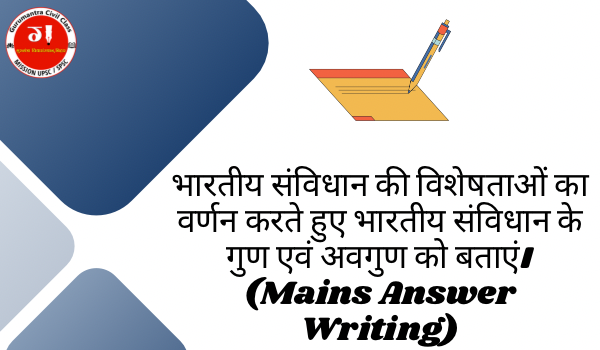
भारतीय संविधान की विशेषताओं का वर्णन करते हुए भारतीय संविधान के गुण एवं अवगुण को बताएं।(Mains Answer Writing)
By - Gurumantra Civil Class
Gurumantra GS Answer Writing Practice

भारत में जनसंख्या नियंत्रण के उपाय पर प्रकाश डालें - Answer writing for Mains Exam
By - Gurumantra Civil Class
जनसंख्या नियंत्रण के लिए किए गए प्रयास एवं उपाय
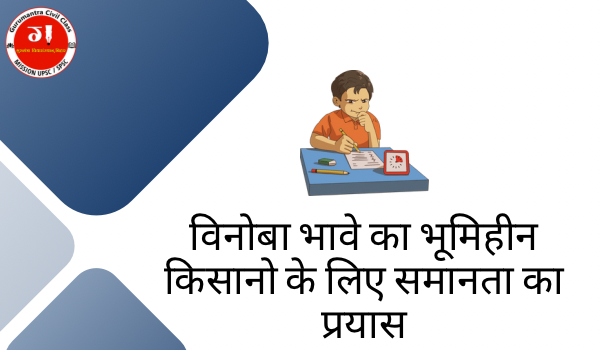
विनोबा भावे का भूमिहीन किसानों के लिए समानता का प्रयास(Vinoba Bhave's attempt at equality for the landless farmers) GS Mains Writing
By - Gurumantra Civil Class
GS Mains Writing for Civil Service

महासागरीय लवणता में विभिन्नता के कारण और प्रभाव ( Causes and Effects of Variation in Ocean Salinity) GS Mains Answer Writing
By - Gurumantra Civil Class
GS Mains Answer Writing for Civil Service Exam.